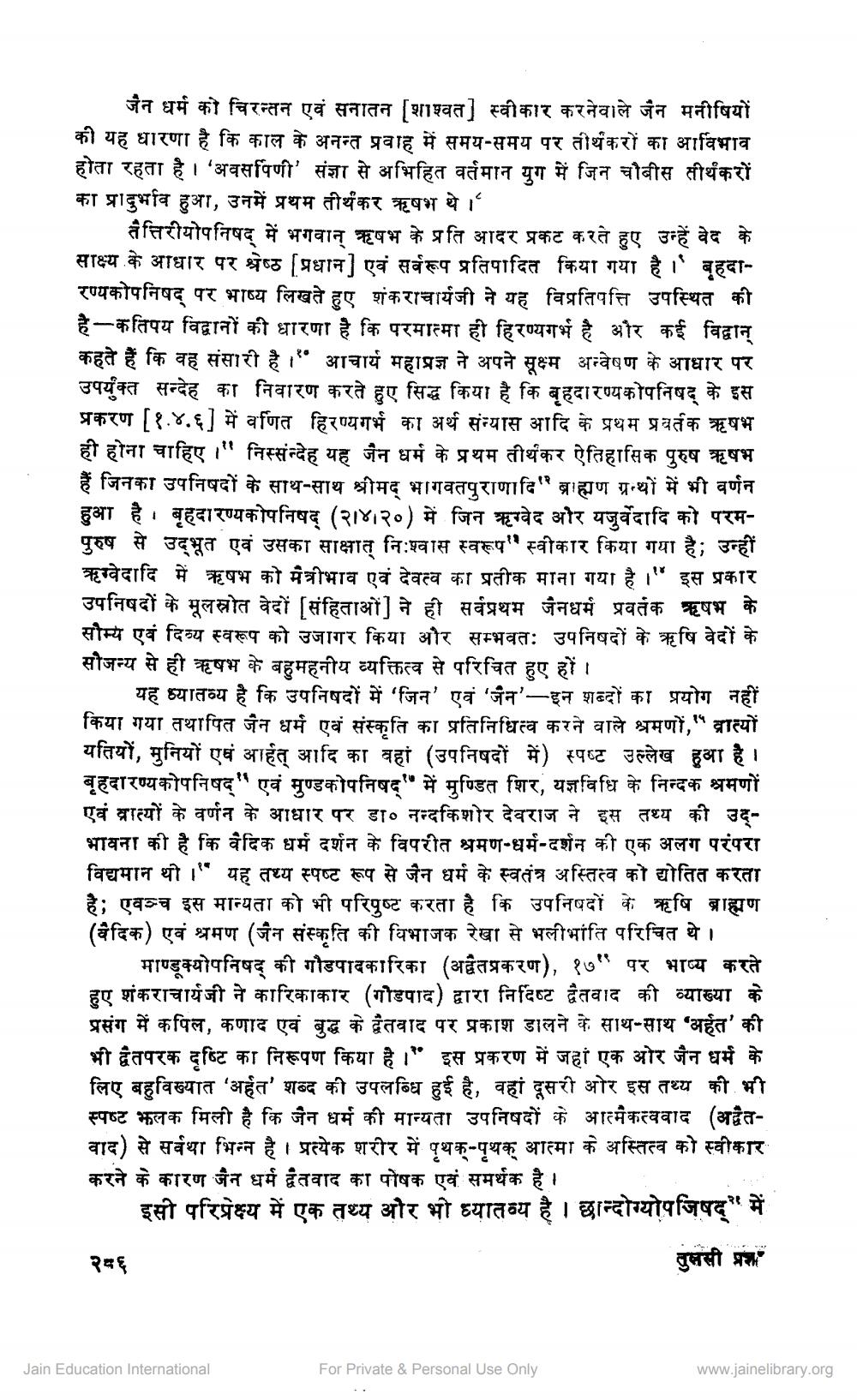________________
जैन धर्म को चिरन्तन एवं सनातन [शाश्वत] स्वीकार करनेवाले जैन मनीषियों की यह धारणा है कि काल के अनन्त प्रवाह में समय-समय पर तीर्थंकरों का आविभाव होता रहता है । 'अवसर्पिणी' संज्ञा से अभिहित वर्तमान युग में जिन चौबीस तीर्थंकरों का प्रादुर्भाव हुआ, उनमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभ थे।
तैत्तिरीयोपनिषद् में भगवान ऋषभ के प्रति आदर प्रकट करते हुए उन्हें वेद के साक्ष्य के आधार पर श्रेष्ठ [प्रधान एवं सर्वरूप प्रतिपादित किया गया है।' बृहदारण्यकोपनिषद् पर भाष्य लिखते हुए शंकराचार्यजी ने यह विप्रतिपत्ति उपस्थित की है-कतिपय विद्वानों की धारणा है कि परमात्मा ही हिरण्यगर्भ है और कई विद्वान् कहते हैं कि वह संसारी है।" आचार्य महाप्रज्ञ ने अपने सूक्ष्म अन्वेषण के आधार पर उपर्युक्त सन्देह का निवारण करते हुए सिद्ध किया है कि बृहदारण्यकोपनिषद् के इस प्रकरण [१.४.६] में वणित हिरण्यगर्भ का अर्थ संन्यास आदि के प्रथम प्रवर्तक ऋषभ ही होना चाहिए ।" निस्सन्देह यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऐतिहासिक पुरुष ऋषभ हैं जिनका उपनिषदों के साथ-साथ श्रीमद् भागवतपुराणादि ब्राह्मण ग्रन्थों में भी वर्णन हुआ है। बृहदारण्यकोपनिषद् (२।४।२०) में जिन ऋग्वेद और यजुर्वेदादि को परमपुरुष से उद्भूत एवं उसका साक्षात् निःश्वास स्वरूप" स्वीकार किया गया है। उन्हीं ऋग्वेदादि में ऋषभ को मैत्रीभाव एवं देवत्व का प्रतीक माना गया है ।" इस प्रकार उपनिषदों के मूलस्रोत वेदों [संहिताओं] ने ही सर्वप्रथम जैनधर्म प्रवर्तक ऋषभ के सौम्य एवं दिव्य स्वरूप को उजागर किया और सम्भवत: उपनिषदों के ऋषि वेदों के सौजन्य से ही ऋषभ के बहुमहनीय व्यक्तित्व से परिचित हुए हों।
यह ध्यातव्य है कि उपनिषदों में 'जिन' एवं 'जन'-इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया तथापित जैन धर्म एवं संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रमणों," व्रात्यों यतियों, मुनियों एवं आर्हत् आदि का वहां (उपनिषदों में) स्पष्ट उल्लेख हुआ है । बृहदारण्यकोपनिषद् एवं मुण्डकोपनिषद् में मुण्डित शिर, यज्ञविधि के निन्दक श्रमणों एवं प्रात्यों के वर्णन के आधार पर डा० नन्दकिशोर देवराज ने इस तथ्य की उद्भावना की है कि वैदिक धर्म दर्शन के विपरीत श्रमण-धर्म-दर्शन की एक अलग परंपरा विद्यमान थी।" यह तथ्य स्पष्ट रूप से जैन धर्म के स्वतंत्र अस्तित्व को धोतित करता है; एवञ्च इस मान्यता को भी परिपुष्ट करता है कि उपनिषदों के ऋषि ब्राह्मण (वैदिक) एवं श्रमण (जैन संस्कृति की विभाजक रेखा से भलीभांति परिचित थे।
माण्डूक्योपनिषद् की गौडपादकारिका (अद्वैतप्रकरण), १७१ पर भाष्य करते हुए शंकराचार्यजी ने कारिकाकार (गौडपाद) द्वारा निर्दिष्ट द्वैतवाद की व्याख्या के प्रसंग में कपिल, कणाद एवं बुद्ध के द्वैतवाद पर प्रकाश डालने के साथ-साथ 'अर्हत' की भी द्वैतपरक दृष्टि का निरूपण किया है।" इस प्रकरण में जहां एक ओर जैन धर्म के लिए बहुविख्यात 'अर्हत' शब्द की उपलब्धि हुई है, वहां दूसरी ओर इस तथ्य की भी स्पष्ट झलक मिली है कि जैन धर्म की मान्यता उपनिषदों के आत्मैकत्ववाद (अद्वैतवाद) से सर्वथा भिन्न है । प्रत्येक शरीर में पृथक्-पृथक् आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने के कारण जैन धर्म द्वैतवाद का पोषक एवं समर्थक है।
इसी परिप्रेक्ष्य में एक तथ्य और भी ध्यातव्य है । छान्दोग्योपजिषद् में २५६
तुलसी प्रश
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org