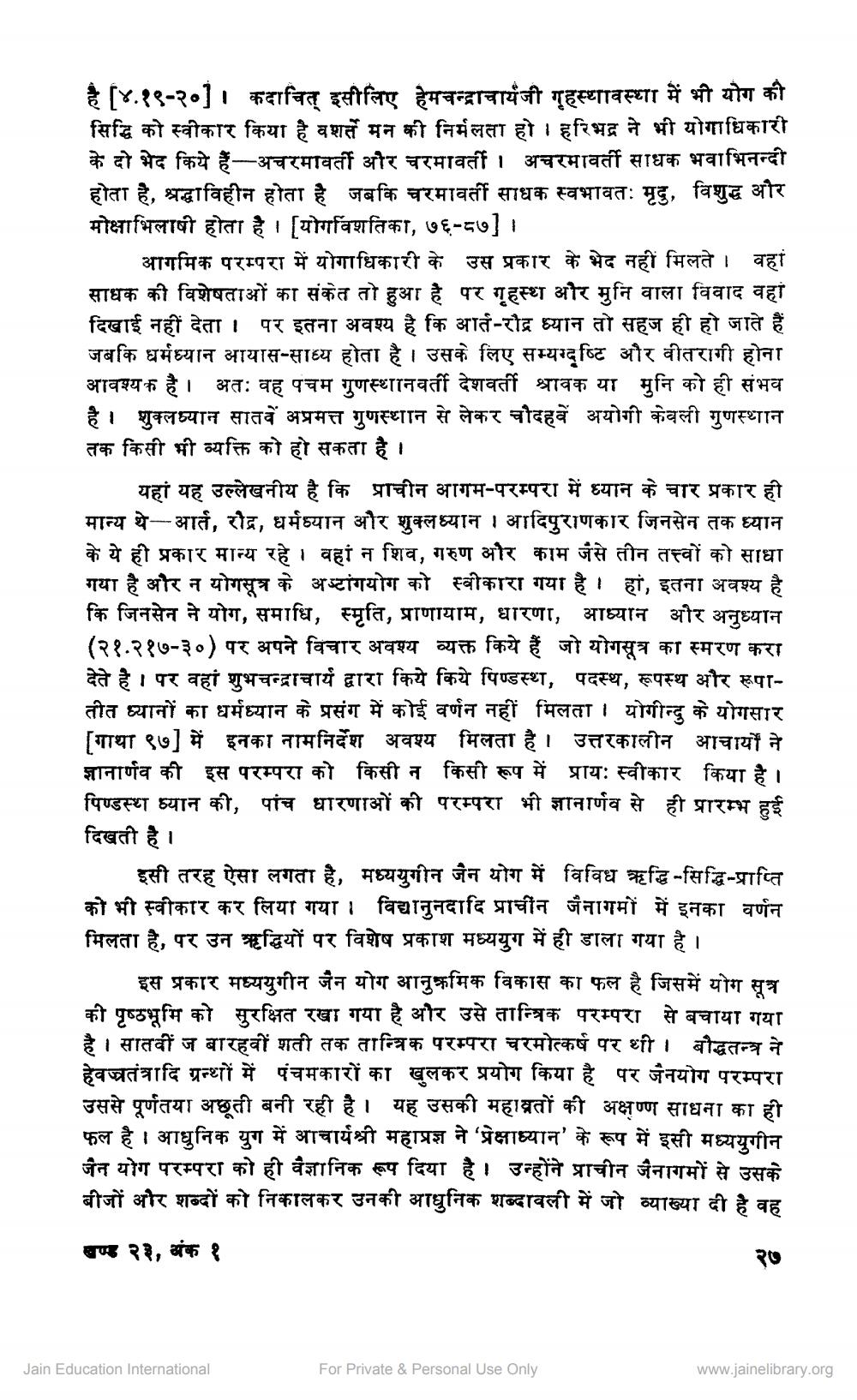________________
है [४.१९-२०] । कदाचित् इसीलिए हेमचन्द्राचार्यजी गृहस्थावस्था में भी योग की सिद्धि को स्वीकार किया है व शर्ते मन की निर्मलता हो । हरिभद्र ने भी योगाधिकारी के दो भेद किये हैं-अचरमावर्ती और चरमावर्ती । अचरमावर्ती साधक भवाभिनन्दी होता है, श्रद्धाविहीन होता है जबकि चरमावर्ती साधक स्वभावतः मृदु, विशुद्ध और मोक्षाभिलाषी होता है । [योगविंशतिका, ७६-८७] ।
आगमिक परम्परा में योगाधिकारी के उस प्रकार के भेद नहीं मिलते। वहां साधक की विशेषताओं का संकेत तो हुआ है पर गृहस्थ और मुनि वाला विवाद वहां दिखाई नहीं देता। पर इतना अवश्य है कि आर्त-रौद्र ध्यान तो सहज ही हो जाते हैं जबकि धर्मध्यान आयास-साध्य होता है। उसके लिए सम्यग्दृष्टि और वीतरागी होना आवश्यक है। अतः वह पचम गुणस्थानवर्ती देशवर्ती श्रावक या मुनि को ही संभव है। शुक्लध्यान सातवें अप्रमत्त गुणस्थान से लेकर चौदहवें अयोगी केवली गुणस्थान तक किसी भी व्यक्ति को हो सकता है ।
___ यहां यह उल्लेखनीय है कि प्राचीन आगम-परम्परा में ध्यान के चार प्रकार ही मान्य थे-आर्त, रोद्र, धर्मध्यान और शुक्लध्यान । आदिपुराणकार जिनसेन तक ध्यान के ये ही प्रकार मान्य रहे। वहां न शिव, गरुण और काम जसे तीन तत्त्वों को साधा गया है और न योगसूत्र के अष्टांगयोग को स्वीकारा गया है। हां, इतना अवश्य है कि जिनसेन ने योग, समाधि, स्मृति, प्राणायाम, धारणा, आध्यान और अनुध्यान (२१.२१७-३०) पर अपने विचार अवश्य व्यक्त किये हैं जो योगसूत्र का स्मरण करा देते है । पर वहां शुभचन्द्राचार्य द्वारा किये किये पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यानों का धर्मध्यान के प्रसंग में कोई वर्णन नहीं मिलता। योगीन्दु के योगसार
गाथा ९७] में इनका नामनिर्देश अवश्य मिलता है। उत्तरकालीन आचार्यों ने ज्ञानार्णव की इस परम्परा को किसी न किसी रूप में प्रायः स्वीकार किया है। पिण्डस्थ ध्यान की, पांच धारणाओं की परम्परा भी ज्ञानार्णव से ही प्रारम्भ हई दिखती है।
इसी तरह ऐसा लगता है, मध्ययुगीन जैन योग में विविध ऋद्धि-सिद्धि-प्राप्ति को भी स्वीकार कर लिया गया। विद्यानुनदादि प्राचीन जैनागमों में इनका वर्णन मिलता है, पर उन ऋद्धियों पर विशेष प्रकाश मध्ययुग में ही डाला गया है।
इस प्रकार मध्ययुगीन जैन योग आनुक्रमिक विकास का फल है जिसमें योग सूत्र की पृष्ठभूमि को सुरक्षित रखा गया है और उसे तान्त्रिक परम्परा से बचाया गया है। सातवीं ज बारहवीं शती तक तान्त्रिक परम्परा चरमोत्कर्ष पर थी। बौद्धतन्त्र ने हेवज्रतंत्रादि ग्रन्थों में पंचमकारों का खुलकर प्रयोग किया है पर जैनयोग परम्परा उससे पूर्णतया अछूती बनी रही है। यह उसकी महाव्रतों की अक्षण्ण साधना का ही फल है । आधुनिक युग में आचार्यश्री महाप्रज्ञ ने 'प्रेक्षाध्यान' के रूप में इसी मध्ययुगीन जैन योग परम्परा को ही वैज्ञानिक रूप दिया है। उन्होंने प्राचीन जैनागमों से उसके बीजों और शब्दों को निकालकर उनकी आधुनिक शब्दावली में जो व्याख्या दी है वह खण्ड २३, अंक १
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org