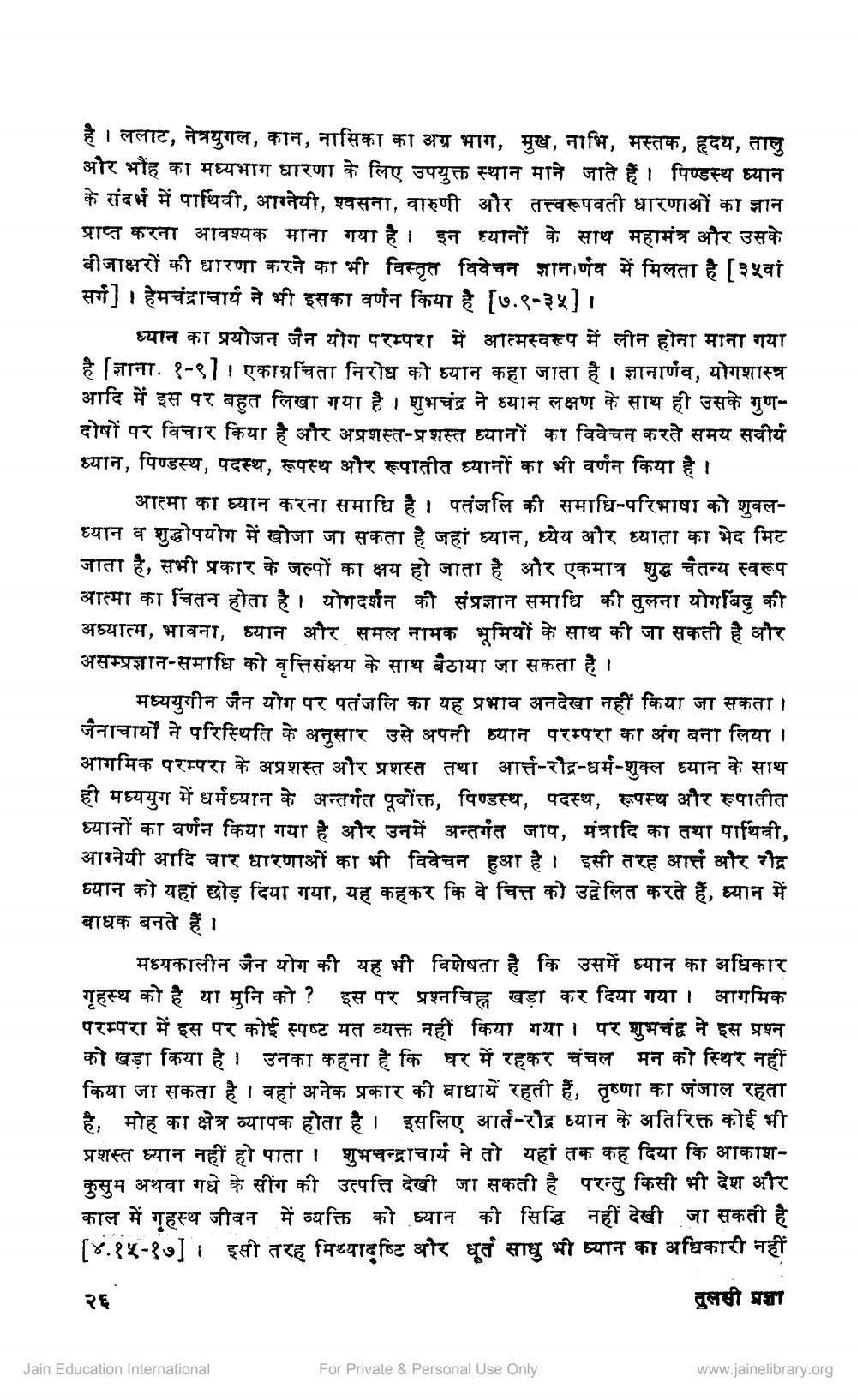________________
है । ललाट, नेत्रयुगल, कान, नासिका का अग्र भाग, मुख, नाभि, मस्तक, हृदय, तालु और भौंह का मध्यभाग धारणा के लिए उपयुक्त स्थान माने जाते हैं। पिण्डस्थ ध्यान के संदर्भ में पार्थिवी, आग्नेयी, श्वसना, वारुणी और तत्त्वरूपवती धारणाओं का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक माना गया है। इन ध्यानों के साथ महामंत्र और उसके बीजाक्षरों की धारणा करने का भी विस्तृत विवेचन ज्ञानार्णव में मिलता है [३५वां सर्ग] । हेमचंद्राचार्य ने भी इसका वर्णन किया है [७.९-३५] ।
ध्यान का प्रयोजन जैन योग परम्परा में आत्मस्वरूप में लीन होना माना गया है [ज्ञाना. १-९] । एकाग्रचिंता निरोध को ध्यान कहा जाता है । ज्ञानार्णव, योगशास्त्र आदि में इस पर बहुत लिखा गया है । शुभचंद्र ने ध्यान लक्षण के साथ ही उसके गुणदोषों पर विचार किया है और अप्रशस्त-प्रशस्त ध्यानों का विवेचन करते समय सवीर्य ध्यान, पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यानों का भी वर्णन किया है।
आत्मा का ध्यान करना समाधि है। पतंजलि की समाधि-परिभाषा को शुक्लध्यान व शुद्धोपयोग में खोजा जा सकता है जहां ध्यान, ध्येय और ध्याता का भेद मिट जाता है, सभी प्रकार के जल्पों का क्षय हो जाता है और एकमात्र शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा का चितन होता है। योगदर्शन की संप्रज्ञान समाधि की तुलना योगबिंदु की अध्यात्म, भावना, ध्यान और समल नामक भूमियों के साथ की जा सकती है और असम्प्रज्ञान-समाधि को वृत्तिसंक्षय के साथ बैठाया जा सकता है ।
मध्ययुगीन जैन योग पर पतंजलि का यह प्रभाव अनदेखा नहीं किया जा सकता। जैनाचार्यों ने परिस्थिति के अनुसार उसे अपनी ध्यान परम्परा का अंग बना लिया । आगमिक परम्परा के अप्रशस्त और प्रशस्त तथा आर्त्त-रौद्र-धर्म-शुक्ल ध्यान के साथ ही मध्ययुग में धर्मध्यान के अन्तर्गत पूर्वोक्त, पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यानों का वर्णन किया गया है और उनमें अन्तर्गत जाप, मंत्रादि का तथा पार्थिवी, आग्नेयी आदि चार धारणाओं का भी विवेचन हुआ है। इसी तरह आर्त और रौद्र ध्यान को यहां छोड़ दिया गया, यह कहकर कि वे चित्त को उद्वेलित करते हैं, ध्यान में बाधक बनते हैं।
मध्यकालीन जैन योग की यह भी विशेषता है कि उसमें ध्यान का अधिकार गृहस्थ को है या मुनि को? इस पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया गया। आगमिक परम्परा में इस पर कोई स्पष्ट मत व्यक्त नहीं किया गया। पर शुभचंद ने इस प्रश्न को खड़ा किया है। उनका कहना है कि घर में रहकर चंचल मन को स्थिर नहीं किया जा सकता है । वहां अनेक प्रकार की बाधायें रहती हैं, तृष्णा का जंजाल रहता है, मोह का क्षेत्र व्यापक होता है। इसलिए आर्त-रौद्र ध्यान के अतिरिक्त कोई भी प्रशस्त ध्यान नहीं हो पाता। शुभचन्द्राचार्य ने तो यहां तक कह दिया कि आकाशकुसुम अथवा गधे के सींग की उत्पत्ति देखी जा सकती है परन्तु किसी भी देश और काल में गृहस्थ जीवन में व्यक्ति को ध्यान की सिद्धि नहीं देखी जा सकती है [४.१५-१७] । इसी तरह मिथ्यादष्टि और धूर्त साधु भी ध्यान का अधिकारी नहीं २६
तुलसी प्रशा
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org