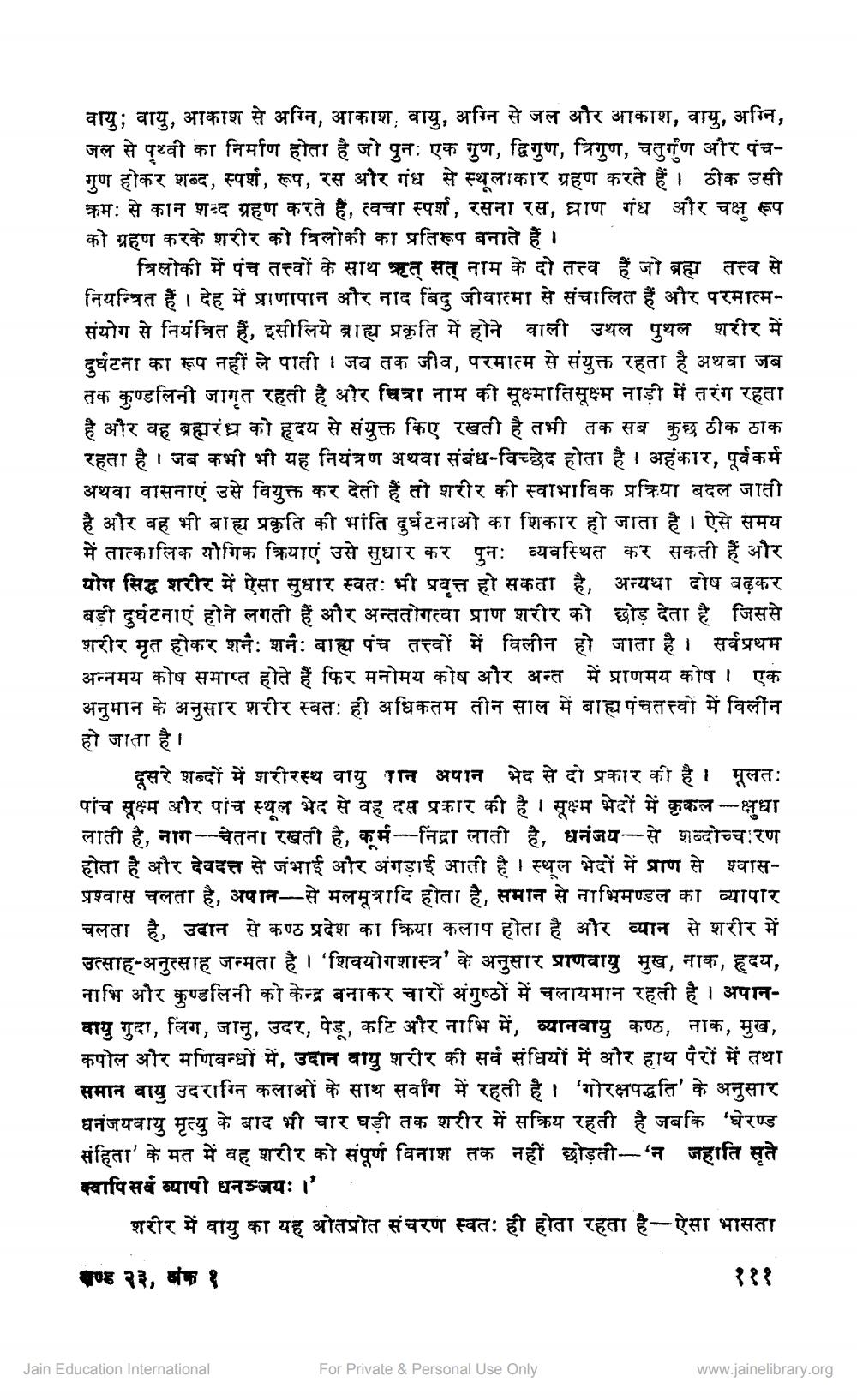________________
वायु; वायु, आकाश से अग्नि, आकाश, वायु, अग्नि से जल और आकाश, वायु, अग्नि, जल से पृथ्वी का निर्माण होता है जो पुनः एक गुण, द्विगुण, त्रिगुण, चतुर्गुण और पंचगुण होकर शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से स्थूलाकार ग्रहण करते हैं। ठीक उसी क्रमः से कान शब्द ग्रहण करते हैं, त्वचा स्पर्श, रसना रस, घ्राण गंध और चक्षु रूप को ग्रहण करके शरीर को त्रिलोकी का प्रतिरूप बनाते हैं ।
त्रिलोकी में पंच तत्त्वों के साथ ऋत् सत् नाम के दो तत्त्व हैं जो ब्रह्म तत्त्व से नियन्त्रित हैं । देह में प्राणापान और नाद बिंदु जीवात्मा से संचालित हैं और परमात्मसंयोग नियंत्रित हैं, इसीलिये ब्राह्म प्रकृति में होने वाली उथल पुथल शरीर में दुर्घटना का रूप नहीं ले पाती । जब तक जीव, परमात्म से संयुक्त रहता है अथवा जब तक कुण्डलिनी जागृत रहती है और चित्रा नाम की सूक्ष्मातिसूक्ष्म नाड़ी तरंग रहता है और वह ब्रह्मरंध्र को हृदय से संयुक्त किए रखती है तभी तक सब कुछ ठीक ठाक रहता है । जब कभी भी यह नियंत्रण अथवा संबंध विच्छेद होता है । अहंकार, पूर्व कर्म अथवा वासनाएं उसे वियुक्त कर देती हैं तो शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया बदल जाती है और वह भी बाह्य प्रकृति की भांति दुर्घटनाओ का शिकार हो जाता है । ऐसे समय तात्कालिक यौगिक क्रियाएं उसे सुधार कर पुनः व्यवस्थित कर सकती हैं और योग सिद्ध शरीर में ऐसा सुधार स्वतः भी प्रवृत्त हो सकता है, अन्यथा दोष बढ़कर बड़ी दुर्घटनाएं होने लगती हैं और अन्ततोगत्वा प्राण शरीर को छोड़ देता है जिससे शरीर मृत होकर शनैः शनैः बाह्य पंच तत्त्वों में विलीन हो जाता है । सर्वप्रथम अन्नमय कोष समाप्त होते हैं फिर मनोमय कोष और अन्त में प्राणमय कोष । एक अनुमान के अनुसार शरीर स्वतः ही अधिकतम तीन साल में बाह्य पंचतत्त्वों में विलीन हो जाता है ।
दूसरे शब्दों में शरीरस्थ वायु पान अपान भेद से दो प्रकार की है । मूलत: पांच सूक्ष्म और पांच स्थूल भेद से वह दस प्रकार की है। सूक्ष्म भेदों में कृकल - क्षुधा लाती है, नाग - चेतना रखती है, कूर्म - निद्रा लाती है, धनंजय - से शब्दोच्चारण होता है और देवदत्त से जंभाई और अंगड़ाई आती है । स्थूल भेदों में प्राण से श्वासप्रश्वास चलता है, अपान - से मलमूत्रादि होता है, समान से नाभिमण्डल का व्यापार चलता है, उदान से कण्ठ प्रदेश का क्रिया कलाप होता है और व्यान से शरीर में उत्साह-अनुत्साह जन्मता है । 'शिवयोगशास्त्र' के अनुसार प्राणवायु मुख, नाक, हृदय, नाभि और कुण्डलिनी को केन्द्र बनाकर चारों अंगुष्ठों में चलायमान रहती है । अपानवायु गुदा, लिंग, जानु, उदर, पेडू, कटि और नाभि में, व्यानवायु कण्ठ, नाक, मुख, कपोल और मणिबन्धों में, उदान वायु शरीर की सर्व संधियों में और हाथ पैरों में तथा समान वायु उदराग्नि कलाओं के साथ सर्वांग में रहती है । 'गोरक्षपद्धति' के अनुसार धनंजयवायु मृत्यु के बाद भी चार घड़ी तक शरीर में सक्रिय रहती है जबकि 'घेरण्ड संहिता' के मत में वह शरीर को संपूर्ण विनाश तक नहीं छोड़ती- 'न जहाति सृते क्वापि सर्व व्यापी धनञ्जयः ।'
शरीर में वायु का यह ओतप्रोत संचरण स्वतः ही होता रहता है-ऐसा भासता
खण्ड २३, अंक १
१११
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org