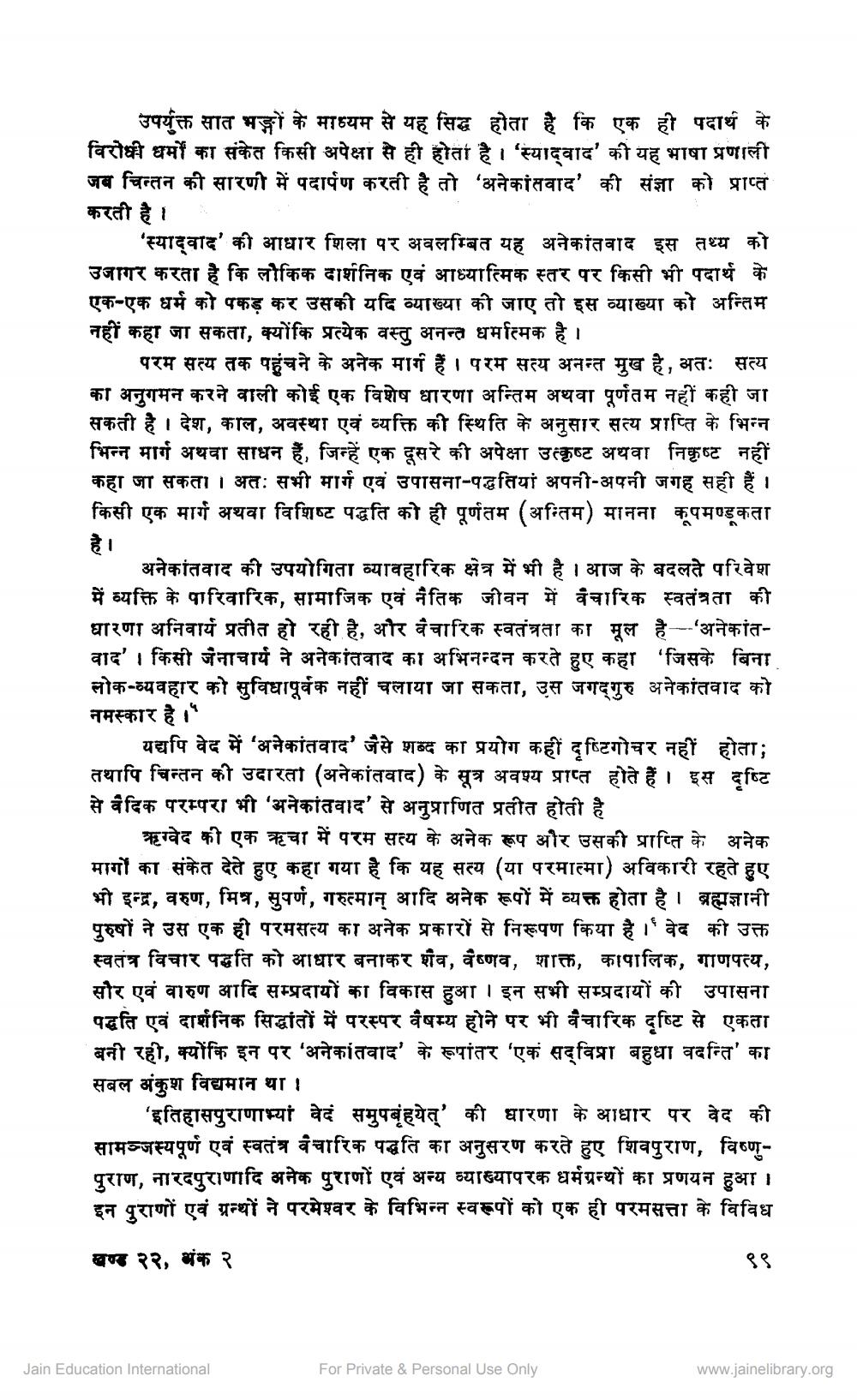________________
उपर्युक्त सात भङ्गों के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि एक ही पदार्थ के विरोधी धर्मों का संकेत किसी अपेक्षा से ही होता है । 'स्याद्वाद' की यह भाषा प्रणाली जब चिन्तन की सारणी में पदार्पण करती है तो 'अनेकांतवाद' की संज्ञा को प्राप्त करती है।
___ 'स्याद्वाद' की आधार शिला पर अवलम्बित यह अनेकांतवाद इस तथ्य को उजागर करता है कि लौकिक दार्शनिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर किसी भी पदार्थ के एक-एक धर्म को पकड़ कर उसकी यदि व्याख्या की जाए तो इस व्याख्या को अन्तिम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अनन्त धर्मात्मक है।
परम सत्य तक पहुंचने के अनेक मार्ग हैं । परम सत्य अनन्त मुख है, अतः सत्य का अनुगमन करने वाली कोई एक विशेष धारणा अन्तिम अथवा पूर्णतम नहीं कही जा सकती है । देश, काल, अवस्था एवं व्यक्ति की स्थिति के अनुसार सत्य प्राप्ति के भिन्न भिन्न मार्ग अथवा साधन हैं, जिन्हें एक दूसरे की अपेक्षा उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट नहीं कहा जा सकता। अत: सभी मार्ग एवं उपासना-पद्धतियां अपनी-अपनी जगह सही हैं। किसी एक मार्ग अथवा विशिष्ट पद्धति को ही पूर्णतम (अन्तिम) मानना कूपमण्डूकता
__ अनेकांतवाद की उपयोगिता व्यावहारिक क्षेत्र में भी है। आज के बदलते परिवेश में व्यक्ति के पारिवारिक, सामाजिक एवं नैतिक जीवन में वैचारिक स्वतंत्रता की धारणा अनिवार्य प्रतीत हो रही है, और वैचारिक स्वतंत्रता का मूल है--'अनेकांतवाद' । किसी जैनाचार्य ने अनेकांतवाद का अभिनन्दन करते हुए कहा 'जिसके बिना लोक-व्यवहार को सुविधापूर्वक नहीं चलाया जा सकता, उस जगद्गुरु अनेकांतवाद को नमस्कार है।
यद्यपि वेद में 'अनेकांतवाद' जैसे शब्द का प्रयोग कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता; तथापि चिन्तन की उदारता (अनेकांतवाद) के सूत्र अवश्य प्राप्त होते हैं। इस दृष्टि से वैदिक परम्परा भी 'अनेकांतवाद' से अनुप्राणित प्रतीत होती है
ऋग्वेद की एक ऋचा में परम सत्य के अनेक रूप और उसकी प्राप्ति के अनेक मार्गों का संकेत देते हुए कहा गया है कि यह सत्य (या परमात्मा) अविकारी रहते हुए भी इन्द्र, वरुण, मित्र, सुपर्ण, गरुत्मान् आदि अनेक रूपों में व्यक्त होता है। ब्रह्मज्ञानी पुरुषों ने उस एक ही परमसत्य का अनेक प्रकारों से निरूपण किया है। वेद की उक्त स्वतंत्र विचार पद्धति को आधार बनाकर शैव, वैष्णव, शाक्त, कापालिक, गाणपत्य, सौर एवं वारुण आदि सम्प्रदायों का विकास हुआ । इन सभी सम्प्रदायों की उपासना पद्धति एवं दार्शनिक सिद्धांतों में परस्पर वैषम्य होने पर भी वैचारिक दृष्टि से एकता बनी रही, क्योंकि इन पर 'अनेकांतवाद' के रूपांतर 'एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति' का सबल अंकुश विद्यमान था।
'इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपद्व्हयेत्' की धारणा के आधार पर वेद की सामञ्जस्यपूर्ण एवं स्वतंत्र वैचारिक पद्धति का अनुसरण करते हुए शिवपुराण, विष्णुपुराण, नारदपुराणादि अनेक पुराणों एवं अन्य व्याख्यापरक धर्मग्रन्थों का प्रणयन हुआ। इन पुराणों एवं ग्रन्थों ने परमेश्वर के विभिन्न स्वरूपों को एक ही परमसत्ता के विविध
खण्ड २२, अंक २
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org