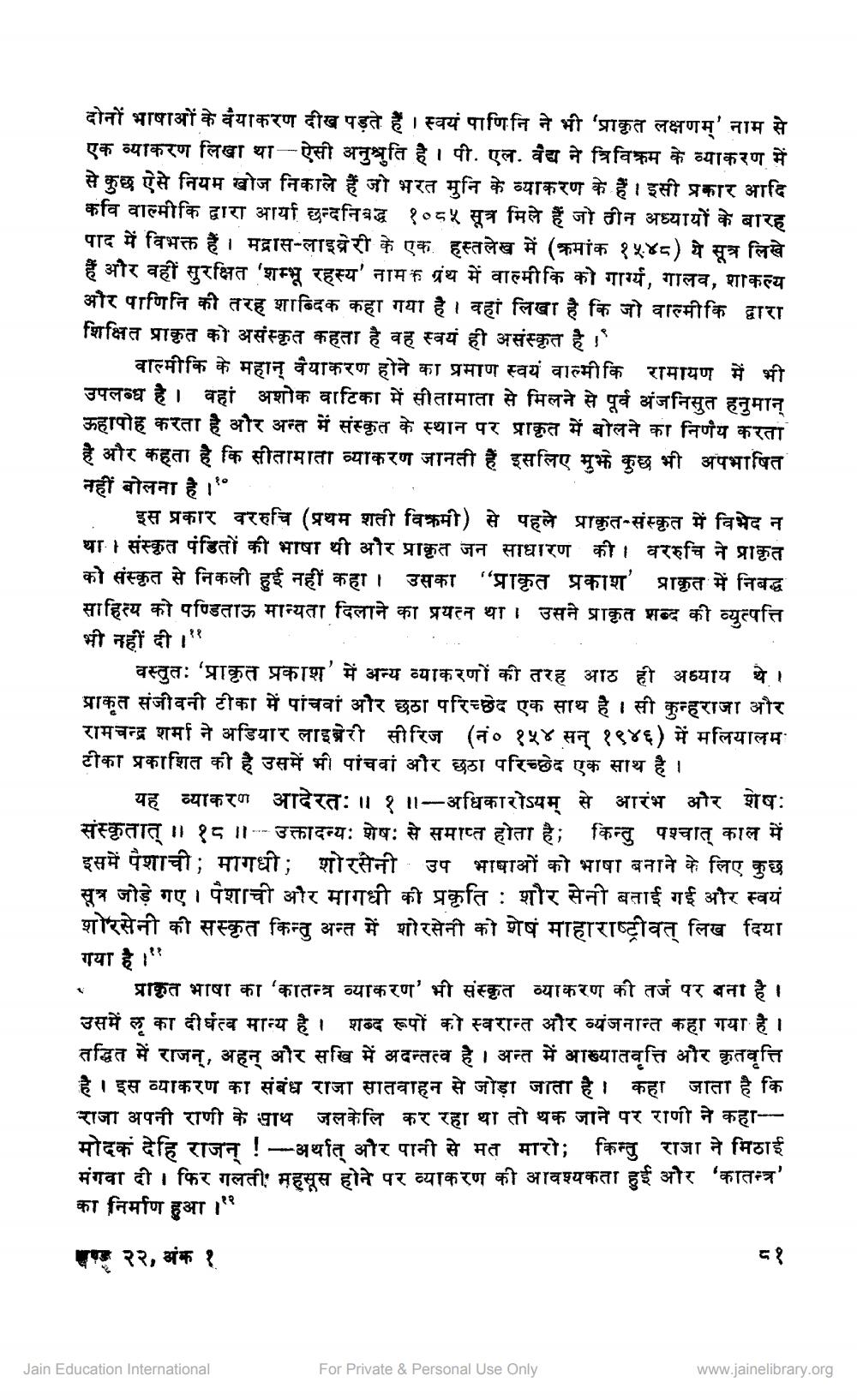________________
दोनों भाषाओं के वैयाकरण दीख पड़ते हैं । स्वयं पाणिनि ने भी 'प्राकृत लक्षणम्' नाम से एक व्याकरण लिखा था-ऐसी अनुश्रुति है । पी. एल. वैद्य ने त्रिविक्रम के व्याकरण में से कुछ ऐसे नियम खोज निकाले हैं जो भरत मुनि के व्याकरण के हैं। इसी प्रकार आदि कवि वाल्मीकि द्वारा आर्या छन्दनिबद्ध १०८५ सूत्र मिले हैं जो तीन अध्यायों के बारह पाद में विभक्त हैं। मद्रास-लाइब्रेरी के एक हस्तलेख में (क्रमांक १५.४८) ये सूत्र लिखे हैं और वहीं सुरक्षित 'शम्भू रहस्य' नामक ग्रंथ में वाल्मीकि को गार्य, गालव, शाकल्य
और पाणिनि की तरह शाब्दिक कहा गया है। वहां लिखा है कि जो वाल्मीकि द्वारा शिक्षित प्राकृत को असंस्कृत कहता है वह स्वयं ही असंस्कृत है।
वाल्मीकि के महान् वैयाकरण होने का प्रमाण स्वयं वाल्मीकि रामायण में भी उपलब्ध है। वहां अशोक वाटिका में सीतामाता से मिलने से पूर्व अंजनिसुत हनुमान ऊहापोह करता है और अन्त में संस्कृत के स्थान पर प्राकृत में बोलने का निर्णय करता है और कहता है कि सीतामाता व्याकरण जानती हैं इसलिए मुझे कुछ भी अपभाषित नहीं बोलना है।
इस प्रकार वररुचि (प्रथम शती विक्रमी) से पहले प्राकृत-संस्कृत में विभेद न था। संस्कृत पंडितों की भाषा थी और प्राकृत जन साधारण की। वररुचि ने प्राकृत को संस्कृत से निकली हुई नहीं कहा। उसका "प्राकृत प्रकाश' प्राकृत में निबद्ध साहित्य को पण्डिताऊ मान्यता दिलाने का प्रयत्न था। उसने प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति भी नहीं दी।
वस्तुतः 'प्राकृत प्रकाश' में अन्य व्याकरणों की तरह आठ ही अध्याय थे। प्राकृत संजीवनी टीका में पांचवां और छठा परिच्छेद एक साथ है । सी कुन्हराजा और रामचन्द्र शर्मा ने अडियार लाइब्रेरी सीरिज (नं० १५४ सन् १९४६) में मलियालम टीका प्रकाशित की है उसमें भी पांचवां और छठा परिच्छेद एक साथ है।
यह व्याकरण आदेरतः ॥ १॥-अधिकारोऽयम् से आरंभ और शेषः संस्कृतात् ॥ १८ ॥-- उक्तादन्यः शेषः से समाप्त होता है; किन्तु पश्चात् काल में इसमें पैशाची; मागधी; शोरसेनी उप भाषाओं को भाषा बनाने के लिए कुछ सूत्र जोड़े गए। पैशाची और मागधी की प्रकृति : शौर सेनी बताई गई और स्वयं शोरसेनी की सस्कृत किन्तु अन्त में शोरसेनी को शेषं माहाराष्ट्रीवत् लिख दिया गया है। । प्राकृत भाषा का 'कातन्त्र व्याकरण' भी संस्कृत व्याकरण की तर्ज पर बना है। उसमें ल का दीर्घत्व मान्य है। शब्द रूपों को स्वरान्त और व्यंजनान्त कहा गया है । तद्धित में राजन्, अहन और सखि में अदन्तत्व है । अन्त में आख्यातवृत्ति और कृतवृत्ति है । इस व्याकरण का संबंध राजा सातवाहन से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि राजा अपनी राणी के साथ जलकेलि कर रहा था तो थक जाने पर राणी ने कहामोदकं देहि राजन् !-अर्थात् और पानी से मत मारो; किन्तु राजा ने मिठाई मंगवा दी। फिर गलती महसूस होने पर व्याकरण की आवश्यकता हुई और 'कातन्त्र' का निर्माण हुआ।
पण्ड २२, अंक १
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org