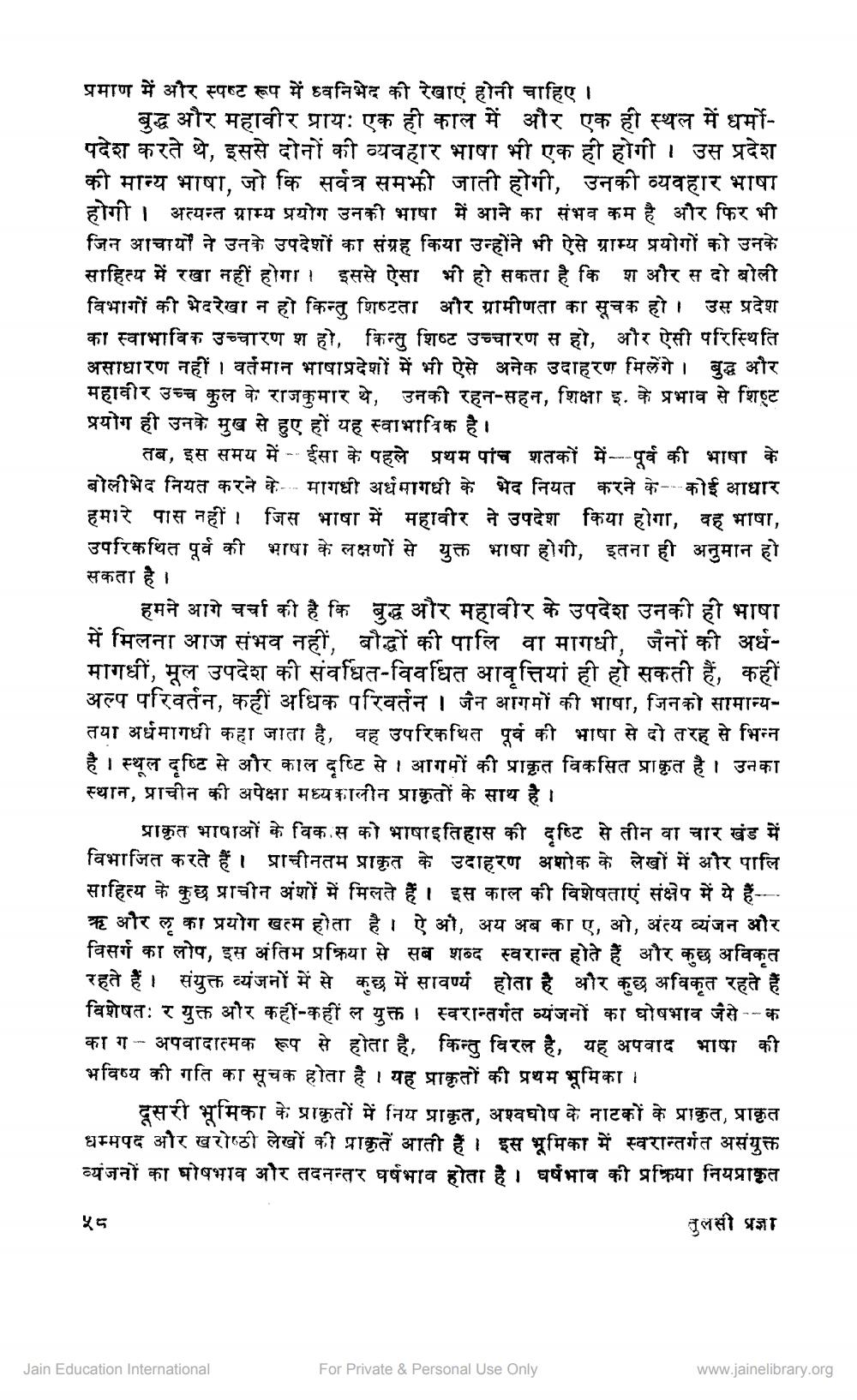________________
प्रमाण में और स्पष्ट रूप में ध्वनिभेद की रेखाएं होनी चाहिए ।
बुद्ध और महावीर प्रायः एक ही काल में और एक ही स्थल में धर्मोपदेश करते थे, इससे दोनों की व्यवहार भाषा भी एक ही होगी । उस प्रदेश की मान्य भाषा, जो कि सर्वत्र समझी जाती होगी, उनकी व्यवहार भाषा होगी । अत्यन्त ग्राम्य प्रयोग उनकी भाषा में आने का संभव कम है और फिर भी जिन आचार्यों ने उनके उपदेशों का संग्रह किया उन्होंने भी ऐसे ग्राम्य प्रयोगों को उनके साहित्य में रखा नहीं होगा । इससे ऐसा भी हो सकता है कि श और स दो बोली विभागों की भेदरेखा न हो किन्तु शिष्टता और ग्रामीणता का सूचक हो । उस प्रदेश का स्वाभाविक उच्चारण श हो, किन्तु शिष्ट उच्चारण स हो, और ऐसी परिस्थिति असाधारण नहीं | वर्तमान भाषाप्रदेशों में भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे । बुद्ध और महावीर उच्च कुल के राजकुमार थे, उनकी रहन-सहन, शिक्षा इ. के प्रभाव से शिष्ट प्रयोग ही उनके मुख से हुए हों यह स्वाभाविक है ।
तब इस समय में -- ईसा के पहले प्रथम पांच शतकों में बोलीभेद नियत करने के मागधी अर्धमागधी के भेद नियत हमारे पास नहीं । जिस भाषा में महावीर ने उपदेश उपरिकथित पूर्व की भाषा के लक्षणों से युक्त भाषा होगी, सकता है ।
हमने आगे चर्चा की है कि बुद्ध और महावीर के उपदेश उनकी ही भाषा में मिलना आज संभव नहीं, बौद्धों की पालि वा मागधी, जैनों की अर्धमागधी, मूल उपदेश की संवर्धित - विवधित आवृत्तियां ही हो सकती हैं, कहीं अल्प परिवर्तन, कहीं अधिक परिवर्तन । जैन आगमों की भाषा, जिनको सामान्यतथा अर्धमागधी कहा जाता है, वह उपरिकथित पूर्व की भाषा से दो तरह से भिन्न है । स्थूल दृष्टि से और काल दृष्टि से । आगमों की प्राकृत विकसित प्राकृत है । उनका स्थान, प्राचीन की अपेक्षा मध्यकालीन प्राकृतों के साथ है ।
प्राकृत भाषाओं के विकास को भाषा इतिहास की दृष्टि से तीन वा चार खंड में विभाजित करते हैं । प्राचीनतम प्राकृत के उदाहरण अशोक के लेखों में और पालि साहित्य के कुछ प्राचीन अंशों में मिलते हैं । इस काल की विशेषताएं संक्षेप में ये हैंऋ और लू का प्रयोग खत्म होता है । ऐ ओ, अय अब का ए, ओ, अंत्य व्यंजन और विसर्ग का लोप इस अंतिम प्रक्रिया से सब शब्द स्वरान्त होते हैं और कुछ अविकृत
,
रहते हैं । संयुक्त व्यंजनों में से कुछ में सावर्ण्य होता है और कुछ अविकृत रहते हैं विशेषतः र युक्त और कहीं-कहीं ल युक्त । स्वरान्तर्गत व्यंजनों का घोषभाव जैसे --- क का ग -- अपवादात्मक रूप से होता है, किन्तु विरल है, यह अपवाद भाषा की भविष्य की गति का सूचक होता है । यह प्राकृतों की प्रथम भूमिका ।
पूर्व की भाषा के कोई आधार
करने के किया होगा, इतना ही अनुमान हो
वह भाषा,
दूसरी भूमिका के प्राकृतों में निय प्राकृत, अश्वघोष के नाटकों के प्राकृत, प्राकृत धम्मपद और खरोष्ठी लेखों की प्राकृतें आती हैं। इस भूमिका में स्वरान्तर्गत असंयुक्त व्यंजनों का घोषभाव और तदनन्तर घर्षभाव होता है । घर्षभाव की प्रक्रिया नियप्राकृत
तुलसी प्रज्ञा
५८
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org