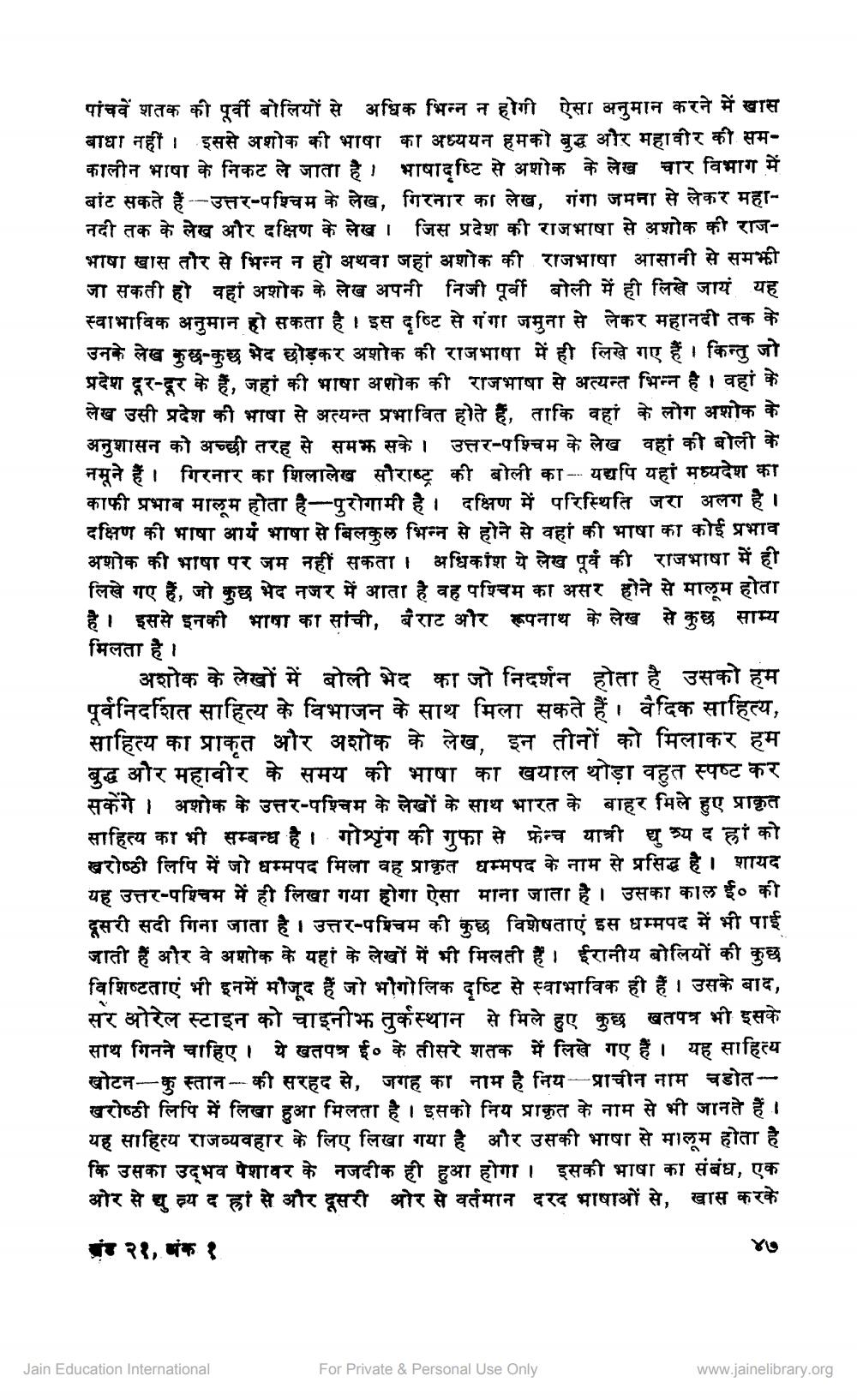________________
पांचवें शतक की पूर्वी बोलियों से अधिक भिन्न न होगी ऐसा अनुमान करने में खास बाधा नहीं। इससे अशोक की भाषा का अध्ययन हमको बुद्ध और महावीर की समकालीन भाषा के निकट ले जाता है। भाषादृष्टि से अशोक के लेख चार विभाग में बांट सकते हैं --उत्तर-पश्चिम के लेख, गिरनार का लेख, गंगा जमना से लेकर महानदी तक के लेख और दक्षिण के लेख । जिस प्रदेश की राजभाषा से अशोक की राजभाषा खास तौर से भिन्न न हो अथवा जहां अशोक की राजभाषा आसानी से समझी जा सकती हो वहां अशोक के लेख अपनी निजी पूर्वी बोली में ही लिखे जायं यह स्वाभाविक अनुमान हो सकता है। इस दृष्टि से गंगा जमुना से लेकर महानदी तक के उनके लेख कुछ-कुछ भेद छोड़कर अशोक की राजभाषा में ही लिखे गए हैं। किन्तु जो प्रदेश दूर-दूर के हैं, जहां की भाषा अशोक की राजभाषा से अत्यन्त भिन्न है। वहां के लेख उसी प्रदेश की भाषा से अत्यन्त प्रभावित होते हैं, ताकि वहां के लोग अशोक के अनुशासन को अच्छी तरह से समझ सके। उत्तर-पश्चिम के लेख वहां की बोली के नमूने हैं। गिरनार का शिलालेख सौराष्ट्र की बोली का-- यद्यपि यहां मध्यदेश का काफी प्रभाब मालूम होता है-पुरोगामी है। दक्षिण में परिस्थिति जरा अलग है । दक्षिण की भाषा आर्य भाषा से बिलकुल भिन्न से होने से वहां की भाषा का कोई प्रभाव अशोक की भाषा पर जम नहीं सकता। अधिकांश ये लेख पूर्व की राजभाषा में ही लिखे गए हैं, जो कुछ भेद नजर में आता है वह पश्चिम का असर होने से मालूम होता है। इससे इनकी भाषा का सांची, बैराट और रूपनाथ के लेख से कुछ साम्य मिलता है।
अशोक के लेखों में बोली भेद का जो निदर्शन होता है उसको हम पूर्वनिदर्शित साहित्य के विभाजन के साथ मिला सकते हैं। वैदिक साहित्य, साहित्य का प्राकृत और अशोक के लेख, इन तीनों को मिलाकर हम बुद्ध और महावीर के समय की भाषा का खयाल थोड़ा वहुत स्पष्ट कर सकेंगे। अशोक के उत्तर-पश्चिम के लेखों के साथ भारत के बाहर मिले हुए प्राकृत साहित्य का भी सम्बन्ध है। गोश्रृंग की गुफा से फ्रेन्च यात्री धु य द ह्रां को खरोष्ठी लिपि में जो धम्मपद मिला वह प्राकृत धम्मपद के नाम से प्रसिद्ध है। शायद यह उत्तर-पश्चिम में ही लिखा गया होगा ऐसा माना जाता है। उसका काल ई० की दूसरी सदी गिना जाता है। उत्तर-पश्चिम की कुछ विशेषताएं इस धम्मपद में भी पाई जाती हैं और वे अशोक के यहां के लेखों में भी मिलती हैं। ईरानीय बोलियों की कुछ विशिष्टताएं भी इनमें मौजूद हैं जो भौगोलिक दृष्टि से स्वाभाविक ही हैं। उसके बाद, सर ओरेल स्टाइन को चाइनीझ तुर्कस्थान से मिले हुए कुछ खतपत्र भी इसके साथ गिनने चाहिए। ये खतपत्र ई. के तीसरे शतक में लिखे गए हैं। यह साहित्य खोटन-कुस्तान --- की सरहद से, जगह का नाम है निय-प्राचीन नाम चडोतखरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ मिलता है । इसको निय प्राकृत के नाम से भी जानते हैं । यह साहित्य राजव्यवहार के लिए लिखा गया है और उसकी भाषा से मालूम होता है कि उसका उद्भव पेशावर के नजदीक ही हुआ होगा। इसकी भाषा का संबंध, एक ओर से घु व्य द ह्रां से और दूसरी ओर से वर्तमान दरद भाषाओं से, खास करके ब्रर २१, अंक १
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org