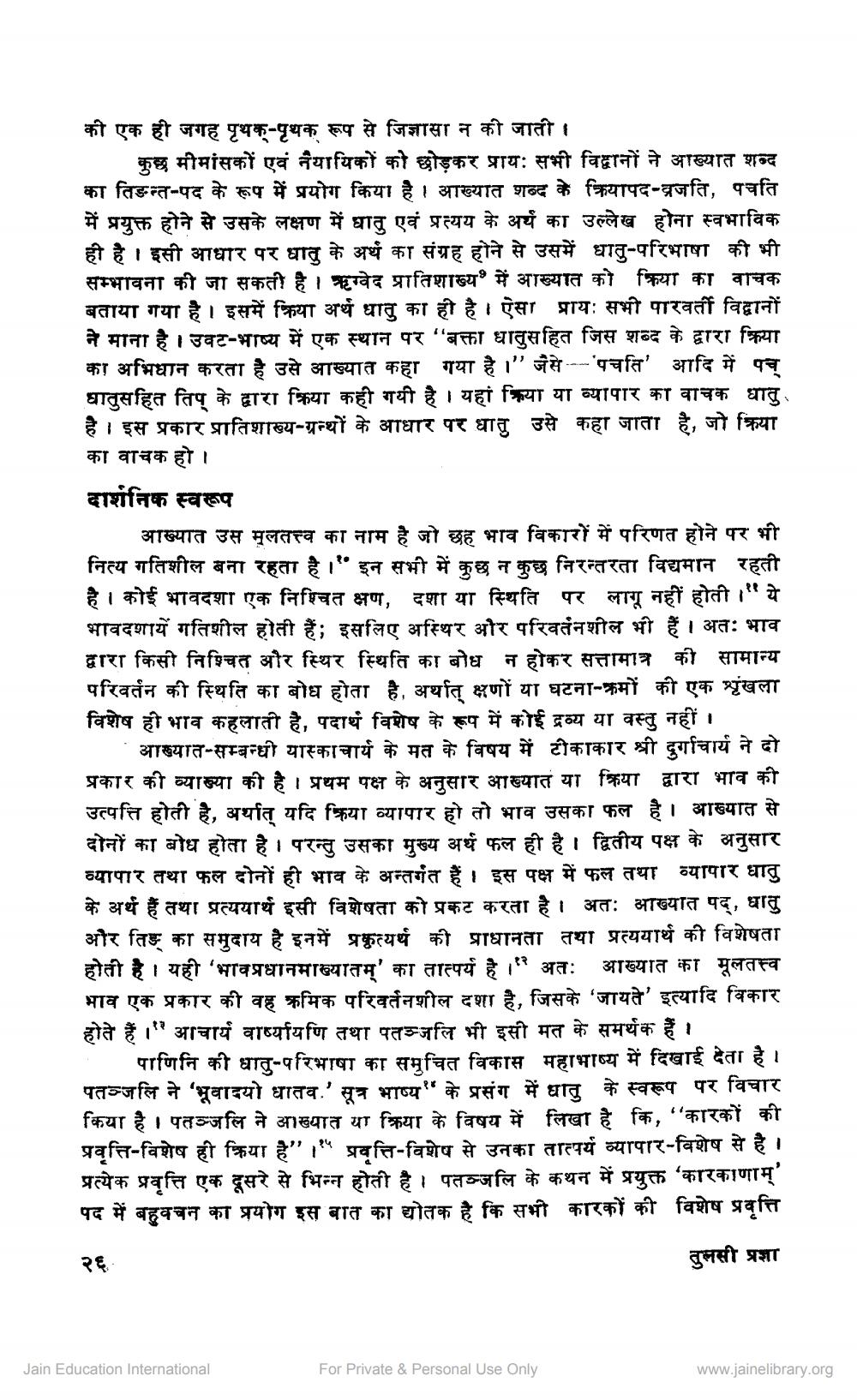________________
की एक ही जगह पृथक्-पृथक रूप से जिज्ञासा न की जाती।
कुछ मीमांसकों एवं नैयायिकों को छोड़कर प्राय: सभी विद्वानों ने आख्यात शब्द का तिङन्त-पद के रूप में प्रयोग किया है। आख्यात शब्द के क्रियापद-व्रजति, पचति में प्रयुक्त होने से उसके लक्षण में धातु एवं प्रत्यय के अर्थ का उल्लेख होना स्वभाविक ही है। इसी आधार पर धातु के अर्थ का संग्रह होने से उसमें धातु-परिभाषा की भी सम्भावना की जा सकती है। ऋग्वेद प्रातिशाख्य' में आख्यात को क्रिया का वाचक बताया गया है। इसमें क्रिया अर्थ धातु का ही है। ऐसा प्रायः सभी पारवर्ती विद्वानों ने माना है । उवट-भाष्य में एक स्थान पर "बक्ता धातुसहित जिस शब्द के द्वारा क्रिया का अभिधान करता है उसे आख्यात कहा गया है।" जैसे ----'पचति' आदि में पच् धातुसहित तिप् के द्वारा क्रिया कही गयी है । यहां क्रिया या व्यापार का वाचक धातु है। इस प्रकार प्रातिशाख्य-ग्रन्थों के आधार पर धातु उसे कहा जाता है, जो क्रिया का वाचक हो। दार्शनिक स्वरूप
आख्यात उस मुलतत्त्व का नाम है जो छह भाव विकारों में परिणत होने पर भी नित्य गतिशील बना रहता है। इन सभी में कुछ न कुछ निरन्तरता विद्यमान रहती है । कोई भावदशा एक निश्चित क्षण, दशा या स्थिति पर लागू नहीं होती।" ये भावदशायें गतिशील होती हैं। इसलिए अस्थिर और परिवर्तनशील भी हैं । अतः भाव द्वारा किसी निश्चित और स्थिर स्थिति का बोध न होकर सत्तामात्र की सामान्य परिवर्तन की स्थिति का बोध होता है, अर्थात् क्षणों या घटना-क्रमों की एक श्रृंखला विशेष ही भाव कहलाती है, पदार्थ विशेष के रूप में कोई द्रव्य या वस्तु नहीं।
' आख्यात-सम्बन्धी यास्काचार्य के मत के विषय में टीकाकार श्री दुर्गाचार्य ने दो प्रकार की व्याख्या की है। प्रथम पक्ष के अनुसार आख्यात या क्रिया द्वारा भाव की उत्पत्ति होती है, अर्थात् यदि क्रिया व्यापार हो तो भाव उसका फल है। आख्यात से दोनों का बोध होता है। परन्तु उसका मुख्य अर्थ फल ही है। द्वितीय पक्ष के अनुसार व्यापार तथा फल दोनों ही भाव के अन्तर्गत हैं। इस पक्ष में फल तथा व्यापार धातु के अर्थ हैं तथा प्रत्ययार्थ इसी विशेषता को प्रकट करता है। अत: आख्यात पद्, धातु और तिङ् का समुदाय है इनमें प्रकृत्यर्थ की प्राधानता तथा प्रत्ययार्थ की विशेषता होती है। यही 'भावप्रधानमाख्यातम्' का तात्पर्य है । अतः आख्यात का मूलतत्त्व भाव एक प्रकार की वह ऋमिक परिवर्तनशील दशा है, जिसके 'जायते' इत्यादि विकार होते हैं । आचार्य वाायणि तथा पतञ्जलि भी इसी मत के समर्थक हैं।
पाणिनि की धातु-परिभाषा का समुचित विकास महाभाष्य में दिखाई देता है । पतञ्जलि ने 'भूवादयो धातव.' सूत्र भाष्य के प्रसंग में धातु के स्वरूप पर विचार किया है । पतञ्जलि ने आख्यात या क्रिया के विषय में लिखा है कि, "कारकों की प्रवृत्ति-विशेष ही क्रिया है"।१५ प्रवत्ति-विशेष से उनका तात्पर्य व्यापार-विशेष से है । प्रत्येक प्रवृत्ति एक दूसरे से भिन्न होती है। पतञ्जलि के कथन में प्रयुक्त 'कारकाणाम्' पद में बहुवचन का प्रयोग इस बात का द्योतक है कि सभी कारकों की विशेष प्रवृत्ति
तुलसी प्रज्ञा
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org