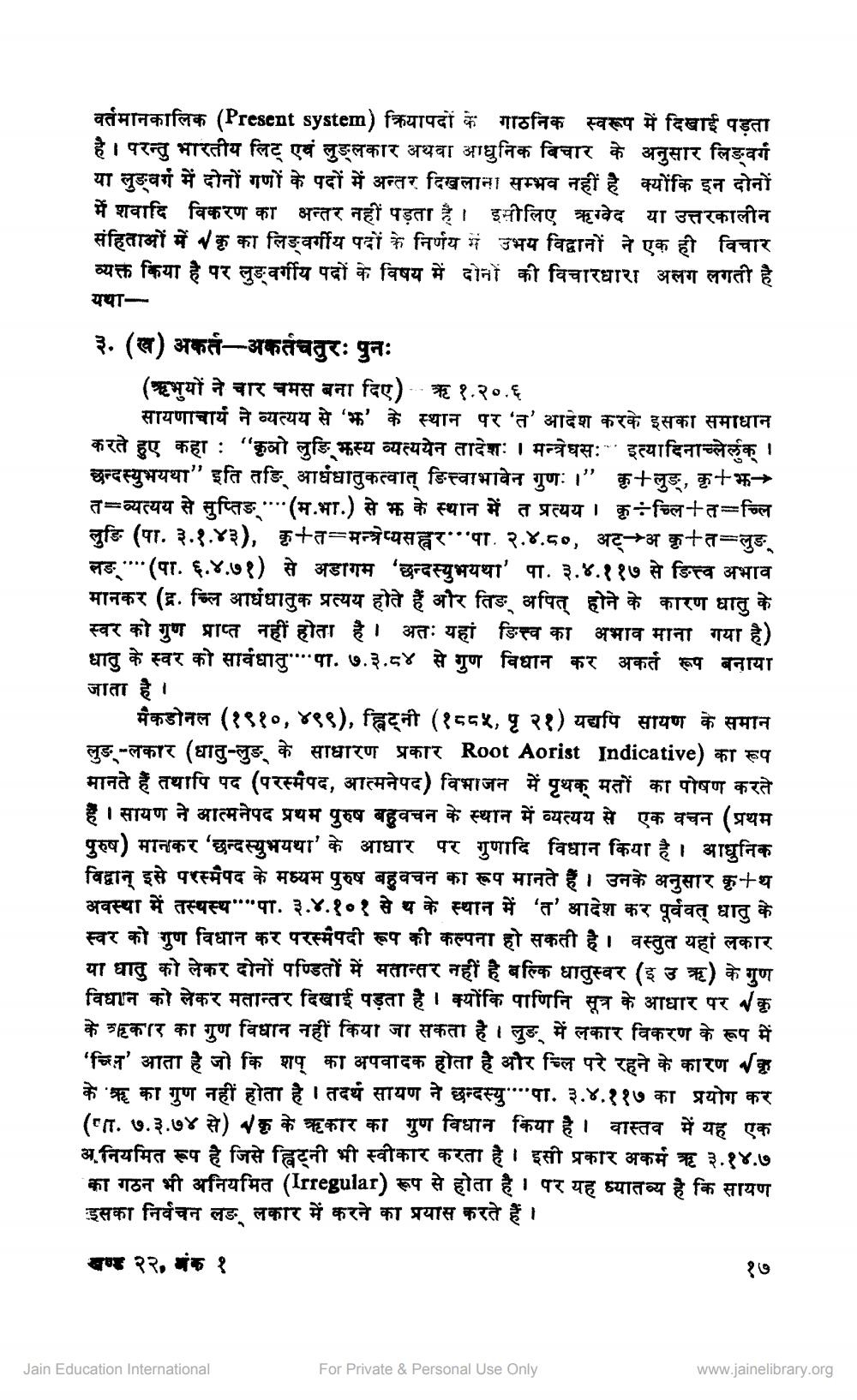________________
अनुसार लिवर्ग
वर्तमानकालिक (Present system) क्रियापदों के गाठनिक स्वरूप में दिखाई पड़ता है । परन्तु भारतीय लिट् एवं लुङ्लकार अथवा आधुनिक विचार के या लुङ्वर्ग में दोनों गणों के पदों में अन्तर दिखलाना सम्भव नहीं है क्योंकि इन दोनों में शवादि विकरण का अन्तर नहीं पड़ता है। इसीलिए ऋग्वेद या उत्तरकालीन संहिताओं में / कृका लिङ्वर्गीय पदों के निर्णय में उभय विद्वानों ने एक ही विचार व्यक्त किया है पर लुङ्वर्गीय पदों के विषय में दोनों की विचारधारा अलग लगती है
यथा
३. (ख) अकर्त - अकर्तचतुरः पुनः
ॠ १.२०.६
इत्यादिनाच्लेर्लुक् । कृ+लुङ्, कृ+झ
।
(ऋभुयों ने चार चमस बना दिए ) सायणाचार्य ने व्यत्यय से 'झ' के स्थान पर 'त' आदेश करके इसका समाधान करते हुए कहा : "कृञो लुङि झस्य व्यत्ययेन तादेशः । मन्त्रेधसः छन्दस्युभयथा" इति तङि आर्धधातुकत्वात् ङित्वाभावेन गुणः ।' त = व्यत्यय से सुप्तिङ . ( म.भा.) से झ के स्थान में त प्रत्यय लुङि (पा. ३.१.४३), कृ + त = मन्त्रेप्यसङ्खर पा. २.४.८०, लङ' (पा. ६.४.७१ ) से अडागम 'छन्दस्युभयथा' पा. ३.४.११७ से ङित्व अभाव मानकर (द्र. ब्लि आर्धधातुक प्रत्यय होते हैं और तिङ अपित् होने के कारण धातु के ङित्व का अभाव माना गया है) विधान कर अकर्त रूप बनाया
कृ : चिल + तच्लि अट्अ कृ + तलुङ
स्वर को गुण प्राप्त नहीं होता है । अतः यहां धातु के स्वर को सार्वधातु पा. ७.३.८४ से गुण जाता है ।
मैकडोनल (१९१०, ४९९), ह्विट्नी (१८८५ पृ २१) यद्यपि सायण समान लुङ - लकार (धातु-लुङ, के साधारण प्रकार Root Aorist Indicative) का रूप मानते हैं तथापि पद ( परस्मैपद, आत्मनेपद ) विभाजन में पृथक् मतों का पोषण करते है । सायण ने आत्मनेपद प्रथम पुरुष बहुवचन के स्थान में व्यत्यय से एक वचन ( प्रथम पुरुष ) मानकर 'छन्दस्युभयथा' के आधार पर गुणादि विधान किया है। आधुनिक विद्वान् इसे परस्मैपद के मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप मानते हैं । उनके अनुसार कृ+थ अवस्था में तस्थस्थ''''पा. ३.४.१०१ से थ के स्थान में 'त' आदेश कर पूर्ववत् धातु के स्वर को गुण विधान कर परस्मैपदी रूप की कल्पना हो सकती है। वस्तुत यहां लकार या धातु को लेकर दोनों पण्डितों में मतान्तर नहीं है बल्कि धातुस्वर ( इ उ ऋ ) के गुण विधान को लेकर मतान्तर दिखाई पड़ता है। क्योंकि पाणिनि सूत्र के आधार पर √ कृ
ऋकार का गुण विधान नहीं किया जा सकता है। लुङ, में लकार विकरण के रूप में 'चिन' आता है जो कि शप् का अपवादक होता है और च्लि परे रहने के कारण √ कृ के ॠ का गुण नहीं होता है । तदर्थ सायण ने छन्दस्यु (पा. ७.३.७४ से ) / कृ के ऋकार का गुण विधान अ. नियमित रूप है जिसे हिट्नी भी स्वीकार करता है। इसी प्रकार अकर्म ऋ ३.१४.७ का गठन भी अनियमित ( Irregular) रूप से होता है । पर यह ध्यातव्य है कि सायण इसका निर्वचन लङ, लकार में करने का प्रयास करते हैं ।
पा. ३.४.११७ का प्रयोग कर किया है । वास्तव में यह एक
खण्ड २२, अंक १
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
१७
www.jainelibrary.org