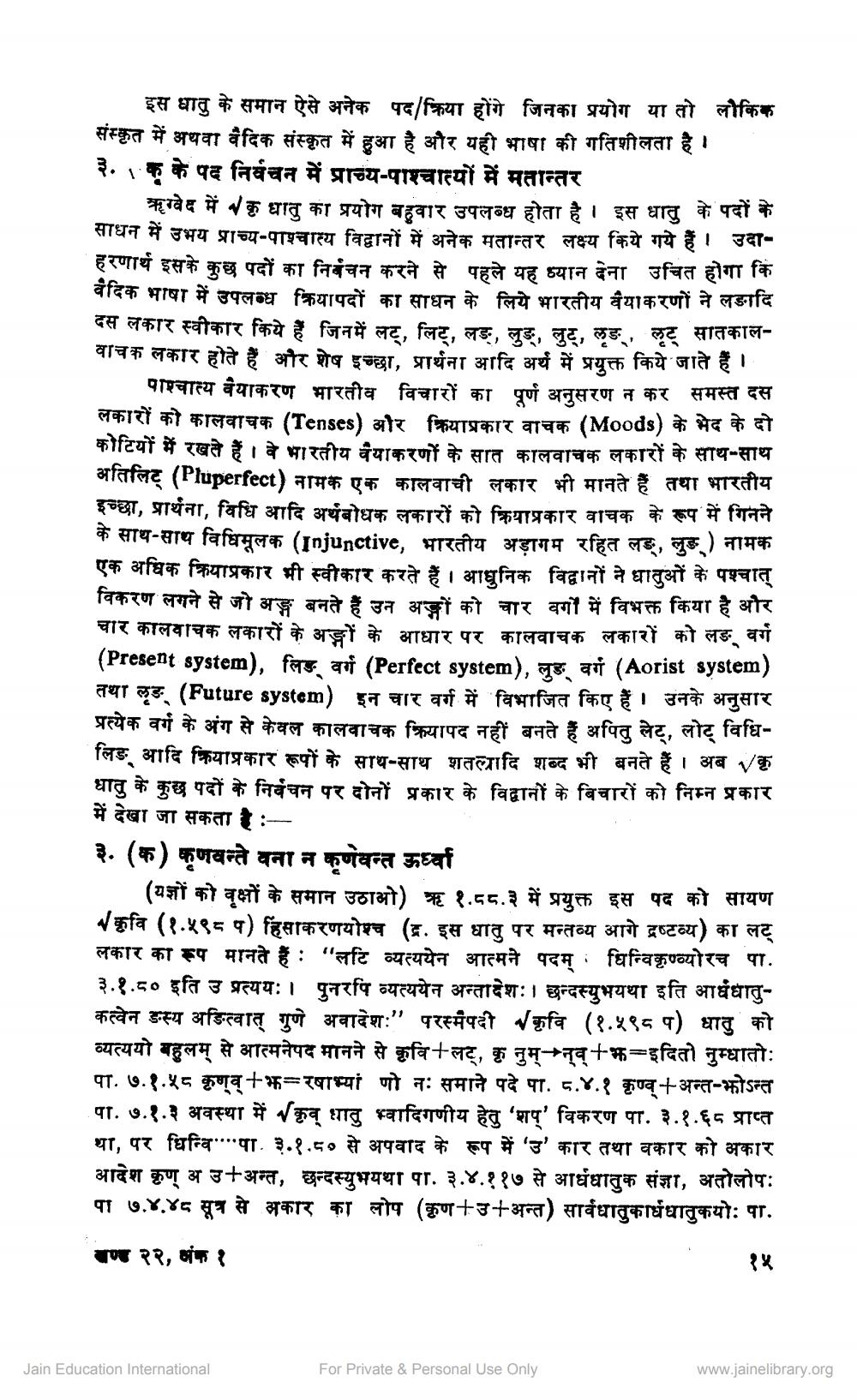________________
इस धातु के समान ऐसे अनेक पद/क्रिया होंगे जिनका प्रयोग या तो लौकिक संस्कृत में अथवा वैदिक संस्कृत में हुआ है और यही भाषा की गतिशीलता है । ३. 1 क के पद निर्वचन में प्राच्य-पाश्चात्यों में मतान्तर
ऋग्वेद में कृ धातु का प्रयोग बहुवार उपलब्ध होता है । इस धातु के पदों के साधन में उभय प्राच्य-पाश्चात्य विद्वानों में अनेक मतान्तर लक्ष्य किये गये हैं। उदाहरणार्थ इसके कुछ पदों का निर्वचन करने से पहले यह ध्यान देना उचित होगा कि वैदिक भाषा में उपलब्ध क्रियापदों का साधन के लिये भारतीय वैयाकरणों ने लङदि दस लकार स्वीकार किये हैं जिनमें लट्, लिट्, लङ, लुङ्, लुट्, लङ, लट् सातकालवाचक लकार होते हैं और शेष इच्छा, प्रार्थना आदि अर्थ में प्रयुक्त किये जाते हैं।
पाश्चात्य वैयाकरण भारतीय विचारों का पूर्ण अनुसरण न कर समस्त दस लकारों को कालवाचक (Tenses) और क्रियाप्रकार वाचक (Moods) के भेद के दो कोटियों में रखते हैं। वे भारतीय वैयाकरणों के सात कालवाचक लकारों के साथ-साथ अतिलिट् (Pluperfect) नामक एक कालवाची लकार भी मानते हैं तथा भारतीय इच्छा, प्रार्थना, विधि आदि अर्थबोधक लकारों को क्रियाप्रकार वाचक के रूप में गिनने के साथ-साथ विधिमूलक (Injunctive, भारतीय अडागम रहित लङ्, लुङ) नामक एक अधिक क्रियाप्रकार भी स्वीकार करते हैं। आधुनिक विद्वानों ने धातुओं के पश्चात् विकरण लगने से जो अङ्ग बनते हैं उन अङ्गों को चार वर्गों में विभक्त किया है और चार कालवाचक लकारों के अङ्गों के आधार पर कालवाचक लकारों को लङ् वर्ग (Present system), लिड वर्ग (Perfect system), लुङ वर्ग (Aorist system) तथा लुङ, (Future system) इन चार वर्ग में विभाजित किए हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ग के अंग से केवल कालवाचक क्रियापद नहीं बनते हैं अपितु लेट, लोट् विधिलिङ आदि क्रियाप्रकार रूपों के साथ-साथ शतलादि शब्द भी बनते हैं । अब VF धातु के कुछ पदों के निर्वचन पर दोनों प्रकार के विद्वानों के विचारों को निम्न प्रकार में देखा जा सकता है:३. (क) कृणवन्ते वना न कृणवन्त ऊर्धा
(यज्ञों को वृक्षों के समान उठाओ) ऋ १.८८.३ में प्रयुक्त इस पद को सायण कृवि (१.५९८ ५) हिंसाकरणयोश्च (द्र. इस धातु पर मन्तव्य आगे द्रष्टव्य) का लट् लकार का रूप मानते हैं : "लटि व्यत्ययेन आत्मने पदम् । धिन्विकृण्व्योरच पा. ३.१.८० इति उ प्रत्ययः। पुनरपि व्यत्ययेन अन्तादेशः। छन्दस्युभयथा इति आर्धधातुकत्वेन डस्य अङित्वात् गुणे अवादेशः" परस्मैपदी कृिवि (१.५९८ प) धातु को व्यत्ययो बहुलम् से आत्मनेपद मानने से कृवि+लट्, कृ नुम्+व+म-इदितो नुम्धातोः पा. ७.१.५८ कृण्व+झरषाभ्यां णो नः समाने पदे पा. ८.४.१ कृण्व+अन्त-झोऽन्त पा. ७.१.३ अवस्था में कृित् धातु भ्वादिगणीय हेतु 'शप्' विकरण पा. ३.१.६८ प्राप्त था, पर धिन्वि""पा. ३.१.८० से अपवाद के रूप में 'उ' कार तथा वकार को अकार आदेश कृण अउ+अन्त, छन्दस्युभयथा पा. ३.४.११७ से आर्धधातुक संज्ञा, अतोलोपः पा ७.४.४८ सूत्र से प्रकार का लोप (कृण+उ+अन्त) सार्वधातुकार्धधातुकयोः पा.
बड २२, अंक
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org