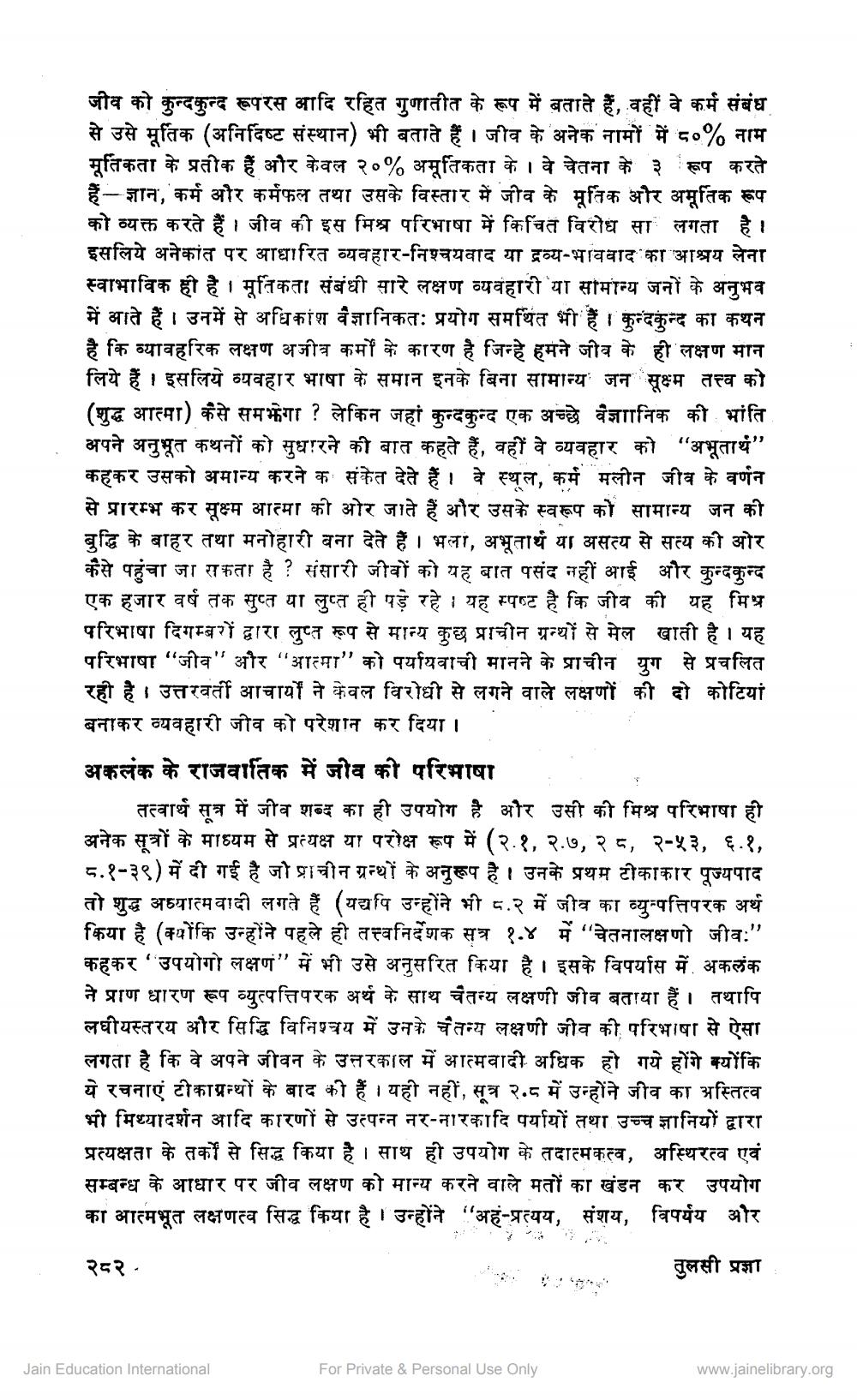________________
जीव को कुन्दकुन्द रूपरस आदि रहित गुणातीत के रूप में बताते हैं, वहीं वे कर्म संबंध से उसे मूर्तिक (अनिर्दिष्ट संस्थान) भी बताते हैं । जीव के अनेक नामों में ८०% नाम मूर्तिकता के प्रतीक हैं और केवल २०% अमूर्तिकता के । वे चेतना के ३ रूप करते हैं-ज्ञान, कर्म और कर्मफल तथा उसके विस्तार में जीव के मूर्तिक और अमूर्तिक रूप को व्यक्त करते हैं। जीव की इस मिश्र परिभाषा में किचित विरोध सा लगता है। इसलिये अनेकांत पर आधारित व्यवहार-निश्चयवाद या द्रव्य-भाववाद का आश्रय लेना स्वाभाविक ही है । मूर्तिकता संबंधी सारे लक्षण व्यवहारी या सामान्य जनों के अनुभव में आते हैं। उनमें से अधिकांश वैज्ञानिकतः प्रयोग समर्थित भी हैं । कुन्दकुन्द का कथन है कि व्यावहरिक लक्षण अजीत्र कर्मों के कारण है जिन्हे हमने जीव के ही लक्षण मान लिये हैं । इसलिये व्यवहार भाषा के समान इनके बिना सामान्य जन सूक्ष्म तत्त्व को (शुद्ध आत्मा) कैसे समझेगा? लेकिन जहां कुन्दकुन्द एक अच्छे वैज्ञानिक की भांति अपने अनुभूत कथनों को सुधारने की बात कहते हैं, वहीं वे व्यवहार को "अभूतार्थ" कहकर उसको अमान्य करने क संकेत देते हैं। वे स्थूल, कर्म मलीन जीव के वर्णन से प्रारम्भ कर सूक्ष्म आत्मा की ओर जाते हैं और उसके स्वरूप को सामान्य जन की बुद्धि के बाहर तथा मनोहारी बना देते हैं। भला, अभूतार्थ या असत्य से सत्य की ओर कैसे पहुंचा जा सकता है ? संसारी जीवों को यह बात पसंद नहीं आई और कुन्दकुन्द एक हजार वर्ष तक सुप्त या लुप्त ही पड़े रहे । यह स्पष्ट है कि जीव की यह मिश्र परिभाषा दिगम्बरों द्वारा लुप्त रूप से मान्य कुछ प्राचीन ग्रन्थों से मेल खाती है। यह परिभाषा "जीव" और "आत्मा" को पर्यायवाची मानने के प्राचीन युग से प्रचलित रही है। उत्तरवर्ती आचार्यों ने केवल विरोधी से लगने वाले लक्षणों की दो कोटियां बनाकर व्यवहारी जीव को परेशान कर दिया । अकलंक के राजवातिक में जीव की परिभाषा
तत्वार्थ सूत्र में जीव शब्द का ही उपयोग है और उसी की मिश्र परिभाषा ही अनेक सूत्रों के माध्यम से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में (२.१, २.७, २८, २-५३, ६.१, ८.१-३९) में दी गई है जो प्राचीन ग्रन्थों के अनुरूप है। उनके प्रथम टीकाकार पूज्यपाद तो शुद्ध अध्यात्मवादी लगते हैं (यद्यपि उन्होंने भी ८.२ में जीव का व्युत्पत्तिपरक अर्थ किया है (क्योंकि उन्होंने पहले ही तत्त्वनिर्देशक सत्र १.४ में "चेतनालक्षणो जीवः" कहकर “उपयोगो लक्षणं' में भी उसे अनुसरित किया है । इसके विपर्यास में अकलंक ने प्राण धारण रूप व्युत्पत्तिपरक अर्थ के साथ चैतन्य लक्षणी जीव बताया हैं। तथापि लघीयस्तरय और सिद्धि विनिश्चय में उनके चैतन्य लक्षणी जीव की परिभाषा से ऐसा लगता है कि वे अपने जीवन के उत्तरकाल में आत्मवादी अधिक हो गये होंगे क्योंकि ये रचनाएं टीकाग्रन्थों के बाद की हैं । यही नहीं, सूत्र २.८ में उन्होंने जीव का अस्तित्व भी मिथ्यादर्शन आदि कारणों से उत्पन्न नर-नारकादि पर्यायों तथा उच्च ज्ञानियों द्वारा प्रत्यक्षता के तर्कों से सिद्ध किया है । साथ ही उपयोग के तदात्मकत्व, अस्थिरत्व एवं सम्बन्ध के आधार पर जीव लक्षण को मान्य करने वाले मतों का खंडन कर उपयोग का आत्मभूत लक्षणत्व सिद्ध किया है । उन्होंने "अहं-प्रत्यय, संशय, विपर्यय और
२८२ .
तुलसी प्रज्ञा
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org