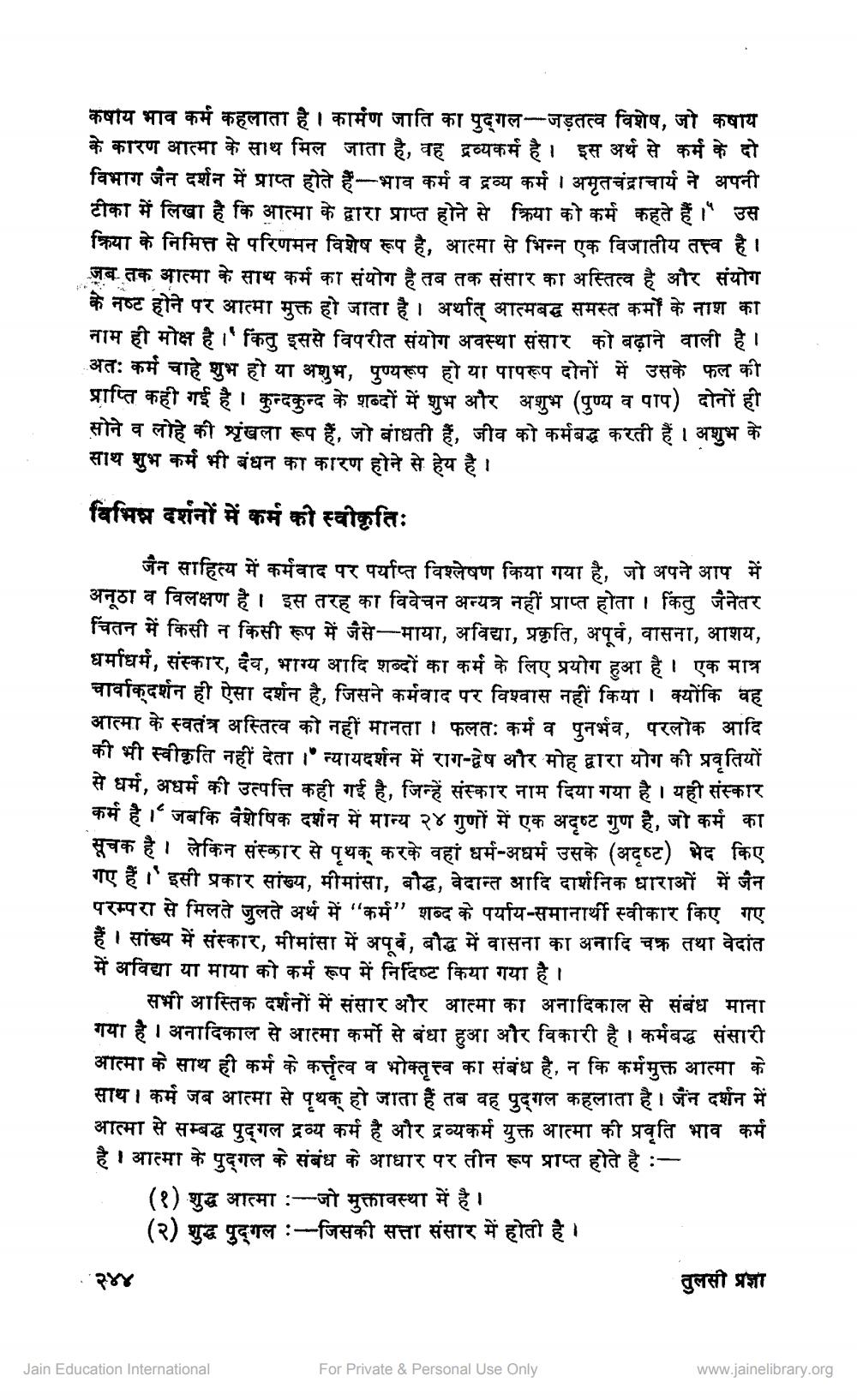________________
कषाय भाव कर्म कहलाता है । कार्मण जाति का पुद्गल-जड़तत्व विशेष, जो कषाय के कारण आत्मा के साथ मिल जाता है, वह द्रव्यकर्म है। इस अर्थ से कर्म के दो विभाग जैन दर्शन में प्राप्त होते हैं-भाव कर्म व द्रव्य कर्म । अमृतचंद्राचार्य ने अपनी टीका में लिखा है कि आत्मा के द्वारा प्राप्त होने से क्रिया को कर्म कहते हैं। उस क्रिया के निमित्त से परिणमन विशेष रूप है, आत्मा से भिन्न एक विजातीय तत्त्व है। जब तक आत्मा के साथ कर्म का संयोग है तब तक संसार का अस्तित्व है और संयोग के नष्ट होने पर आत्मा मुक्त हो जाता है। अर्थात् आत्मबद्ध समस्त कर्मों के नाश का नाम ही मोक्ष है। किंतु इससे विपरीत संयोग अवस्था संसार को बढ़ाने वाली है। अतः कर्म चाहे शुभ हो या अशुभ, पुण्यरूप हो या पापरूप दोनों में उसके फल की प्राप्ति कही गई है । कुन्दकुन्द के शब्दों में शुभ और अशुभ (पुण्य व पाप) दोनों ही सोने व लोहे की शृंखला रूप हैं, जो बांधती हैं, जीव को कर्मबद्ध करती हैं । अशुभ के साथ शुभ कर्म भी बंधन का कारण होने से हेय है। विभिन्न दर्शनों में कर्म को स्वीकृतिः
जैन साहित्य में कर्मवाद पर पर्याप्त विश्लेषण किया गया है, जो अपने आप में अनूठा व विलक्षण है। इस तरह का विवेचन अन्यत्र नहीं प्राप्त होता । किंतु जैनेतर चिंतन में किसी न किसी रूप में जैसे-माया, अविद्या, प्रकृति, अपूर्व, वासना, आशय, धर्माधर्म, संस्कार, दैव, भाग्य आदि शब्दों का कर्म के लिए प्रयोग हुआ है । एक मात्र चार्वाक्दर्शन ही ऐसा दर्शन है, जिसने कर्मवाद पर विश्वास नहीं किया। क्योंकि वह आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व को नहीं मानता । फलतः कर्म व पुनर्भव, परलोक आदि की भी स्वीकृति नहीं देता। न्यायदर्शन में राग-द्वेष और मोह द्वारा योग की प्रवृतियों से धर्म, अधर्म की उत्पत्ति कही गई है, जिन्हें संस्कार नाम दिया गया है। यही संस्कार कर्म है। जबकि वैशेषिक दर्शन में मान्य २४ गुणों में एक अदृष्ट गुण है, जो कर्म का सूचक है। लेकिन संस्कार से पृथक् करके वहां धर्म-अधर्म उसके (अदृष्ट) भेद किए गए हैं। इसी प्रकार सांख्य, मीमांसा, बौद्ध, वेदान्त आदि दार्शनिक धाराओं में जैन परम्परा से मिलते जुलते अर्थ में "कर्म" शब्द के पर्याय-समानार्थी स्वीकार किए गए हैं । सांख्य में संस्कार, मीमांसा में अपूर्व, बौद्ध में वासना का अनादि चक्र तथा वेदांत में अविद्या या माया को कर्म रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
सभी आस्तिक दर्शनों में संसार और आत्मा का अनादिकाल से संबंध माना गया है । अनादिकाल से आत्मा कर्मो से बंधा हुआ और विकारी है। कर्मबद्ध संसारी आत्मा के साथ ही कर्म के कर्तृत्व व भोक्तृत्त्व का संबंध है, न कि कर्ममुक्त आत्मा के साथ । कर्म जब आत्मा से पृथक् हो जाता हैं तब वह पुद्गल कहलाता है। जैन दर्शन में आत्मा से सम्बद्ध पुद्गल द्रव्य कर्म है और द्रव्यकर्म युक्त आत्मा की प्रवृति भाव कर्म है । आत्मा के पुद्गल के संबंध के आधार पर तीन रूप प्राप्त होते है :
(१) शुद्ध आत्मा :-जो मुक्तावस्था में है। (२) शुद्ध पुद्गल :-जिसकी सत्ता संसार में होती है।
. २४४
तुलसी प्रज्ञा
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org