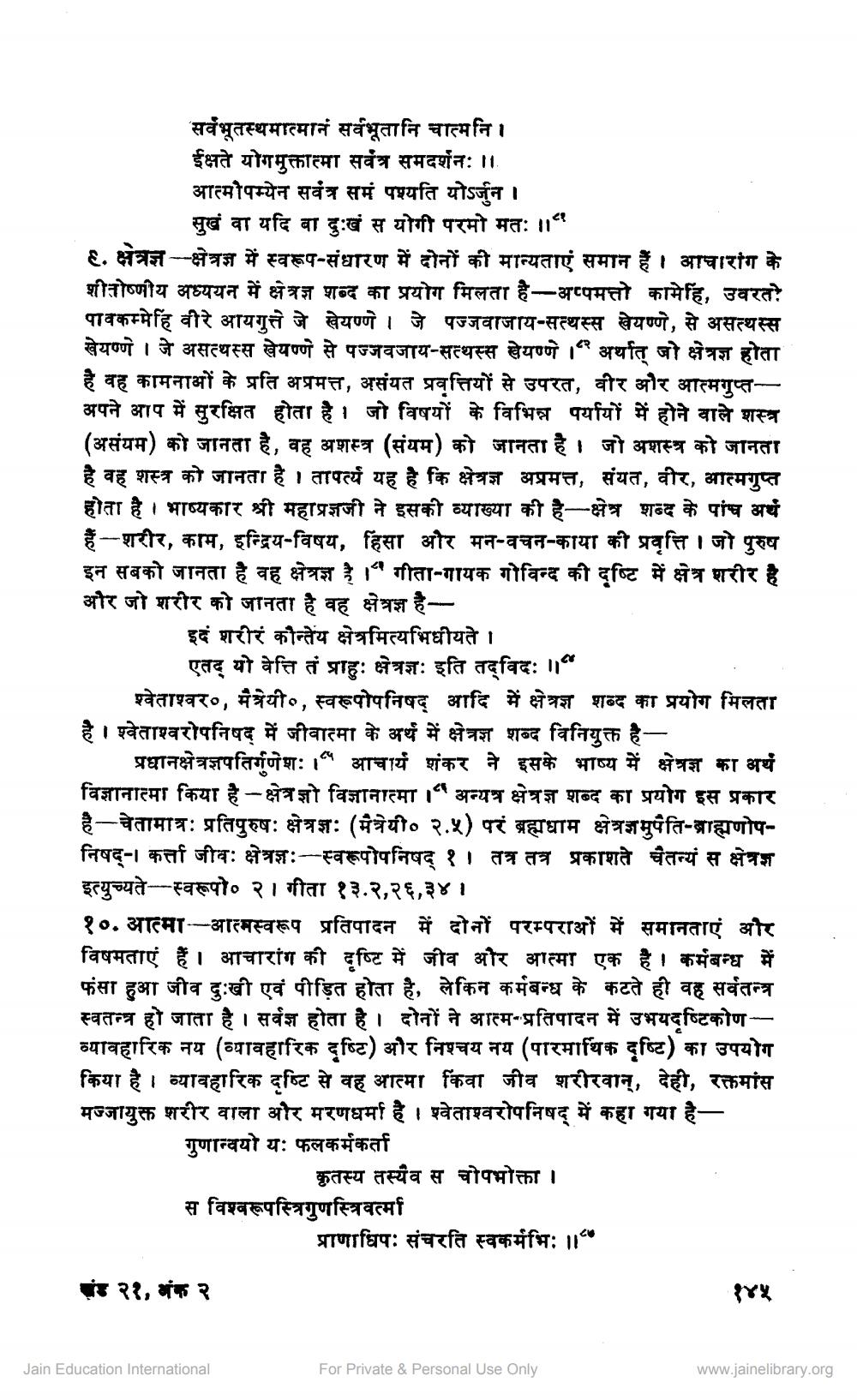________________
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । ईक्षते योगमुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ।। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन । सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ "
६. क्षेत्रज्ञ -क्षेत्रज्ञ में स्वरूप- संधारण में दोनों की मान्यताएं समान हैं । आचारांग के शीतोष्णीय अध्ययन में क्षेत्रज्ञ शब्द का प्रयोग मिलता है-अप्पमत्तो कामेहि, उवरतो पावकम्मे हि वीरे आयगुत्ते जे खेयण्णे । जे पज्जवाजाय - सत्थस्स खेयण्णे, से असत्थस्स खेयणे । जे असत्थस्स खेयपणे से पज्जवजाय - सत्थस्स खेयण्णे । अर्थात् जो क्षेत्रज्ञ होता है वह कामनाओं के प्रति अप्रमत्त, असंयत प्रवृत्तियों से उपरत, वीर और आत्मगुप्त - अपने आप में सुरक्षित होता है । जो विषयों के विभिन्न पर्यायों में होने वाले शस्त्र ( असंयम) को जानता है, वह अशस्त्र ( संयम ) को जानता है । जो अशस्त्र को जानता है वह शस्त्र को जानता है । तापर्त्य यह है कि क्षेत्रज्ञ अप्रमत्त, संयत, वीर, आत्मगुप्त होता है । भाष्यकार श्री महाप्रज्ञजी ने इसकी व्याख्या की है— क्षेत्र शब्द के पांच अर्थ हैं - शरीर, काम, इन्द्रिय-विषय, हिंसा और मन वचन काया की प्रवृत्ति । जो पुरुष इन सबको जानता है वह क्षेत्रज्ञ है ।" गीता-गायक गोविन्द की दृष्टि में क्षेत्र शरीर है और जो शरीर को जानता है वह क्षेत्रज्ञ है
इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते ।
एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञः इति तद्विदः ॥ "
श्वेताश्वर०, मैत्रेयी०, स्वरूपोपनिषद् आदि में क्षेत्रज्ञ शब्द का प्रयोग मिलता है | श्वेताश्वरोपनिषद् में जीवात्मा के अर्थ में क्षेत्रज्ञ शब्द विनियुक्त है
प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेशः । " आचार्य शंकर ने इसके भाष्य में क्षेत्रज्ञ का अर्थ विज्ञानात्मा किया है - क्षेत्रज्ञो विज्ञानात्मा ।" अन्यत्र क्षेत्रज्ञ शब्द का प्रयोग इस प्रकार है - चेतामात्रः प्रतिपुरुषः क्षेत्रज्ञः (मैत्रेयी० २. ५) परं ब्रह्मधाम क्षेत्रज्ञमुपैति ब्राह्मणोपनिषद् | कर्त्ता जीवः क्षेत्रज्ञ :- स्वरूपोपनिषद् १ । तत्र तत्र प्रकाशते चैतन्यं स क्षेत्रज्ञ इत्युच्यते-- स्वरूपो० २ । गीता १३.२,२६,३४ ॥
१०. आत्मा - आत्मस्वरूप प्रतिपादन में दोनों परम्पराओं में समानताएं और विषमताएं हैं। आचारांग की दृष्टि में जीव और आत्मा एक है। कर्मबन्ध में फंसा हुआ जीव दुःखी एवं पीड़ित होता है, लेकिन कर्मबन्ध के कटते ही वह सर्वतन्त्र स्वतन्त्र हो जाता है । सर्वज्ञ होता है। दोनों ने आत्म- प्रतिपादन में उभयदृष्टिकोण - व्यावहारिक नय ( व्यावहारिक दृष्टि ) और निश्चय नय (पारमार्थिक दृष्टि ) का उपयोग किया है । व्यावहारिक दृष्टि से वह आत्मा किंवा जीव शरीरवान्, देही, रक्तमांस मज्जायुक्त शरीर वाला और मरणधर्मा है । श्वेताश्वरोपनिषद् में कहा गया है
गुणान्वयो यः फलकर्मकर्ता
कृतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता । स विश्वरूपस्त्रिगुण स्त्रिवत्र्मा
प्राणाधिपः संचरति स्वकर्मभिः ||
२१, अंक २
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
१४५
www.jainelibrary.org