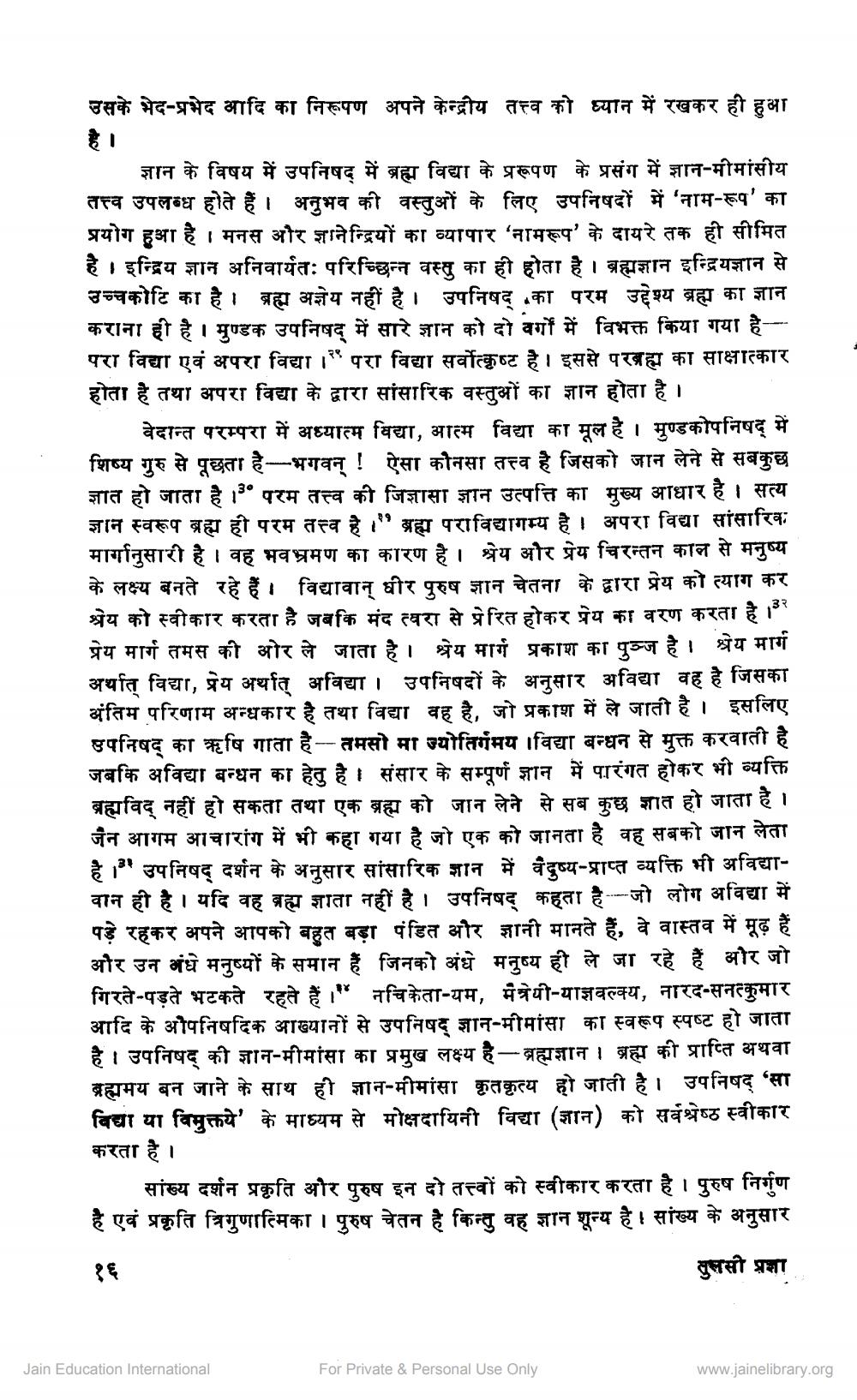________________
उसके भेद-प्रभेद आदि का निरूपण अपने केन्द्रीय तत्त्व को ध्यान में रखकर ही हुआ
ज्ञान के विषय में उपनिषद् में ब्रह्म विद्या के प्ररूपण के प्रसंग में ज्ञान-मीमांसीय तत्त्व उपलब्ध होते हैं। अनुभव की वस्तुओं के लिए उपनिषदों में 'नाम-रूप' का प्रयोग हुआ है । मनस और ज्ञानेन्द्रियों का व्यापार 'नामरूप' के दायरे तक ही सीमित है । इन्द्रिय ज्ञान अनिवार्यतः परिच्छिन्न वस्तु का ही होता है । ब्रह्मज्ञान इन्द्रियज्ञान से उच्चकोटि का है। ब्रह्म अज्ञेय नहीं है। उपनिषद् का परम उद्देश्य ब्रह्म का ज्ञान कराना ही है । मुण्डक उपनिषद् में सारे ज्ञान को दो वर्गों में विभक्त किया गया है-- परा विद्या एवं अपरा विद्या ।२९ परा विद्या सर्वोत्कृष्ट है। इससे परब्रह्म का साक्षात्कार होता है तथा अपरा विद्या के द्वारा सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान होता है ।
वेदान्त परम्परा में अध्यात्म विद्या, आत्म विद्या का मूल है । मुण्डकोपनिषद् में शिष्य गुरु से पूछता है-भगवन् ! ऐसा कौनसा तत्त्व है जिसको जान लेने से सबकुछ ज्ञात हो जाता है। परम तत्त्व की जिज्ञासा ज्ञान उत्पत्ति का मुख्य आधार है । सत्य ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही परम तत्त्व है।" ब्रह्म पराविद्यागम्य है। अपरा विद्या सांसारिक मार्गानुसारी है । वह भवभ्रमण का कारण है। श्रेय और प्रेय चिरन्तन काल से मनुष्य के लक्ष्य बनते रहे हैं। विद्यावान् धीर पुरुष ज्ञान चेतना के द्वारा प्रेय को त्याग कर श्रेय को स्वीकार करता है जबकि मंद त्वरा से प्रेरित होकर प्रेय का वरण करता है । प्रेय मार्ग तमस की ओर ले जाता है। श्रेय मार्ग प्रकाश का पुञ्ज है। श्रेय मार्ग अर्थात् विद्या, प्रेय अर्थात् अविद्या। उपनिषदों के अनुसार अविद्या वह है जिसका अंतिम परिणाम अन्धकार है तथा विद्या वह है, जो प्रकाश में ले जाती है। इसलिए उपनिषद् का ऋषि गाता है-तमसो मा ज्योतिर्गमय ।विद्या बन्धन से मुक्त करवाती है जबकि अविद्या बन्धन का हेतु है। संसार के सम्पूर्ण ज्ञान में पारंगत होकर भी व्यक्ति ब्रह्मविद् नहीं हो सकता तथा एक ब्रह्म को जान लेने से सब कुछ ज्ञात हो जाता है । जैन आगम आचारांग में भी कहा गया है जो एक को जानता है वह सबको जान लेता है।" उपनिषद् दर्शन के अनुसार सांसारिक ज्ञान में वैदुष्य-प्राप्त व्यक्ति भी अविद्यावान ही है । यदि वह ब्रह्म ज्ञाता नहीं है। उपनिषद् कहता है--जो लोग अविद्या में पड़े रहकर अपने आपको बहुत बड़ा पंडित और ज्ञानी मानते हैं, वे वास्तव में मूढ़ हैं और उन अंधे मनुष्यों के समान हैं जिनको अंधे मनुष्य ही ले जा रहे हैं और जो गिरते-पड़ते भटकते रहते हैं।" नचिकेता-यम, मैत्रेयी-याज्ञवल्क्य, नारद-सनत्कुमार आदि के औपनिषदिक आख्यानों से उपनिषद् ज्ञान-मीमांसा का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। उपनिषद् की ज्ञान-मीमांसा का प्रमुख लक्ष्य है- ब्रह्मज्ञान । ब्रह्म की प्राप्ति अथवा ब्रह्ममय बन जाने के साथ ही ज्ञान-मीमांसा कृतकृत्य हो जाती है। उपनिषद् ‘सा विद्या या विमुक्तये' के माध्यम से मोक्षदायिनी विद्या (ज्ञान) को सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करता है।
सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष इन दो तत्त्वों को स्वीकार करता है । पुरुष निर्गुण है एवं प्रकृति त्रिगुणात्मिका । पुरुष चेतन है किन्तु वह ज्ञान शून्य है। सांख्य के अनुसार
तुलसी प्रशा
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org