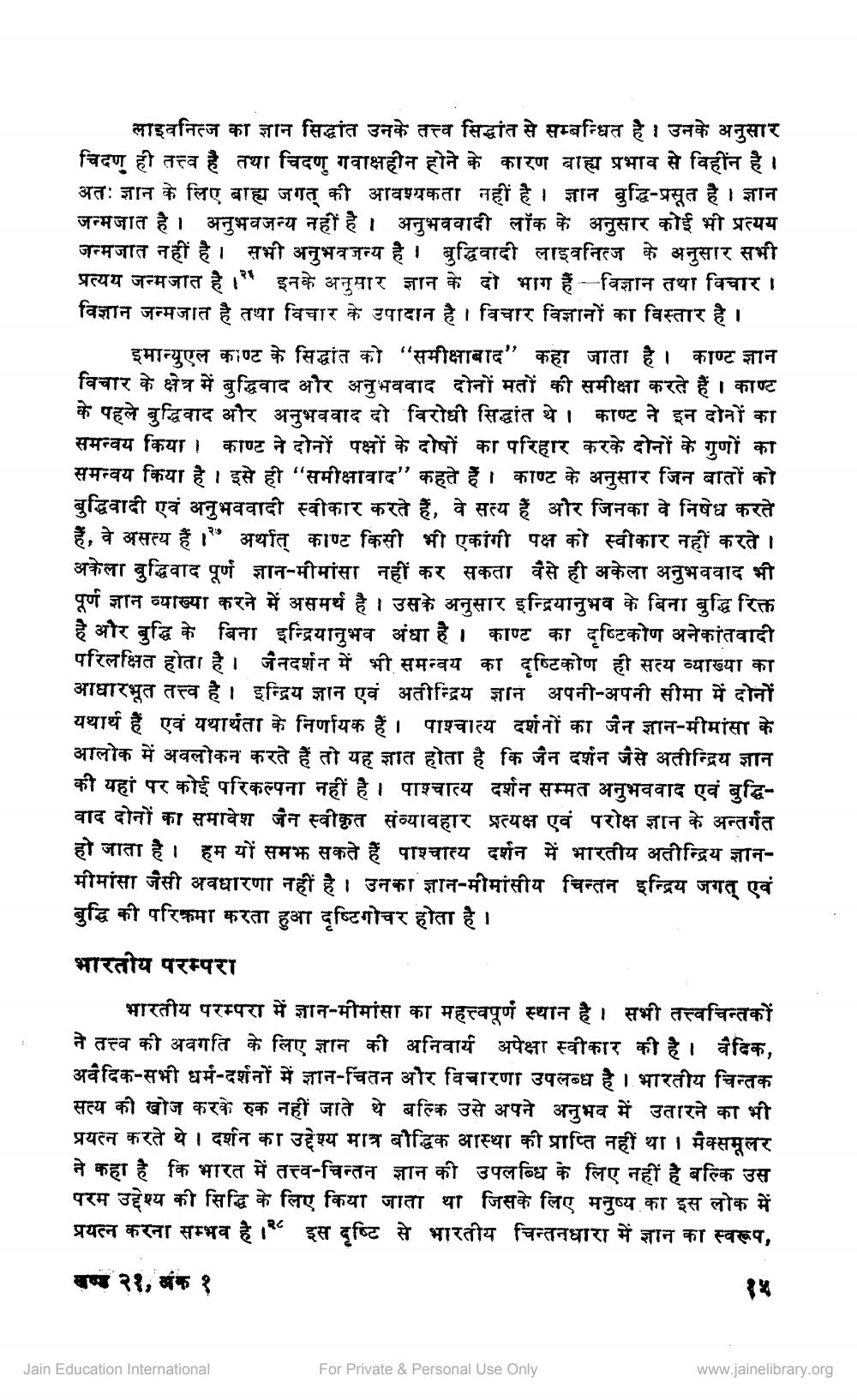________________
लाइवनिज का ज्ञान सिद्धांत उनके तत्त्व सिद्धांत से सम्बन्धित है । उनके अनुसार चिदणु ही तत्त्व है तथा चिदणु गवाक्षहीन होने के कारण बाह्य प्रभाव से विहीन है । अतः ज्ञान के लिए बाह्य जगत् की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान बुद्धि- प्रसूत है | ज्ञान जन्मजात है | अनुभवजन्य नहीं है । अनुभववादी लॉक के अनुसार कोई भी प्रत्यय जन्मजात नहीं है । सभी अनुभवजन्य है । बुद्धिवादी लाइवनित्ज के अनुसार सभी प्रत्यय जन्मजात है ।" इनके अनुसार ज्ञान के दो भाग हैं विज्ञान तथा विचार । विज्ञान जन्मजात है तथा विचार के उपादान है। विचार विज्ञानों का विस्तार है ।
इमान्युएल काट के सिद्धांत को "समीक्षाबाद" कहा जाता है । काण्ट ज्ञान विचार के क्षेत्र में बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों मतों की समीक्षा करते हैं । काट के पहले बुद्धिवाद और अनुभववाद दो विरोधी सिद्धांत थे । काण्ट ने इन दोनों का समन्वय किया । काण्ट ने दोनों पक्षों के दोषों का परिहार करके दोनों के गुणों का समन्वय किया है । इसे ही "समीक्षावाद" कहते हैं । काण्ट के अनुसार जिन बातों को बुद्धिवादी एवं अनुभववादी स्वीकार करते हैं, वे सत्य हैं और जिनका वे निषेध करते हैं, वे असत्य हैं ।" अर्थात् काण्ट किसी भी एकांगी पक्ष को स्वीकार नहीं करते । अकेला बुद्धिवाद पूर्ण ज्ञान-मीमांसा नहीं कर सकता वैसे ही अकेला अनुभववाद भी पूर्ण ज्ञान व्याख्या करने में असमर्थ है। उसके अनुसार इन्द्रियानुभव के बिना बुद्धि रिक्त है और बुद्धि के बिना इन्द्रियानुभव अंधा है । काण्ट का दृष्टिकोण अनेकांतवादी परिलक्षित होता है। जैनदर्शन में भी समन्वय का दृष्टिकोण ही सत्य व्याख्या का आधारभूत तत्त्व है । इन्द्रिय ज्ञान एवं अतीन्द्रिय ज्ञान अपनी-अपनी सीमा में दोनों यथार्थ हैं एवं यथार्थता के निर्णायक हैं । पाश्चात्य दर्शनों का जैन ज्ञान-मीमांसा के आलोक में अवलोकन करते हैं तो यह ज्ञात होता है कि जैन दर्शन जैसे अतीन्द्रिय ज्ञान की यहां पर कोई परिकल्पना नहीं है । पाश्चात्य दर्शन सम्मत अनुभववाद एवं बुद्धिवाद दोनों का समावेश जैन स्वीकृत संव्यावहार प्रत्यक्ष एवं परोक्ष ज्ञान के अन्तर्गत हो जाता है । हम यों समझ सकते हैं पाश्चात्य दर्शन में भारतीय अतीन्द्रिय ज्ञानमीमांसा जैसी अवधारणा नहीं है । उनका ज्ञान-मीमांसीय चिन्तन इन्द्रिय जगत् एवं बुद्धि की परिक्रमा करता हुआ दृष्टिगोचर होता है ।
भारतीय परम्परा
भारतीय परम्परा में ज्ञान-मीमांसा का महत्त्वपूर्ण स्थान है । सभी तत्त्वचिन्तकों ने तत्त्व की अवगति के लिए ज्ञान की अनिवार्य अपेक्षा स्वीकार की है। वैदिक, अवैदिक-सभी धर्म-दर्शनों में ज्ञान-चिंतन और विचारणा उपलब्ध है । भारतीय चिन्तक सत्य की खोज करके रुक नहीं जाते थे बल्कि उसे अपने अनुभव में उतारने का भी प्रयत्न करते थे । दर्शन का उद्देश्य मात्र बौद्धिक आस्था की प्राप्ति नहीं था । मैक्समूलर ने कहा है कि भारत में तत्त्व-चिन्तन ज्ञान की उपलब्धि के लिए नहीं है बल्कि उस परम उद्देश्य की सिद्धि के लिए किया जाता था जिसके लिए मनुष्य का इस लोक में प्रयत्न करना सम्भव है । इस दृष्टि से भारतीय चिन्तनधारा में ज्ञान का स्वरूप,
२८
खण्ड २१, अंक १
१५
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org