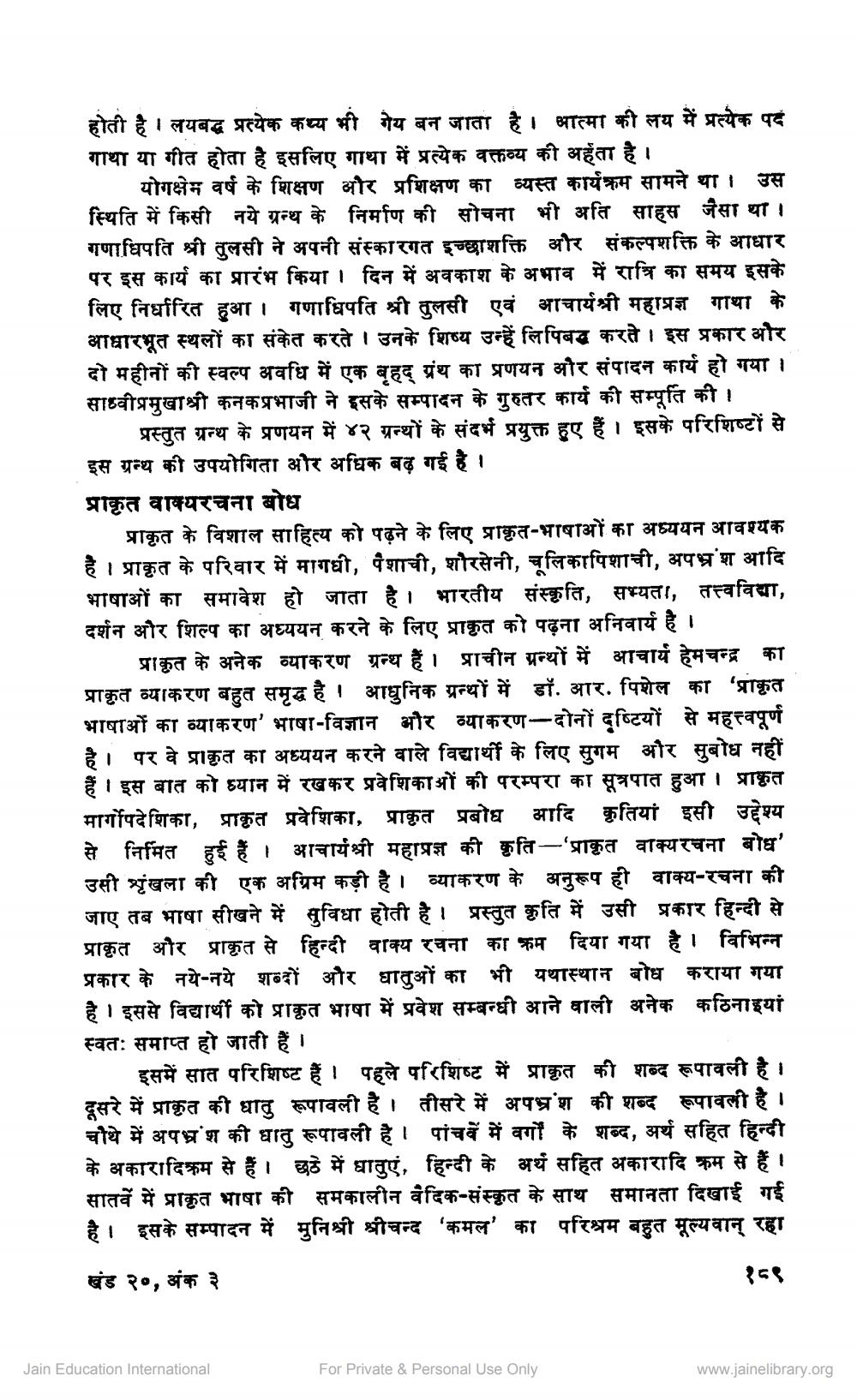________________
होती है । लयबद्ध प्रत्येक कथ्य भी गेय बन जाता है। आत्मा की लय में प्रत्येक पद गाथा या गीत होता है इसलिए गाथा में प्रत्येक वक्तव्य की अर्हता है ।
योगक्षेम वर्ष के शिक्षण और प्रशिक्षण का व्यस्त कार्यक्रम सामने था। उस स्थिति में किसी नये ग्रन्थ के निर्माण की सोचना भी अति साहस जैसा था। गणाधिपति श्री तुलसी ने अपनी संस्कारगत इच्छाशक्ति और संकल्पशक्ति के आधार पर इस कार्य का प्रारंभ किया। दिन में अवकाश के अभाव में रात्रि का समय इसके लिए निर्धारित हुआ। गणाधिपति श्री तुलसी एवं आचार्यश्री महाप्रज्ञ गाथा के आधारभूत स्थलों का संकेत करते । उनके शिष्य उन्हें लिपिबद्ध करते । इस प्रकार और दो महीनों की स्वल्प अवधि में एक बृहद् ग्रंथ का प्रणयन और संपादन कार्य हो गया। साध्वीप्रमुखाश्री कनकप्रभाजी ने इसके सम्पादन के गुरुतर कार्य की सम्पूर्ति की।
___ प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रणयन में ४२ ग्रन्थों के संदर्भ प्रयुक्त हुए हैं। इसके परिशिष्टों से इस ग्रन्थ की उपयोगिता और अधिक बढ़ गई है। प्राकृत वाक्यरचना बोध
प्राकृत के विशाल साहित्य को पढ़ने के लिए प्राकृत-भाषाओं का अध्ययन आवश्यक है । प्राकृत के परिवार में मागधी, पैशाची, शौरसेनी, चूलिकापिशाची, अपभ्रंश आदि भाषाओं का समावेश हो जाता है। भारतीय संस्कृति, सभ्यता, तत्त्वविद्या, दर्शन और शिल्प का अध्ययन करने के लिए प्राकृत को पढ़ना अनिवार्य है ।
प्राकृत के अनेक व्याकरण ग्रन्थ हैं। प्राचीन ग्रन्थों में आचार्य हेमचन्द्र का प्राकृत व्याकरण बहुत समृद्ध है । आधुनिक ग्रन्थों में डॉ. आर. पिशेल का 'प्राकृत भाषाओं का व्याकरण' भाषा-विज्ञान और व्याकरण-दोनों दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। पर वे प्राकृत का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी के लिए सुगम और सुबोध नहीं हैं । इस बात को ध्यान में रखकर प्रवेशिकाओं की परम्परा का सूत्रपात हुआ। प्राकृत मार्गोपदेशिका, प्राकृत प्रवेशिका, प्राकृत प्रबोध आदि कृतियां इसी उद्देश्य से निर्मित हुई हैं । आचार्यश्री महाप्रज्ञ की कृति–'प्राकृत वाक्यरचना बोध' उसी श्रृंखला की एक अग्रिम कड़ी है। व्याकरण के अनुरूप ही वाक्य-रचना की जाए तब भाषा सीखने में सुविधा होती है। प्रस्तुत कृति में उसी प्रकार हिन्दी से प्राकृत और प्राकृत से हिन्दी वाक्य रचना का क्रम दिया गया है। विभिन्न प्रकार के नये-नये शब्दों और धातुओं का भी यथास्थान बोध कराया गया है । इससे विद्यार्थी को प्राकृत भाषा में प्रवेश सम्बन्धी आने वाली अनेक कठिनाइयां स्वतः समाप्त हो जाती हैं।
इसमें सात परिशिष्ट हैं। पहले परिशिष्ट में प्राकृत की शब्द रूपावली है। दूसरे में प्राकृत की धातु रूपावली है। तीसरे में अपभ्रंश की शब्द रूपावली है । चौथे में अपभ्रंश की धातु रूपावली है। पांचवें में वर्गों के शब्द, अर्थ सहित हिन्दी के अकारादिक्रम से हैं। छठे में धातुएं, हिन्दी के अर्थ सहित अकारादि क्रम से हैं । सातवें में प्राकृत भाषा की समकालीन वैदिक-संस्कृत के साथ समानता दिखाई गई है। इसके सम्पादन में मुनिश्री श्रीचन्द 'कमल' का परिश्रम बहुत मूल्यवान् रहा खंड २०, अंक ३
१८९
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org