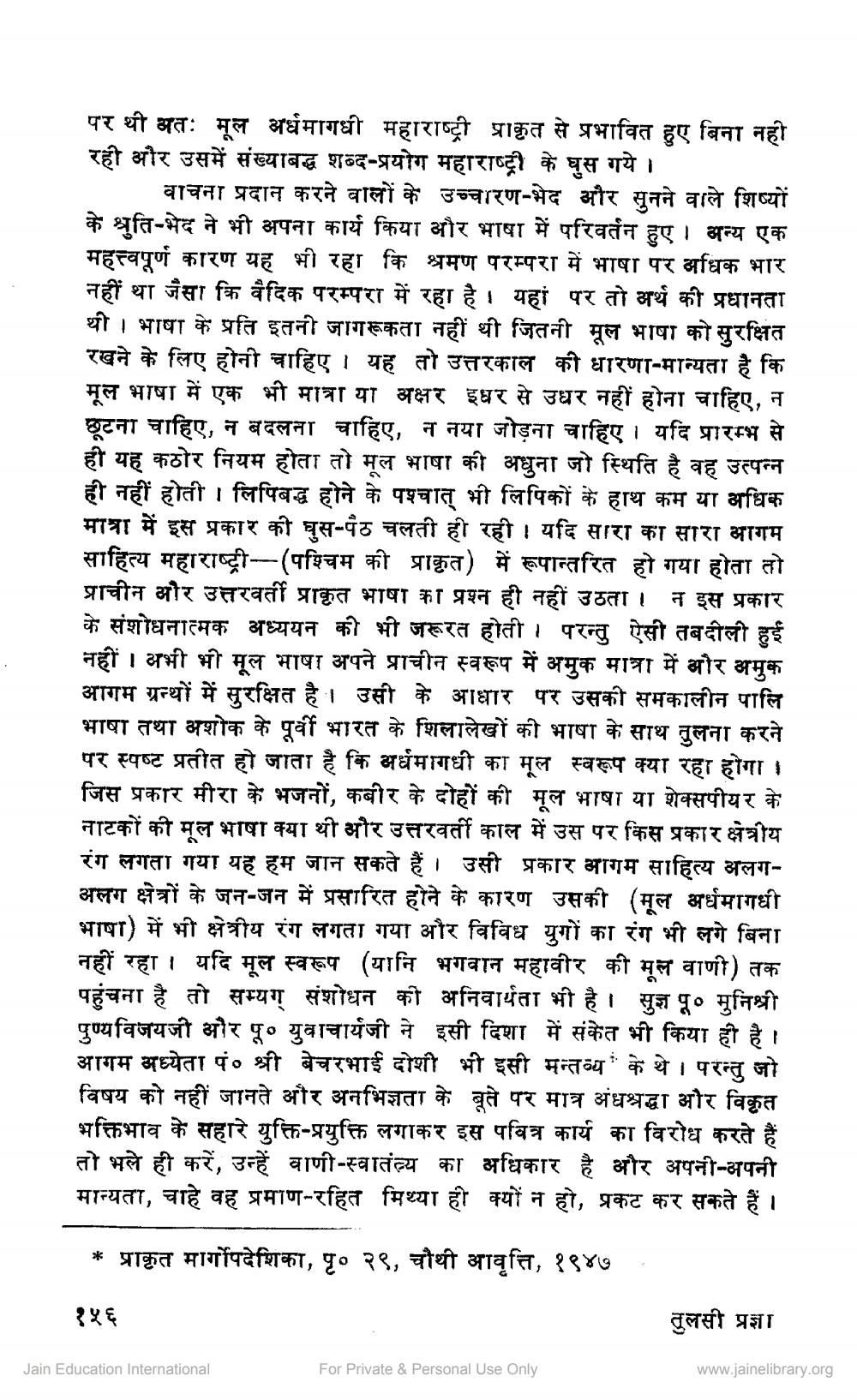________________
पर थी अतः मूल अर्धमागधी महाराष्ट्री प्राकृत से प्रभावित हुए बिना नही रही और उसमें संख्याबद्ध शब्द-प्रयोग महाराष्ट्री के घुस गये।
वाचना प्रदान करने वालों के उच्चारण-भेद और सुनने वाले शिष्यों के श्रुति-भेद ने भी अपना कार्य किया और भाषा में परिवर्तन हुए। अन्य एक महत्त्वपूर्ण कारण यह भी रहा कि श्रमण परम्परा में भाषा पर अधिक भार नहीं था जैसा कि वैदिक परम्परा में रहा है। यहां पर तो अर्थ की प्रधानता थी। भाषा के प्रति इतनी जागरूकता नहीं थी जितनी मूल भाषा को सुरक्षित रखने के लिए होनी चाहिए। यह तो उत्तरकाल की धारणा-मान्यता है कि मूल भाषा में एक भी मात्रा या अक्षर इधर से उधर नहीं होना चाहिए, न छूटना चाहिए, न बदलना चाहिए, न नया जोड़ना चाहिए। यदि प्रारम्भ से ही यह कठोर नियम होता तो मूल भाषा की अधुना जो स्थिति है वह उत्पन्न ही नहीं होती । लिपिबद्ध होने के पश्चात् भी लिपिकों के हाथ कम या अधिक मात्रा में इस प्रकार की घुस-पैठ चलती ही रही। यदि सारा का सारा आगम साहित्य महाराष्ट्री-(पश्चिम की प्राकृत) में रूपान्तरित हो गया होता तो प्राचीन और उत्तरवर्ती प्राकृत भाषा का प्रश्न ही नहीं उठता। न इस प्रकार के संशोधनात्मक अध्ययन की भी जरूरत होती। परन्तु ऐसी तबदीली हुई नहीं। अभी भी मूल भाषा अपने प्राचीन स्वरूप में अमुक मात्रा में और अमुक आगम ग्रन्थों में सुरक्षित है। उसी के आधार पर उसकी समकालीन पालि भाषा तथा अशोक के पूर्वी भारत के शिलालेखों की भाषा के साथ तुलना करने पर स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि अर्धमागधी का मूल स्वरूप क्या रहा होगा। जिस प्रकार मीरा के भजनों, कबीर के दोहों की मूल भाषा या शेक्सपीयर के नाटकों की मूल भाषा क्या थी और उत्तरवर्ती काल में उस पर किस प्रकार क्षेत्रीय रंग लगता गया यह हम जान सकते हैं। उसी प्रकार आगम साहित्य अलगअलग क्षेत्रों के जन-जन में प्रसारित होने के कारण उसकी (मूल अर्धमागधी भाषा) में भी क्षेत्रीय रंग लगता गया और विविध युगों का रंग भी लगे बिना नहीं रहा । यदि मूल स्वरूप (यानि भगवान महावीर की मूल वाणी) तक पहुंचना है तो सम्यग् संशोधन की अनिवार्यता भी है। सुज्ञ पू० मुनिश्री पुण्यविजयजी और पू० युवाचार्यजी ने इसी दिशा में संकेत भी किया ही है। आगम अध्येता पं० श्री बेचरभाई दोशी भी इसी मन्तव्य के थे। परन्तु जो विषय को नहीं जानते और अनभिज्ञता के बूते पर मात्र अंधश्रद्धा और विकृत भक्तिभाव के सहारे युक्ति-प्रयुक्ति लगाकर इस पवित्र कार्य का विरोध करते हैं तो भले ही करें, उन्हें वाणी-स्वातंत्र्य का अधिकार है और अपनी-अपनी मान्यता, चाहे वह प्रमाण-रहित मिथ्या ही क्यों न हो, प्रकट कर सकते हैं।
* प्राकृत मार्गोपदेशिका, पृ० २९, चौथी आवृत्ति, १९४७ .
तुलसी प्रज्ञा
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org