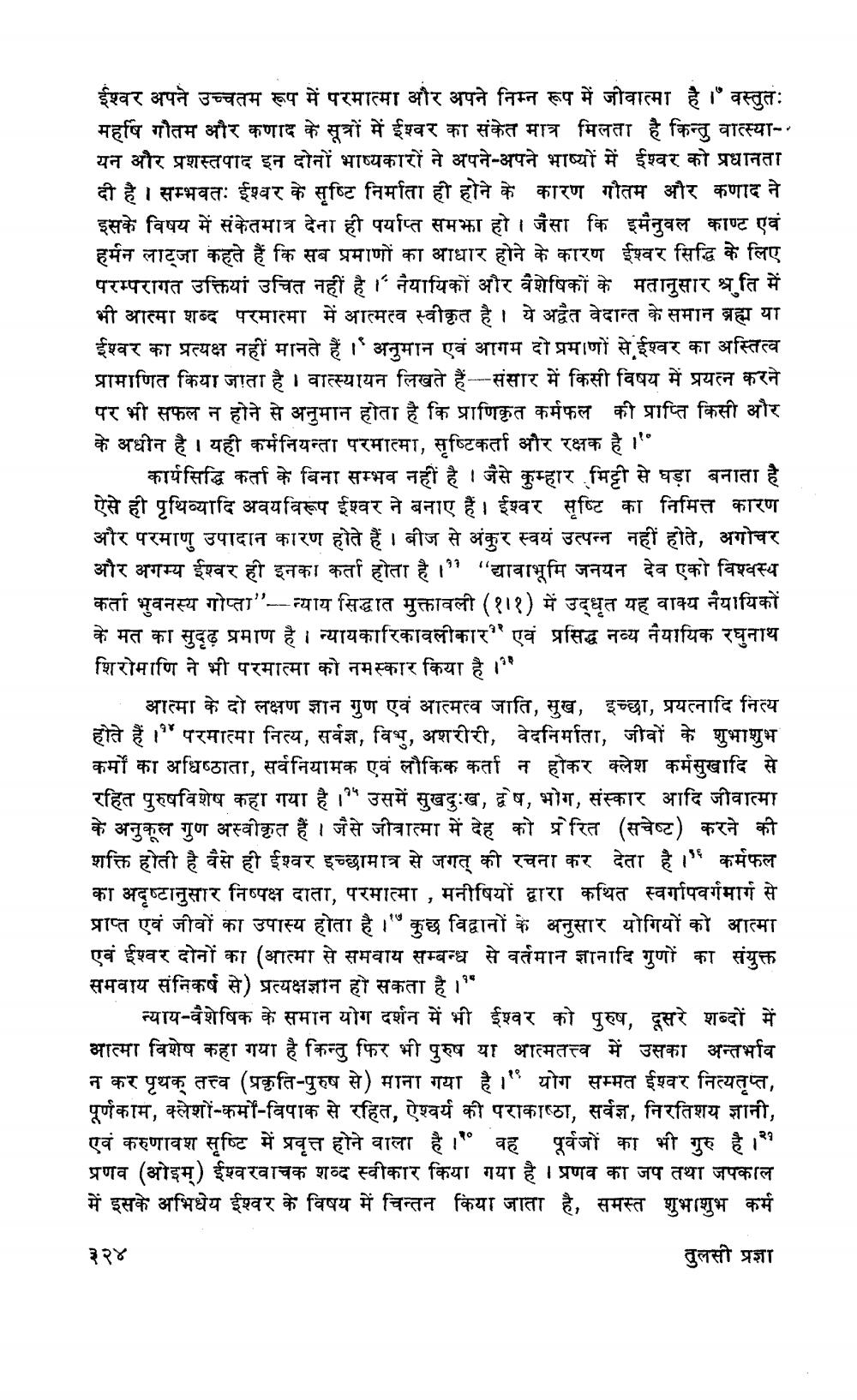________________
ईश्वर अपने उच्चतम रूप में परमात्मा और अपने निम्न रूप में जीवात्मा है। वस्तुतः महर्षि गौतम और कणाद के सूत्रों में ईश्वर का संकेत मात्र मिलता है किन्तु वात्स्यायन और प्रशस्तपाद इन दोनों भाष्यकारों ने अपने-अपने भाष्यों में ईश्वर को प्रधानता दी है । सम्भवतः ईश्वर के सृष्टि निर्माता ही होने के कारण गौतम और कणाद ने इसके विषय में संकेतमात्र देना ही पर्याप्त समझा हो। जैसा कि इमैनुवल काण्ट एवं हर्मन लाट्जा कहते हैं कि सब प्रमाणों का आधार होने के कारण ईश्वर सिद्धि के लिए परम्परागत उक्तियां उचित नहीं है। नैयायिकों और वैशेषिकों के मतानुसार श्रुति में भी आत्मा शब्द परमात्मा में आत्मत्व स्वीकृत है। ये अद्वैत वेदान्त के समान ब्रह्म या ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं। अनुमान एवं आगम दो प्रमाणों से ईश्वर का अस्तित्व प्रामाणित किया जाता है । वात्स्यायन लिखते हैं---संसार में किसी विषय में प्रयत्न करने पर भी सफल न होने से अनुमान होता है कि प्राणिकृत कर्मफल की प्राप्ति किसी और के अधीन है। यही कर्मनियन्ता परमात्मा, सृष्टिकर्ता और रक्षक है ।"
कार्यसिद्धि कर्ता के बिना सम्भव नहीं है । जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है ऐसे ही पृथिव्यादि अवयविरूप ईश्वर ने बनाए हैं। ईश्वर सृष्टि का निमित्त कारण और परमाणु उपादान कारण होते हैं । बीज से अंकुर स्वयं उत्पन्न नहीं होते, अगोचर और अगम्य ईश्वर ही इनका कर्ता होता है ।" "द्यावाभूमि जनयन देव एको विश्वस्थ कर्ता भुवनस्य गोप्ता"-न्याय सिद्धात मुक्तावली (१।१) में उद्धृत यह वाक्य नैयायिकों के मत का सुदृढ़ प्रमाण है । न्यायकारिकावलीकार एवं प्रसिद्ध नव्य नैयायिक रघुनाथ शिरोमाणि ने भी परमात्मा को नमस्कार किया है ।
आत्मा के दो लक्षण ज्ञान गुण एवं आत्मत्व जाति, सुख, इच्छा, प्रयत्नादि नित्य होते हैं।" परमात्मा नित्य, सर्वज्ञ, विभु, अशरीरी, वेदनिर्माता, जीवों के शुभाशुभ कर्मों का अधिष्ठाता, सर्वनियामक एवं लौकिक कर्ता न होकर क्लेश कर्मसुखादि से रहित पुरुषविशेष कहा गया है। उसमें सुखदुःख, द्वेष, भोग, संस्कार आदि जीवात्मा के अनुकूल गुण अस्वीकृत हैं । जैसे जीवात्मा में देह को प्रेरित (सचेष्ट) करने की शक्ति होती है वैसे ही ईश्वर इच्छामात्र से जगत् की रचना कर देता है। कर्मफल का अदृष्टानुसार निष्पक्ष दाता, परमात्मा , मनीषियों द्वारा कथित स्वर्गापवर्गमार्ग से प्राप्त एवं जीवों का उपास्य होता है। कुछ विद्वानों के अनुसार योगियों को आत्मा एवं ईश्वर दोनों का (आत्मा से समवाय सम्बन्ध से वर्तमान ज्ञानादि गुणों का संयुक्त समवाय संनिकर्ष से) प्रत्यक्षज्ञान हो सकता है।"
न्याय-वैशेषिक के समान योग दर्शन में भी ईश्वर को पुरुष, दूसरे शब्दों में आत्मा विशेष कहा गया है किन्तु फिर भी पुरुष या आत्मतत्त्व में उसका अन्तर्भाव न कर पृथक् तत्त्व (प्रकृति-पुरुष से) माना गया है। योग सम्मत ईश्वर नित्यतृप्त, पूर्णकाम, क्लेशों-कर्मो-विपाक से रहित, ऐश्वर्य की पराकाष्ठा, सर्वज्ञ, निरतिशय ज्ञानी, एवं करुणावश सृष्टि में प्रवृत्त होने वाला है। वह पूर्वजों का भी गुरु है।" प्रणव (ओइम्) ईश्वरवाचक शब्द स्वीकार किया गया है । प्रणव का जप तथा जपकाल में इसके अभिधेय ईश्वर के विषय में चिन्तन किया जाता है, समस्त शुभाशुभ कर्म ३२४
तुलसी प्रज्ञा