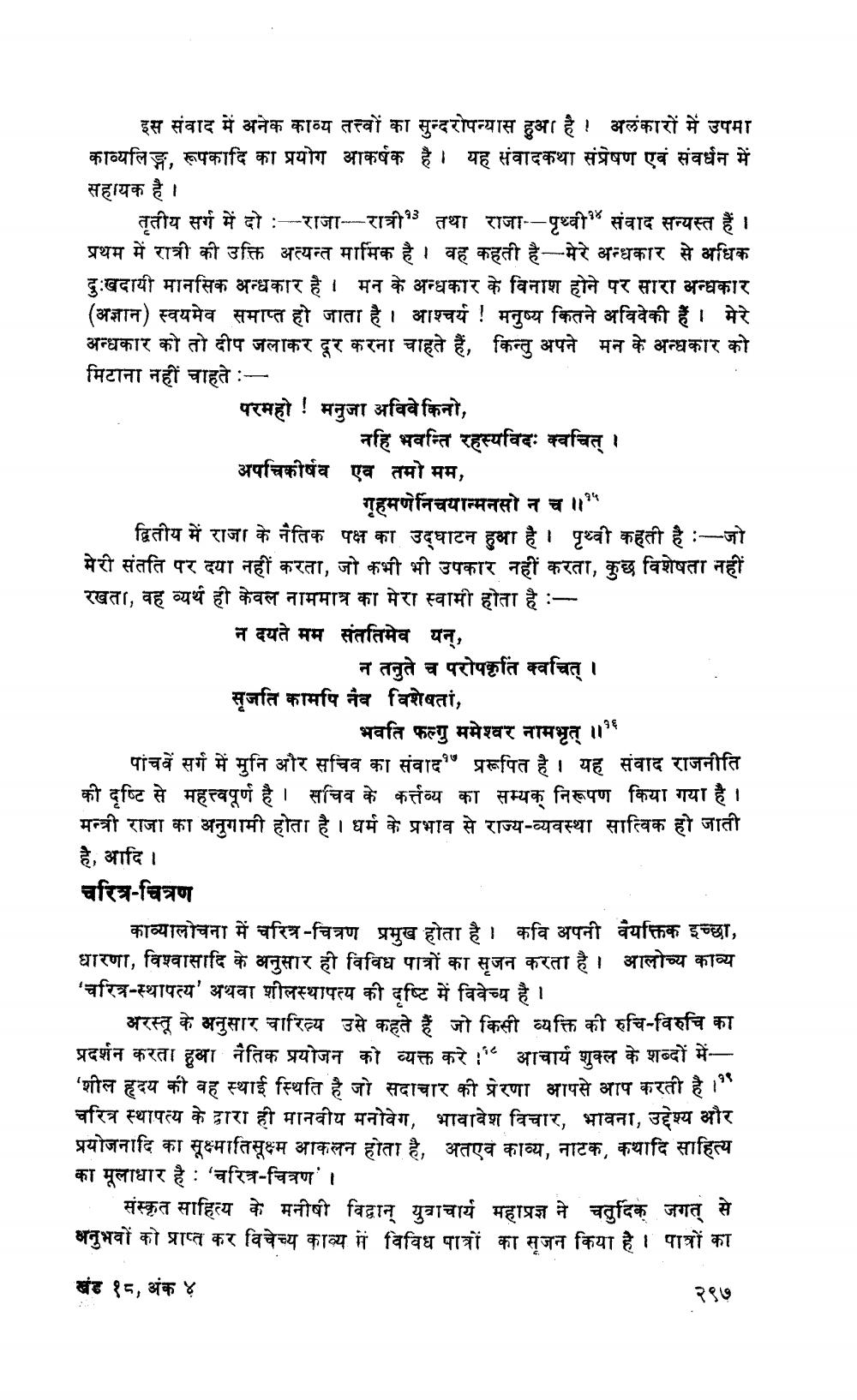________________
इस संवाद में अनेक काव्य तत्त्वों का सुन्दरोपन्यास हुआ है। अलंकारों में उपमा काव्यलिङ्ग, रूपकादि का प्रयोग आकर्षक है। यह संवादकथा संप्रेषण एवं संवर्धन में सहायक है।
___ तृतीय सर्ग में दो :--राजा-रात्री तथा राजा--पृथ्वी संवाद सन्यस्त हैं । प्रथम में रात्री की उक्ति अत्यन्त मार्मिक है। वह कहती है-मेरे अन्धकार से अधिक दुःखदायी मानसिक अन्धकार है। मन के अन्धकार के विनाश होने पर सारा अन्धकार (अज्ञान) स्वयमेव समाप्त हो जाता है। आश्चर्य ! मनुष्य कितने अविवेकी हैं। मेरे अन्धकार को तो दीप जलाकर दूर करना चाहते हैं, किन्तु अपने मन के अन्धकार को मिटाना नहीं चाहते :
परमहो ! मनुजा अविवे किनो,
नहि भवन्ति रहस्यविदः क्वचित् । अपचिकीर्षव एव तमो मम,
गृहमणेनिचयान्मनसो न च ॥१५ द्वितीय में राजा के नैतिक पक्ष का उद्घाटन हुआ है। पृथ्वी कहती है :-जो मेरी संतति पर दया नहीं करता, जो कभी भी उपकार नहीं करता, कुछ विशेषता नहीं रखता, वह व्यर्थ ही केवल नाममात्र का मेरा स्वामी होता है :
न दयते मम संततिमेव यन्,
न तनुते च परोपकृति क्वचित् । सृजति कामपि नैव विशेषतां,
भवति फल्गु ममेश्वर नामभृत् ॥ पांचवें सर्ग में मुनि और सचिव का संवाद प्ररूपित है। यह संवाद राजनीति की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। सचिव के कर्तव्य का सम्यक् निरूपण किया गया है । मन्त्री राजा का अनुगामी होता है । धर्म के प्रभाव से राज्य-व्यवस्था सात्विक हो जाती है, आदि। चरित्र-चित्रण
काव्यालोचना में चरित्र-चित्रण प्रमुख होता है। कवि अपनी वैयक्तिक इच्छा, धारणा, विश्वासादि के अनुसार ही विविध पात्रों का सृजन करता है। आलोच्य काव्य 'चरित्र-स्थापत्य' अथवा शीलस्थापत्य की दृष्टि में विवेच्य है।
अरस्तू के अनुसार चारित्र्य उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति की रुचि-विरुचि का प्रदर्शन करता हुआ नैतिक प्रयोजन को व्यक्त करे ! आचार्य शुक्ल के शब्दों में'शील हृदय की वह स्थाई स्थिति है जो सदाचार की प्रेरणा आपसे आप करती है।" चरित्र स्थापत्य के द्वारा ही मानवीय मनोवेग, भावावेश विचार, भावना, उद्देश्य और प्रयोजनादि का सूक्ष्मातिसूक्ष्म आकलन होता है, अतएव काव्य, नाटक, कथादि साहित्य का मूलाधार है : 'चरित्र-चित्रण।
संस्कृत साहित्य के मनीषी विद्वान् युवाचार्य महाप्रज्ञ ने चतुर्दिक जगत् से अनुभवों को प्राप्त कर विचेच्य काव्य में विविध पात्रों का सृजन किया है। पात्रों का बंड १८, अंक ४
२९७