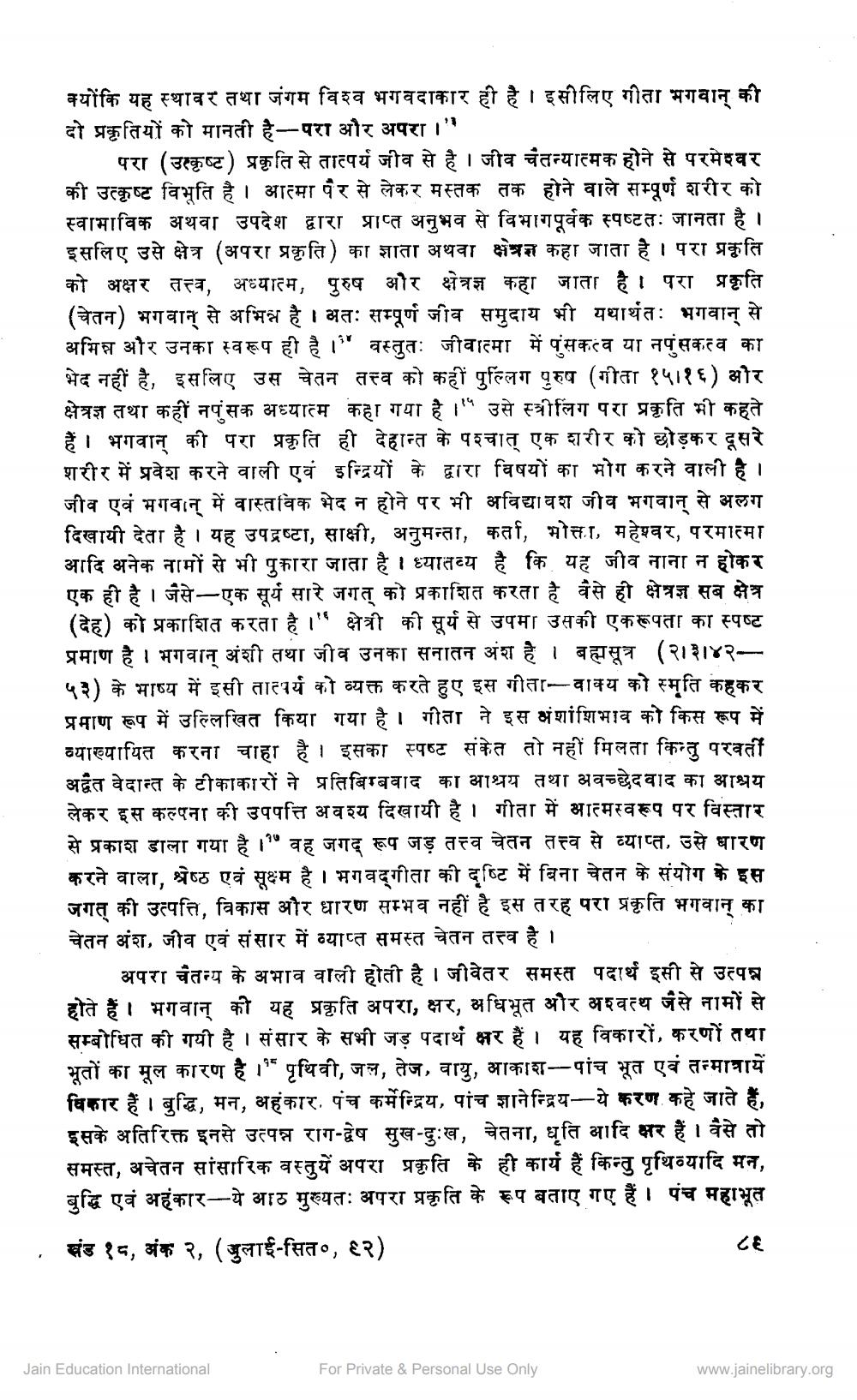________________
क्योंकि यह स्थावर तथा जंगम विश्व भगवदाकार ही है । इसीलिए गीता भगवान् की दो प्रकृतियों को मानती है-परा और अपरा।"
परा (उस्कृष्ट) प्रकृति से तात्पर्य जीव से है । जीव चैतन्यात्मक होने से परमेश्वर की उत्कृष्ट विभुति है। आत्मा पैर से लेकर मस्तक तक होने वाले सम्पूर्ण शरीर को स्वाभाविक अथवा उपदेश द्वारा प्राप्त अनुभव से विभागपूर्वक स्पष्टतः जानता है । इसलिए उसे क्षेत्र (अपरा प्रकृति) का ज्ञाता अथवा क्षेत्रज्ञ कहा जाता है । परा प्रकृति को अक्षर तत्त्व, अध्यात्म, पुरुष और क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। परा प्रकृति (चेतन) भगवान् से अभिन्न है । अतः सम्पूर्ण जीव समुदाय भी यथार्थतः भगवान् से अभिन्न और उनका स्वरूप ही है ।" वस्तुतः जीवात्मा में पुंसकत्व या नपुंसकत्व का भेद नहीं है, इसलिए उस चेतन तत्त्व को कहीं पुल्लिग पुरुष (गीता १५।१६) और क्षेत्रज्ञ तथा कहीं नपुंसक अध्यात्म कहा गया है ।" उसे स्त्रीलिंग परा प्रकृति भी कहते हैं। भगवान् की परा प्रकृति ही देहान्त के पश्चात् एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करने वाली एवं इन्द्रियों के द्वारा विषयों का भोग करने वाली है। जीव एवं भगवान् में वास्तविक भेद न होने पर भी अविद्या वश जीव भगवान् से अलग दिखायी देता है । यह उपद्रष्टा, साक्षी, अनुमन्ता, कर्ता, भोत्ता, महेश्वर, परमात्मा आदि अनेक नामों से भी पुकारा जाता है । ध्यातव्य है कि यह जीव नाना न होकर एक ही है। जैसे-एक सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करता है वैसे ही क्षेत्रज्ञ सब क्षेत्र (देह) को प्रकाशित करता है। क्षेत्री की सूर्य से उपमा उसकी एकरूपता का स्पष्ट प्रमाण है । भगवान् अंशी तथा जीव उनका सनातन अंश है । बह्मसूत्र (२।३।४२५३) के भाष्य में इसी तात्पर्य को व्यक्त करते हुए इस गीता-वाक्य को स्मृति कहकर प्रमाण रूप में उल्लिखित किया गया है। गीता ने इस अंशांशिभाव को किस रूप में व्याख्यायित करना चाहा है। इसका स्पष्ट संकेत तो नहीं मिलता किन्तु परवर्ती अद्वैत वेदान्त के टीकाकारों ने प्रतिबिम्बवाद का आश्रय तथा अवच्छेदवाद का आश्रय लेकर इस कल्पना की उपपत्ति अवश्य दिखायी है। गीता में आत्मस्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। वह जगद् रूप जड़ तत्त्व चेतन तत्त्व से व्याप्त, उसे धारण करने वाला, श्रेष्ठ एवं सूक्ष्म है । भगवद्गीता की दृष्टि में बिना चेतन के संयोग के इस जगत् की उत्पत्ति, विकास और धारण सम्भव नहीं है इस तरह परा प्रकृति भगवान का चेतन अंश, जीव एवं संसार में व्याप्त समस्त चेतन तत्त्व है।
अपरा चैतन्य के अभाव वाली होती है । जीवेतर समस्त पदार्थ इसी से उत्पन्न होते हैं। भगवान् की यह प्रकृति अपरा, क्षर, अधिभूत और अश्वत्थ जैसे नामों से सम्बोधित की गयी है । संसार के सभी जड़ पदार्थ क्षर हैं। यह विकारों, करणों तथा भूतों का मूल कारण है । पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश-पांच भूत एवं तन्मात्रायें धिकार हैं । बुद्धि, मन, अहंकार. पंच कर्मेन्द्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय-ये करण कहे जाते हैं, इसके अतिरिक्त इनसे उत्पन्न राग-द्वेष सुख-दुःख, चेतना, धृति आदि क्षर हैं । वैसे तो समस्त, अचेतन सांसारिक वस्तुयें अपरा प्रकृति के ही कार्य हैं किन्तु पृथिव्यादि मन,
बुद्धि एवं अहंकार-ये आठ मुख्यतः अपरा प्रकृति के रूप बताए गए हैं। पंच महाभूत . खंड १८, अंक २, (जुलाई-सित०, ६२)
८६
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org