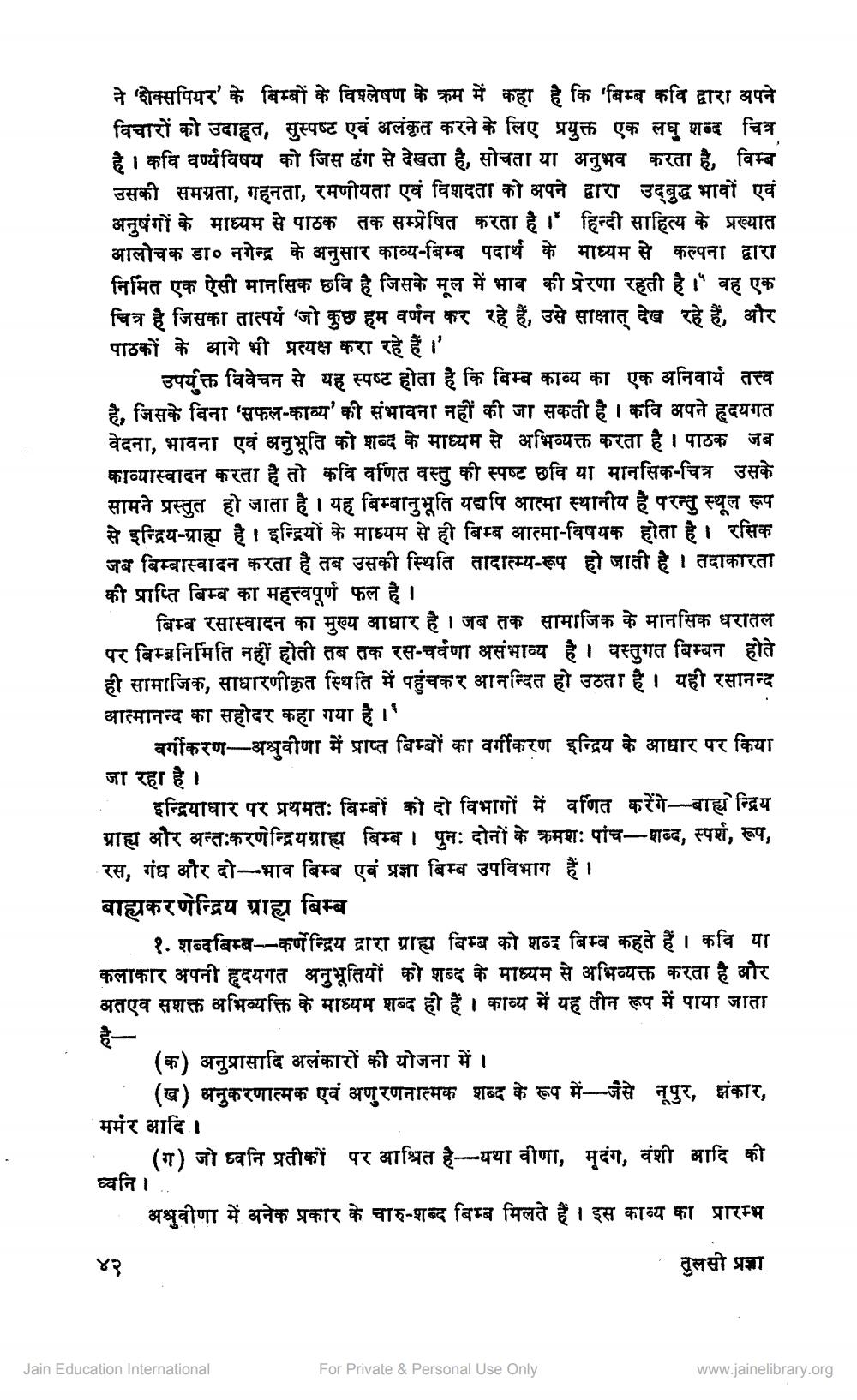________________
द्वारा
ने 'शेक्सपियर' के बिम्बों के विश्लेषण के क्रम में कहा है कि 'बिम्ब कवि द्वारा अपने विचारों को उदाहृत, सुस्पष्ट एवं अलंकृत करने के लिए प्रयुक्त एक लघु शब्द चित्र है । कवि वर्ण्यविषय को जिस ढंग से देखता है, सोचता या अनुभव करता है, विम्ब उसकी समग्रता, गहनता, रमणीयता एवं विशदता को अपने उबुद्ध भावों एवं अनुषंगों के माध्यम से पाठक तक सम्प्रेषित करता है । आलोचक डा० नगेन्द्र के अनुसार काव्य- बिम्ब पदार्थ के निर्मित एक ऐसी मानसिक छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है ।" वह एक चित्र है जिसका तात्पर्य 'जो कुछ हम वर्णन कर रहे हैं, उसे साक्षात् देख रहे हैं, और पाठकों के आगे भी प्रत्यक्ष करा रहे हैं ।'
उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि बिम्ब काव्य का एक अनिवार्य तत्त्व है, जिसके बिना 'सफल - काव्य' की संभावना नहीं की जा सकती है । कवि अपने हृदयगत वेदना, भावना एवं अनुभूति को शब्द माध्यम से अभिव्यक्त करता है । पाठक जब काव्यास्वादन करता है तो कवि वर्णित वस्तु की स्पष्ट छवि या मानसिक चित्र उसके सामने प्रस्तुत हो जाता है । यह बिम्बानुभूति यद्यपि आत्मा स्थानीय है परन्तु स्थूल रूप से इन्द्रियग्राह्म है । इन्द्रियों के माध्यम से ही बिम्ब आत्मा-विषयक होता है । रसिक जब बिम्बास्वादन करता है तब उसकी स्थिति तादात्म्य रूप हो जाती है । तदाकारता की प्राप्ति बिम्ब का महत्त्वपूर्ण फल है ।
बिम्ब रसास्वादन का मुख्य आधार है । जब तक सामाजिक के मानसिक धरातल पर बिम्ब निर्मिति नहीं होती तब तक रस चर्वणा असंभाव्य है । वस्तुगत बिम्बन होते ही सामाजिक, साधारणीकृत स्थिति में पहुंचकर आनन्दित हो उठता है । यही रसानन्द आत्मानन्द का सहोदर कहा गया है । "
वर्गीकरण - अश्रुवीणा में प्राप्त बिम्बों का वर्गीकरण इन्द्रिय के आधार पर किया जा रहा है ।
हिन्दी साहित्य के प्रख्यात माध्यम से कल्पना द्वारा
इन्द्रियाधार पर प्रथमतः बिम्बों को दो विभागों में वर्णित करेंगे — बाह्य न्द्रिय ग्राह्य और अन्तःकरणेन्द्रियग्राह्य बिम्ब । पुनः दोनों के क्रमश: पांच - शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और दो-भाव बिम्ब एवं प्रज्ञा बिम्ब उपविभाग हैं । बाह्यकरणेन्द्रियग्राह्य बिम्ब
१. शब्द बिम्ब - - कर्णेन्द्रिय द्वारा ग्राह्य बिम्ब को शब्द बिम्ब कहते हैं । कवि या कलाकार अपनी हृदयगत अनुभूतियों को शब्द के माध्यम से अभिव्यक्त करता है और अतएव सशक्त अभिव्यक्ति के माध्यम शब्द ही हैं । काव्य में यह तीन रूप में पाया जाता
(क) अनुप्रासादि अलंकारों की योजना में ।
(ख) अनुकरणात्मक एवं अणुरणनात्मक शब्द के रूप में— जैसे नूपुर, झंकार, मर्मर आदि ।
(ग) जो ध्वनि प्रतीकों पर आश्रित है- - यथा वीणा, मृदंग, वंशी आदि की ध्वनि ।
वीणा में अनेक प्रकार के चारु- शब्द बिम्ब मिलते हैं । इस काव्य का प्रारम्भ
तुलसी प्रज्ञा
४२
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org