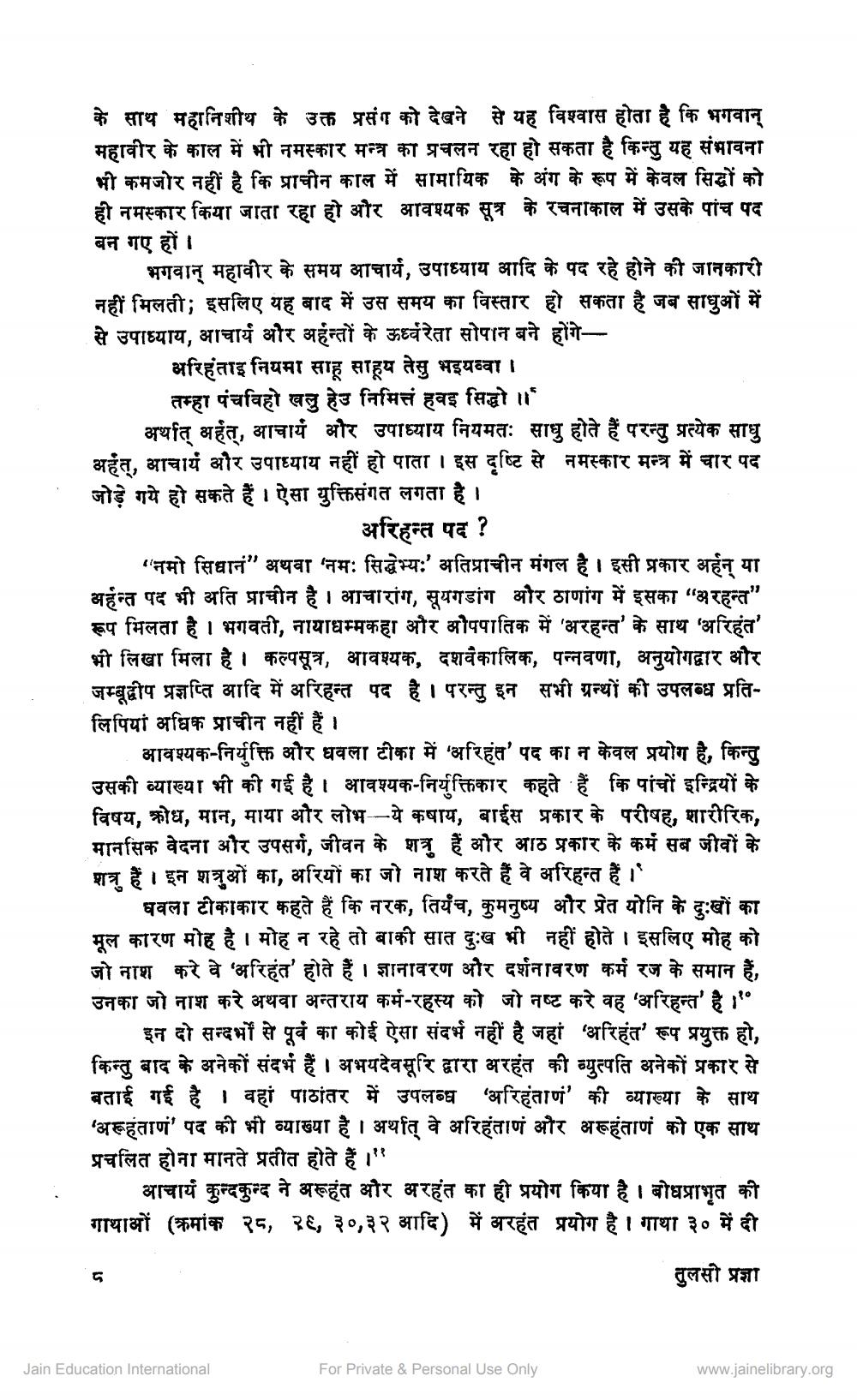________________
के साथ महानिशीथ के उक्त प्रसंग को देखने से यह विश्वास होता है कि भगवान् महावीर के काल में भी नमस्कार मन्त्र का प्रचलन रहा हो सकता है किन्तु यह संभावना भी कमजोर नहीं है कि प्राचीन काल में सामायिक के अंग के रूप में केवल सिद्धों को ही नमस्कार किया जाता रहा हो और आवश्यक सूत्र के रचनाकाल में उसके पांच पद बन गए हों ।
भगवान् महावीर के समय आचार्य, उपाध्याय आदि के पद रहे होने की जानकारी नहीं मिलती; इसलिए यह बाद में उस समय का विस्तार हो सकता है जब साधुओं में से उपाध्याय, आचार्य और अर्हन्तों के ऊर्ध्वरेता सोपान बने होंगे
अरिहंताइ नियमा साहू साहूय तेसु भइयव्वा ।
तम्हा पंचविहो खलु हेउ निमित्तं हवइ सिद्धो ॥
अर्थात् अर्हत्, आचार्य और उपाध्याय नियमतः साधु होते हैं परन्तु प्रत्येक साधु अर्हत्, आचार्य और उपाध्याय नहीं हो पाता । इस दृष्टि से नमस्कार मन्त्र में चार पद जोड़े गये हो सकते हैं । ऐसा युक्तिसंगत लगता है ।
अरिहन्त पद ?
" नमो सिधानं" अथवा 'नमः सिद्धेभ्यः' अतिप्राचीन मंगल है। इसी प्रकार अर्हन् या अर्हन्त पद भी अति प्राचीन है । आचारांग, सूयगडांग और ठाणांग में इसका "अरहन्त" रूप मिलता है | भगवती, नायाधम्मकहा और औपपातिक में 'अरहन्त' के साथ 'अरिहंत' भी लिखा मिला है । कल्पसूत्र, आवश्यक, दशवैकालिक, पन्नवणा, अनुयोगद्वार और जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति आदि में अरिहन्त पद है । परन्तु इन सभी ग्रन्थों की उपलब्ध प्रतिलिपियां अधिक प्राचीन नहीं हैं ।
आवश्यक नियुक्ति और धवला टीका में 'अरिहंत' पद का न केवल प्रयोग है, किन्तु उसकी व्याख्या भी की गई है । आवश्यक नियुक्तिकार कहते हैं कि पांचों इन्द्रियों के विषय, क्रोध, मान, माया और लोभ - ये कषाय, बाईस प्रकार के परीषह, शारीरिक, मानसिक वेदना और उपसर्ग, जीवन के शत्रु हैं और आठ प्रकार के कर्म सब जीवों के शत्रु हैं । इन शत्रुओं का, अरियों का जो नाश करते हैं वे अरिहन्त हैं ।
घवला टीकाकार कहते हैं कि नरक, तिर्यंच, कुमनुष्य और प्रेत योनि के दुःखों का मूल कारण मोह है । मोह न रहे तो बाकी सात दुःख भी नहीं होते । इसलिए मोह को जो नाश करे वे 'अरिहंत' होते हैं । ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म रज के समान हैं, उनका जो नाश करे अथवा अन्तराय कर्म - रहस्य को जो नष्ट करे वह 'अरिहन्त' है ।"
इन दो सन्दर्भों से पूर्व का कोई ऐसा संदर्भ नहीं है जहां 'अरिहंत' रूप प्रयुक्त हो, किन्तु बाद के अनेकों संदर्भ हैं। अभयदेवसूरि द्वारा अरहंत की व्युत्पति अनेकों प्रकार से बताई गई है । वहां पाठांतर में उपलब्ध 'अरिहंताणं' की व्याख्या के साथ 'अरुहंताणं' पद की भी व्याख्या है । अर्थात् वे अरिहंताणं और अहंताणं को एक साथ प्रचलित होना मानते प्रतीत होते हैं । "
आचार्य कुन्दकुन्द ने अरूहंत और अरहंत का ही प्रयोग किया है । बोधप्राभृत की गाथाओं (क्रमांक २८, २६, ३०, ३२ आदि) में अरहंत प्रयोग है | गाथा ३० में दी
तुलसी प्रज्ञा
८
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org