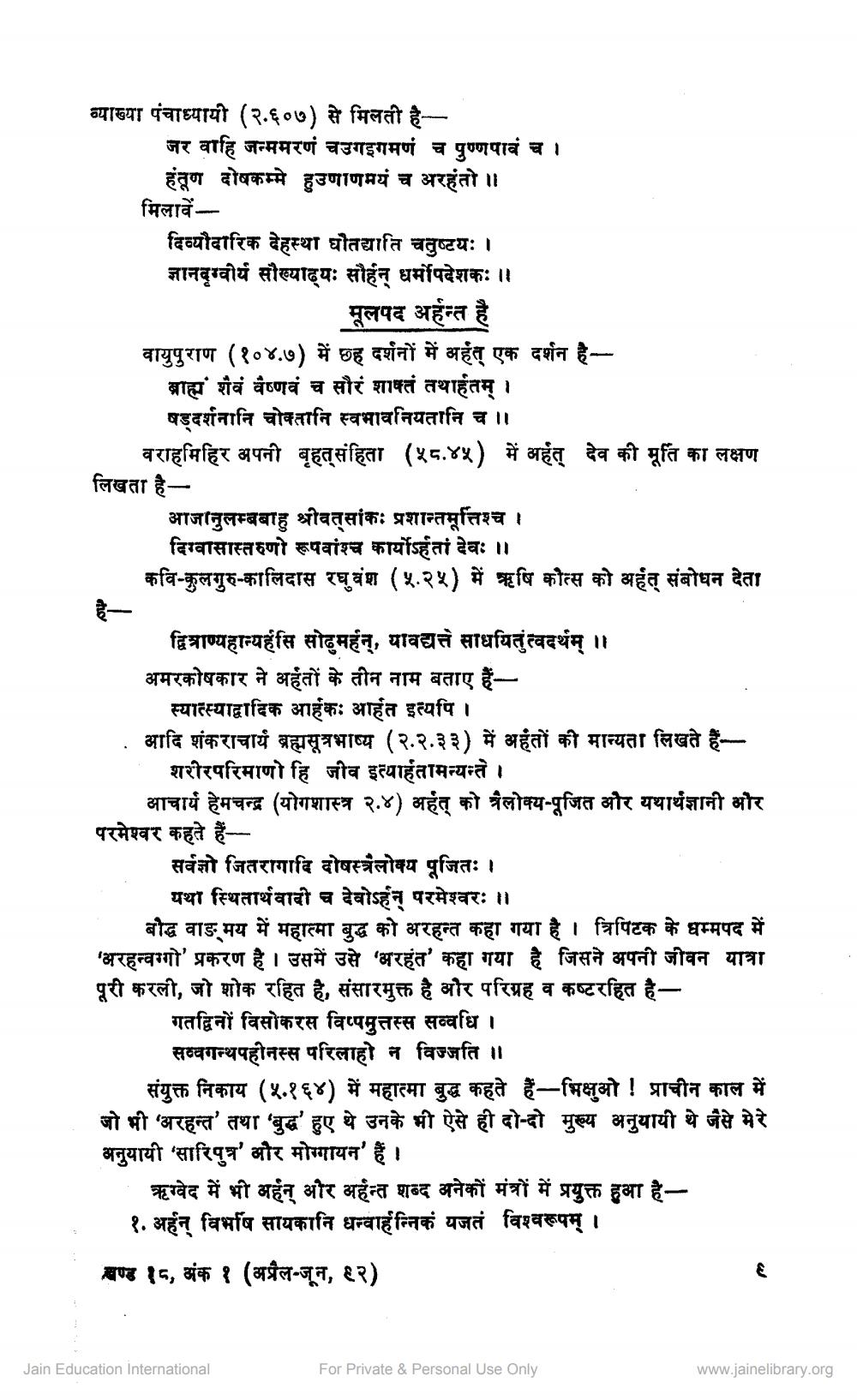________________
व्याख्या पंचाध्यायी (२.६०७) से मिलती है
जर वाहि जन्ममरणं चउगइगमणं च पुण्णपावं च । हंतूण दोषकम्मे हुउणाणमयं च अरहंतो॥ मिलावें
दिव्यौदारिक देहस्था घौतद्याति चतुष्टयः । ज्ञानदृग्वीर्य सौख्याढ्यः सौहंन धर्मोपदेशकः ।।
____ मूलपद अर्हन्त है वायुपुराण (१०४.७) में छह दर्शनों में अर्हत् एक दर्शन हैब्राह्म शैवं वैष्णवं च सौरं शाक्तं तथाहतम् ।
षड्दर्शनानि चोक्तानि स्वभावनियतानि च ।।
वराहमिहिर अपनी बृहत्संहिता (५८.४५) में अर्हत् देव की मूर्ति का लक्षण लिखता है
आजानुलम्बबाहु श्रीवत्सांकः प्रशान्तमूर्तिश्च । दिग्वासास्तरुणो रूपवांश्च कार्योऽर्हतां देवः ॥ कवि-कुलगुरु-कालिदास रघुवंश (५.२५) में ऋषि कौत्स को अहंत संबोधन देता
द्वित्राण्यहान्यहसि सोढुमर्हन्, यावद्यत्त साधयितुं त्वदर्थम् ॥ अमरकोषकार ने अहंतों के तीन नाम बताए हैं
स्यात्स्याद्वादिक आर्हकः आर्हत इत्यपि । . आदि शंकराचार्य ब्रह्मसूत्रभाष्य (२.२.३३) में अहंतों की मान्यता लिखते हैं
शरीरपरिमाणो हि जीव इत्याहंतामन्यन्ते ।
आचार्य हेमचन्द्र (योगशास्त्र २.४) अर्हत् को त्रैलोक्य-पूजित और यथार्थज्ञानी और परमेश्वर कहते हैं
सर्वज्ञो जितरागादि दोषस्त्रलोक्य पूजितः।
यथा स्थितार्थवादी च देवोऽहन परमेश्वरः॥ बौद्ध वाङमय में महात्मा बुद्ध को अरहन्त कहा गया है । त्रिपिटक के धम्मपद में 'अरहन्वग्गो' प्रकरण है । उसमें उसे 'मरहंत' कहा गया है जिसने अपनी जीवन यात्रा पूरी करली, जो शोक रहित है, संसारमुक्त है और परिग्रह व कष्टरहित है
गतद्विनों विसोकरस विप्पमुत्तस्स सव्वधि । सव्वगन्थपहीनस्स परिलाहो न विज्जति । संयुक्त निकाय (५.१६४) में महात्मा बुद्ध कहते हैं-भिक्षुमो ! प्राचीन काल में जो भी 'अरहन्त' तथा 'बुद्ध' हुए थे उनके भी ऐसे ही दो-दो मुख्य अनुयायी थे जैसे मेरे अनुयायी 'सारिपुत्र' और मोग्गायन' हैं।
ऋग्वेद में भी अर्हन और अर्हन्त शब्द अनेकों मंत्रों में प्रयुक्त हुआ है१. अर्हन् विर्षि सायकानि धन्वाह न्निकं यजतं विश्वरूपम् । खण्ड १८, अंक १ (अप्रैल-जून, १२)
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org