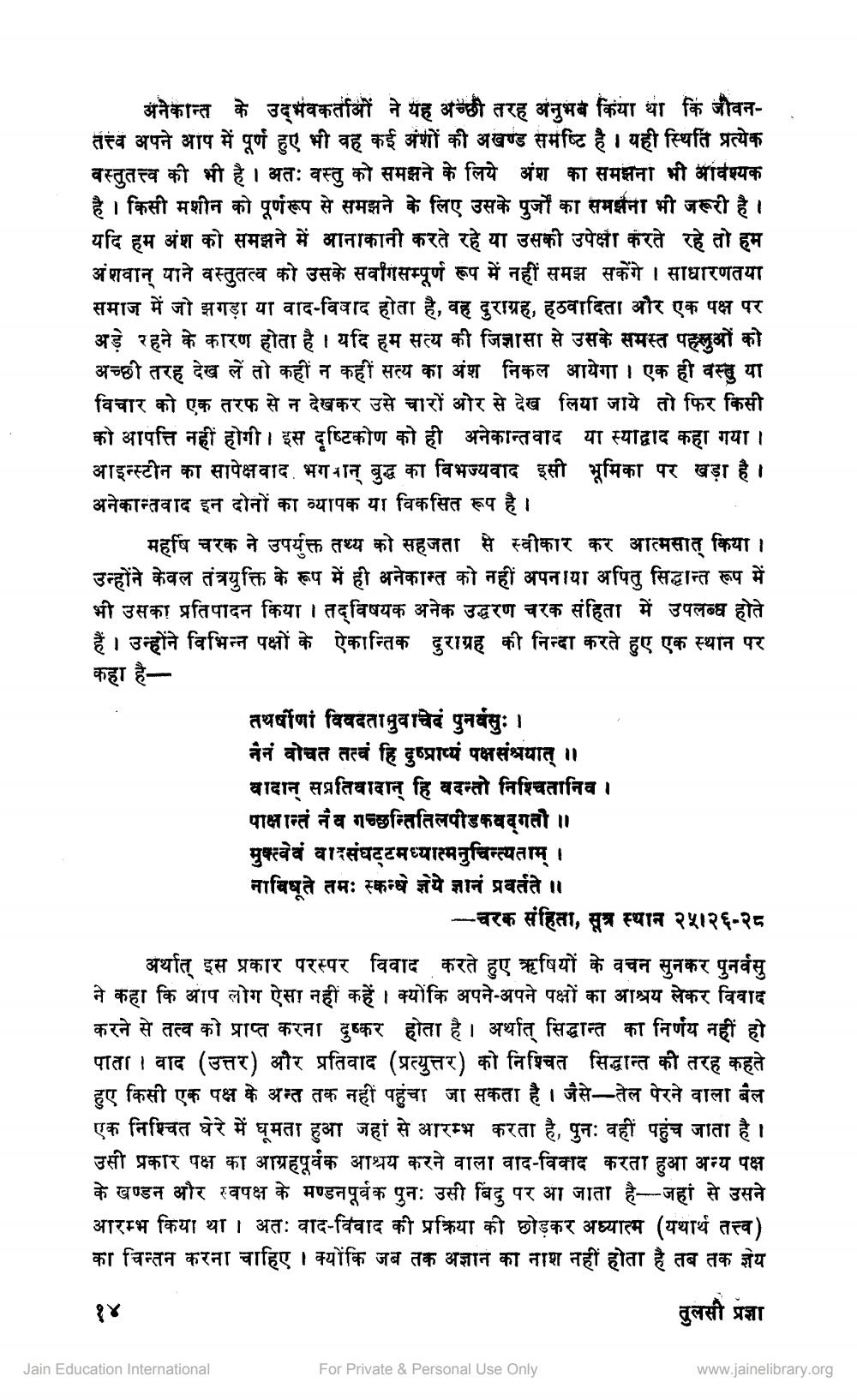________________
अनेकान्त के उद्भवकर्ताओं ने यह अच्छी तरह अनुभब किया था कि जीवनतत्व अपने आप में पूर्ण हुए भी वह कई अंशों की अखण्ड समष्टि है । यही स्थिति प्रत्येक वस्तुतत्त्व की भी है । अतः वस्तु को समझने के लिये अंश का समझना भी आवश्यक है । किसी मशीन को पूर्णरूप से समझने के लिए उसके पुों का समर्शना भी जरूरी है। यदि हम अंश को समझने में आनाकानी करते रहे या उसकी उपेक्षा करते रहे तो हम अंशवान् याने वस्तुतत्व को उसके सर्वांगसम्पूर्ण रूप में नहीं समझ सकेंगे । साधारणतया समाज में जो झगड़ा या वाद-विवाद होता है, वह दुराग्रह, हठवादिता और एक पक्ष पर अड़े रहने के कारण होता है। यदि हम सत्य की जिज्ञासा से उसके समस्त पहलुओं को अच्छी तरह देख लें तो कहीं न कहीं सत्य का अंश निकल आयेगा। एक ही वस्तु या विचार को एक तरफ से न देखकर उसे चारों ओर से देख लिया जाये तो फिर किसी को आपत्ति नहीं होगी। इस दृष्टिकोण को ही अनेकान्त वाद या स्याद्वाद कहा गया। आइन्स्टीन का सापेक्षवाद भगवान बुद्ध का विभज्यवाद इसी भूमिका पर खड़ा है। अनेकान्तवाद इन दोनों का व्यापक या विकसित रूप है।
महर्षि चरक ने उपर्युक्त तथ्य को सहजता से स्वीकार कर आत्मसात् किया। उन्होंने केवल तंत्रयुक्ति के रूप में ही अनेकान्त को नहीं अपनाया अपितु सिद्धान्त रूप में भी उसका प्रतिपादन किया । तद्विषयक अनेक उद्धरण चरक संहिता में उपलब्ध होते हैं। उन्होंने विभिन्न पक्षों के ऐकान्तिक दुराग्रह की निन्दा करते हुए एक स्थान पर कहा है
तथर्षीणां विवदतावाचेदं पुनर्वसुः। नैनं वोचत तत्वं हि दुष्प्राप्यं पक्षसंश्रयात् ॥ वादान् सप्रतिवादान् हि बदन्तो निश्चितानिव । पाक्षान्तं नैव गच्छन्तितिलपीडकवद्गती॥ मुक्त्वेवं वादसंघट्टमध्यात्मनुचिन्त्यताम् । नाविधूते तमः स्कन्धे ज्ञेये ज्ञानं प्रवर्तते ।
-चरक संहिता, सूत्र स्थान २५।२६-२८ अर्थात् इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुए ऋषियों के वचन सुनकर पुनर्वसु ने कहा कि आप लोग ऐसा नहीं कहें। क्योंकि अपने-अपने पक्षों का आश्रय लेकर विवाद करने से तत्व को प्राप्त करना दुष्कर होता है। अर्थात् सिद्धान्त का निर्णय नहीं हो पाता । वाद (उत्तर) और प्रतिवाद (प्रत्युत्तर) को निश्चित सिद्धान्त की तरह कहते हुए किसी एक पक्ष के अन्त तक नहीं पहुंचा जा सकता है । जैसे-तेल पेरने वाला बैल एक निश्चित घेरे में घूमता हुआ जहां से आरम्भ करता है, पुनः वहीं पहुंच जाता है। उसी प्रकार पक्ष का आग्रहपूर्वक आश्रय करने वाला वाद-विवाद करता हुआ अन्य पक्ष के खण्डन और स्वपक्ष के मण्डनपूर्वक पुनः उसी बिंदु पर आ जाता है-जहां से उसने आरम्भ किया था। अतः वाद-विवाद की प्रक्रिया की छोड़कर अध्यात्म (यथार्थ तत्त्व) का चिन्तन करना चाहिए । क्योंकि जब तक अज्ञान का नाश नहीं होता है तब तक ज्ञेय
तुलसी प्रज्ञा
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org