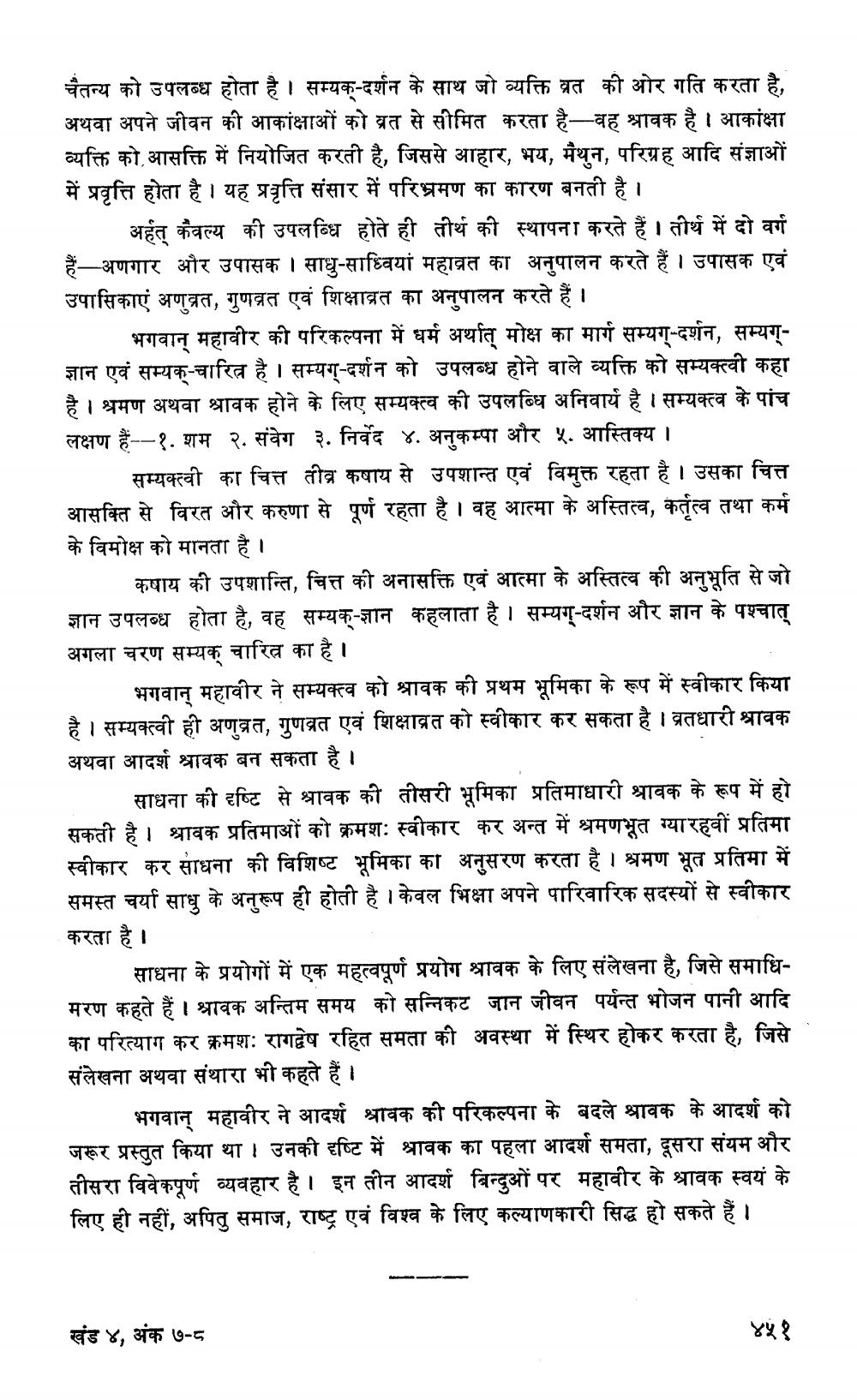________________
चैतन्य को उपलब्ध होता है । सम्यक्-दर्शन के साथ जो व्यक्ति व्रत की ओर गति करता है, अथवा अपने जीवन की आकांक्षाओं को व्रत से सीमित करता है—वह श्रावक है । आकांक्षा व्यक्ति को आसक्ति में नियोजित करती है, जिससे आहार, भय, मैथुन, परिग्रह आदि संज्ञाओं में प्रवृत्ति होता है । यह प्रवृत्ति संसार में परिभ्रमण का कारण बनती है।
अर्हत् कैवल्य की उपलब्धि होते ही तीर्थ की स्थापना करते हैं । तीर्थ में दो वर्ग हैं—अणगार और उपासक । साधु-साध्वियां महाव्रत का अनुपालन करते हैं । उपासक एवं उपासिकाएं अणुव्रत, गुणव्रत एवं शिक्षाव्रत का अनुपालन करते हैं ।
भगवान् महावीर की परिकल्पना में धर्म अर्थात् मोक्ष का मार्ग सम्यग्-दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्-चारित्र है । सम्यग्-दर्शन को उपलब्ध होने वाले व्यक्ति को सम्यक्त्वी कहा है । श्रमण अथवा श्रावक होने के लिए सम्यक्त्व की उपलब्धि अनिवार्य है । सम्यक्त्व के पांच लक्षण हैं--१. शम २. संवेग ३. निर्वेद ४. अनुकम्पा और ५. आस्तिक्य ।
__सम्यक्त्वी का चित्त तीव्र कषाय से उपशान्त एवं विमुक्त रहता है। उसका चित्त आसक्ति से विरत और करुणा से पूर्ण रहता है । वह आत्मा के अस्तित्व, कर्तृत्व तथा कर्म के विमोक्ष को मानता है।
कषाय की उपशान्ति, चित्त की अनासक्ति एवं आत्मा के अस्तित्व की अनुभूति से जो ज्ञान उपलब्ध होता है, वह सम्यक्-ज्ञान कहलाता है । सम्यग-दर्शन और ज्ञान के पश्चात् अगला चरण सम्यक् चारित्र का है।
भगवान महावीर ने सम्यक्त्व को श्रावक की प्रथम भूमिका के रूप में स्वीकार किया है । सम्यक्त्वी ही अणुव्रत, गुणव्रत एवं शिक्षाव्रत को स्वीकार कर सकता है । व्रतधारी श्रावक अथवा आदर्श श्रावक बन सकता है।
साधना की दृष्टि से श्रावक की तीसरी भूमिका प्रतिमाधारी श्रावक के रूप में हो सकती है। श्रावक प्रतिमाओं को क्रमशः स्वीकार कर अन्त में श्रमणभूत ग्यारहवीं प्रतिमा स्वीकार कर साधना की विशिष्ट भूमिका का अनुसरण करता है । श्रमण भूत प्रतिमा में समस्त चर्या साधु के अनुरूप ही होती है । केवल भिक्षा अपने पारिवारिक सदस्यों से स्वीकार करता है।
साधना के प्रयोगों में एक महत्वपूर्ण प्रयोग श्रावक के लिए संलेखना है, जिसे समाधिमरण कहते हैं । श्रावक अन्तिम समय को सन्निकट जान जीवन पर्यन्त भोजन पानी आदि का परित्याग कर क्रमशः रागद्वेष रहित समता की अवस्था में स्थिर होकर करता है, जिसे संलेखना अथवा संथारा भी कहते हैं।
भगवान् महावीर ने आदर्श श्रावक की परिकल्पना के बदले श्रावक के आदर्श को जरूर प्रस्तुत किया था। उनकी दृष्टि में श्रावक का पहला आदर्श समता, दूसरा संयम और तीसरा विवेकपूर्ण व्यवहार है। इन तीन आदर्श बिन्दुओं पर महावीर के श्रावक स्वयं के लिए ही नहीं, अपितु समाज, राष्ट्र एवं विश्व के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो सकते हैं।
खंड ४, अंक ७-८
४५१