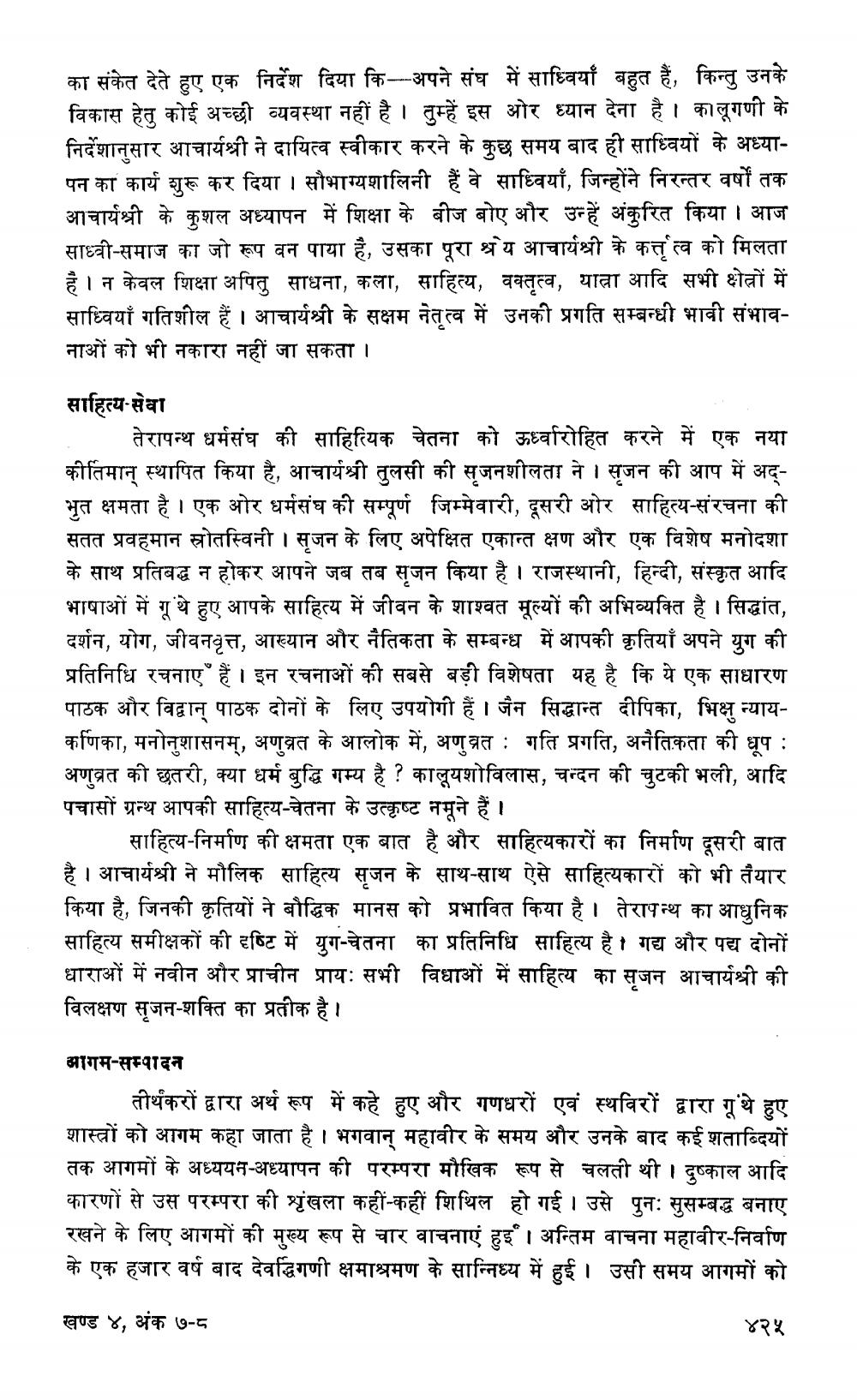________________
का संकेत देते हुए एक निर्देश दिया कि--अपने संघ में साध्वियां बहुत हैं, किन्तु उनके विकास हेतु कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है । तुम्हें इस ओर ध्यान देना है। कालूगणी के निर्देशानुसार आचार्यश्री ने दायित्व स्वीकार करने के कुछ समय बाद ही साध्वियों के अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया । सौभाग्यशालिनी हैं वे साध्वियां, जिन्होंने निरन्तर वर्षों तक आचार्यश्री के कुशल अध्यापन में शिक्षा के बीज बोए और उन्हें अंकुरित किया । आज साध्वी-समाज का जो रूप बन पाया है, उसका पूरा श्रेय आचार्यश्री के कर्तृत्व को मिलता है । न केवल शिक्षा अपितु साधना, कला, साहित्य, वक्तृत्व, यात्रा आदि सभी क्षेत्रों में साध्वियाँ गतिशील हैं । आचार्यश्री के सक्षम नेतृत्व में उनकी प्रगति सम्बन्धी भावी संभावनाओं को भी नकारा नहीं जा सकता।
साहित्य सेवा
तेरापन्थ धर्मसंघ की साहित्यिक चेतना को ऊर्ध्वारोहित करने में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, आचार्यश्री तुलसी की सृजनशीलता ने । सृजन की आप में अद्भुत क्षमता है। एक ओर धर्मसंघ की सम्पूर्ण जिम्मेवारी, दूसरी ओर साहित्य-संरचना की सतत प्रवहमान स्रोतस्विनी । सृजन के लिए अपेक्षित एकान्त क्षण और एक विशेष मनोदशा के साथ प्रतिबद्ध न होकर आपने जब तब सृजन किया है। राजस्थानी, हिन्दी, संस्कृत आदि भाषाओं में गूथे हुए आपके साहित्य में जीवन के शाश्वत मूल्यों की अभिव्यक्ति है । सिद्धांत, दर्शन, योग, जीवनवृत्त, आख्यान और नैतिकता के सम्बन्ध में आपकी कृतियाँ अपने युग की प्रतिनिधि रचनाएं हैं। इन रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये एक साधारण पाठक और विद्वान् पाठक दोनों के लिए उपयोगी हैं । जैन सिद्धान्त दीपिका, भिक्षु न्यायकणिका, मनोनुशासनम्, अणुव्रत के आलोक में, अणुव्रत : गति प्रगति, अनैतिकता की धूप : अणुव्रत की छतरी, क्या धर्म बुद्धि गम्य है ? कालूयशोविलास, चन्दन की चुटकी भली, आदि पचासों ग्रन्थ आपकी साहित्य-चेतना के उत्कृष्ट नमूने हैं।
साहित्य-निर्माण की क्षमता एक बात है और साहित्यकारों का निर्माण दूसरी बात है । आचार्यश्री ने मौलिक साहित्य सृजन के साथ-साथ ऐसे साहित्यकारों को भी तैयार किया है, जिनकी कृतियों ने बौद्धिक मानस को प्रभावित किया है। तेरापन्थ का आधुनिक साहित्य समीक्षकों की दृष्टि में युग-चेतना का प्रतिनिधि साहित्य है। गद्य और पद्य दोनों धाराओं में नवीन और प्राचीन प्रायः सभी विधाओं में साहित्य का सृजन आचार्यश्री की विलक्षण सृजन-शक्ति का प्रतीक है।
आगम-सम्पादन
तीर्थंकरों द्वारा अर्थ रूप में कहे हुए और गणधरों एवं स्थविरों द्वारा गूथे हुए शास्त्रों को आगम कहा जाता है । भगवान् महावीर के समय और उनके बाद कई शताब्दियों तक आगमों के अध्ययन-अध्यापन की परम्परा मौखिक रूप से चलती थी। दुष्काल आदि कारणों से उस परम्परा की शृंखला कहीं-कहीं शिथिल हो गई। उसे पुनः सुसम्बद्ध बनाए रखने के लिए आगमों की मुख्य रूप से चार वाचनाएं हुई । अन्तिम वाचना महावीर-निर्वाण के एक हजार वर्ष बाद देवद्धिगणी क्षमाश्रमण के सान्निध्य में हुई। उसी समय आगमों को
खण्ड ४, अंक ७-८
४२५