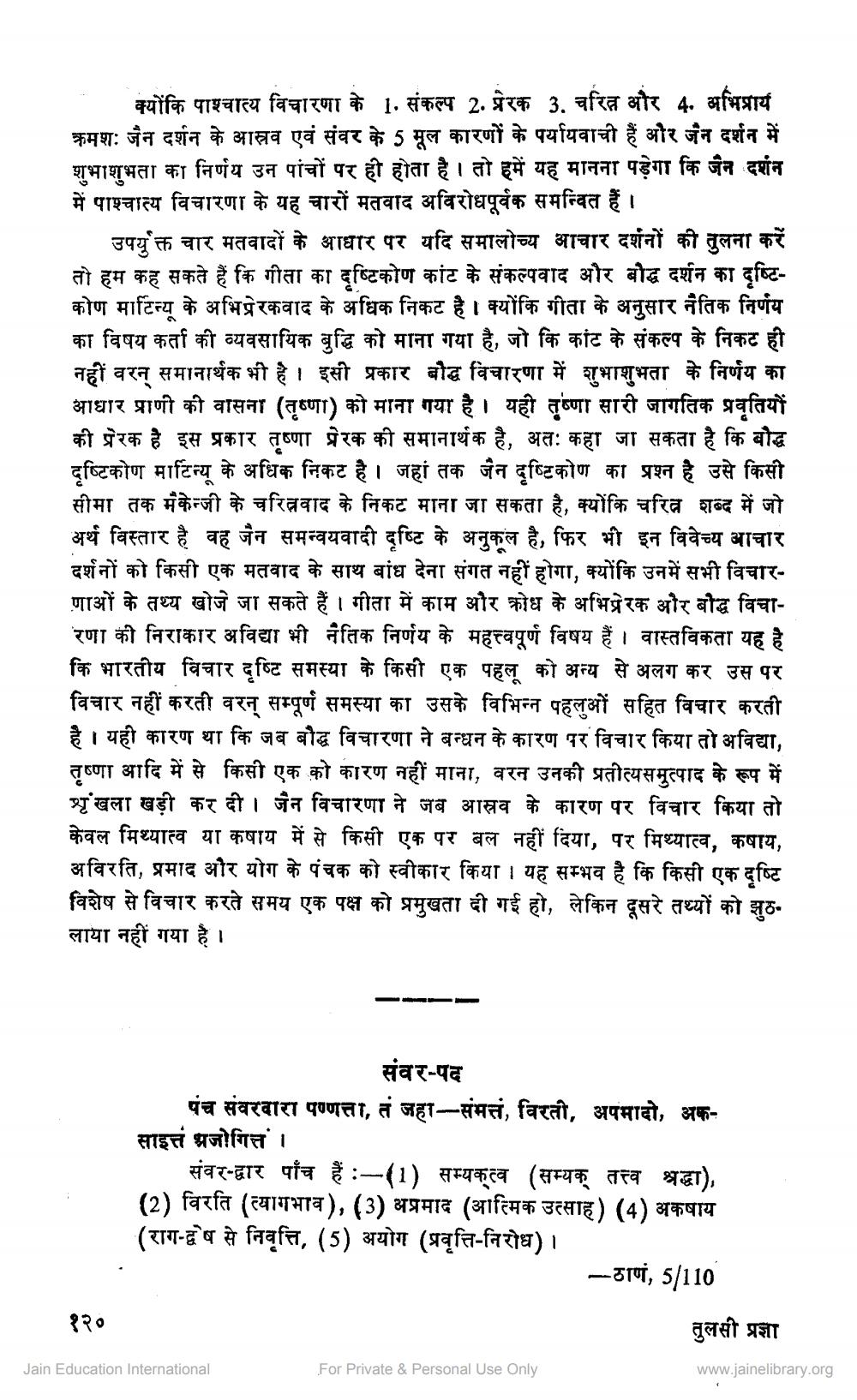________________
क्योंकि पाश्चात्य विचारणा के 1. संकल्प 2. प्रेरक 3. चरित्र और 4. अभिप्राय क्रमशः जैन दर्शन के आस्रव एवं संवर के 5 मूल कारणों के पर्यायवाची हैं और जैन दर्शन में शुभाशुभता का निर्णय उन पांचों पर ही होता है । तो हमें यह मानना पड़ेगा कि जैन दर्शन में पाश्चात्य विचारणा के यह चारों मतवाद अविरोधपूर्वक समन्वित हैं।
उपर्युक्त चार मतवादों के आधार पर यदि समालोच्य आचार दर्शनों की तुलना करें तो हम कह सकते हैं कि गीता का दृष्टिकोण कांट के संकल्पवाद और बौद्ध दर्शन का दृष्टिकोण मार्टिन्यू के अभिप्रेरकवाद के अधिक निकट है । क्योंकि गीता के अनुसार नैतिक निर्णय का विषय कर्ता की व्यवसायिक बुद्धि को माना गया है, जो कि कांट के संकल्प के निकट ही नहीं वरन् समानार्थक भी है। इसी प्रकार बौद्ध विचारणा में शुभाशुभता के निर्णय का आधार प्राणी की वासना (तृष्णा) को माना गया है। यही तृष्णा सारी जागतिक प्रवृतियों की प्रेरक है इस प्रकार तष्णा प्रेरक की समानार्थक है, अत: कहा जा सकता है कि बौद्ध दृष्टिकोण मार्टिन्यू के अधिक निकट है। जहां तक जैन दृष्टिकोण का प्रश्न है उसे किसी सीमा तक मैकेन्जी के चरित्रवाद के निकट माना जा सकता है, क्योंकि चरित्न शब्द में जो अर्थ विस्तार है वह जैन समन्वयवादी दृष्टि के अनुकूल है, फिर भी इन विवेच्य आचार दर्शनों को किसी एक मतवाद के साथ बांध देना संगत नहीं होगा, क्योंकि उनमें सभी विचारणाओं के तथ्य खोजे जा सकते हैं । गीता में काम और क्रोध के अभिप्रेरक और बौद्ध विचारणा की निराकार अविद्या भी नैतिक निर्णय के महत्त्वपूर्ण विषय हैं। वास्तविकता यह है कि भारतीय विचार दृष्टि समस्या के किसी एक पहलू को अन्य से अलग कर उस पर विचार नहीं करती वरन् सम्पूर्ण समस्या का उसके विभिन्न पहलुओं सहित विचार करती है। यही कारण था कि जब बौद्ध विचारणा ने बन्धन के कारण पर विचार किया तो अविद्या, तृष्णा आदि में से किसी एक को कारण नहीं माना, वरन उनकी प्रतीत्यसमुत्पाद के रूप में शृंखला खड़ी कर दी। जैन विचारणा ने जब आस्रव के कारण पर विचार किया तो केवल मिथ्यात्व या कषाय में से किसी एक पर बल नहीं दिया, पर मिथ्यात्व, कषाय, अविरति, प्रमाद और योग के पंचक को स्वीकार किया । यह सम्भव है कि किसी एक दृष्टि विशेष से विचार करते समय एक पक्ष को प्रमुखता दी गई हो, लेकिन दूसरे तथ्यों को झुठलाया नहीं गया है।
संवर-पद पंच संवरवारा पण्णत्ता, तं जहा-संमत्तं, विरती, अपमादो, अकसाइत्तं प्रजोगित्तं ।
संवर-द्वार पाँच हैं :-(1) सम्यक्त्व (सम्यक् तत्त्व श्रद्धा), (2) विरति (त्यागभाव), (3) अप्रमाद (आत्मिक उत्साह) (4) अकषाय (राग-द्वेष से निवृत्ति, (5) अयोग (प्रवृत्ति-निरोध)।
-ठाणं, 5/110
१२०
तुलसी प्रज्ञा
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org