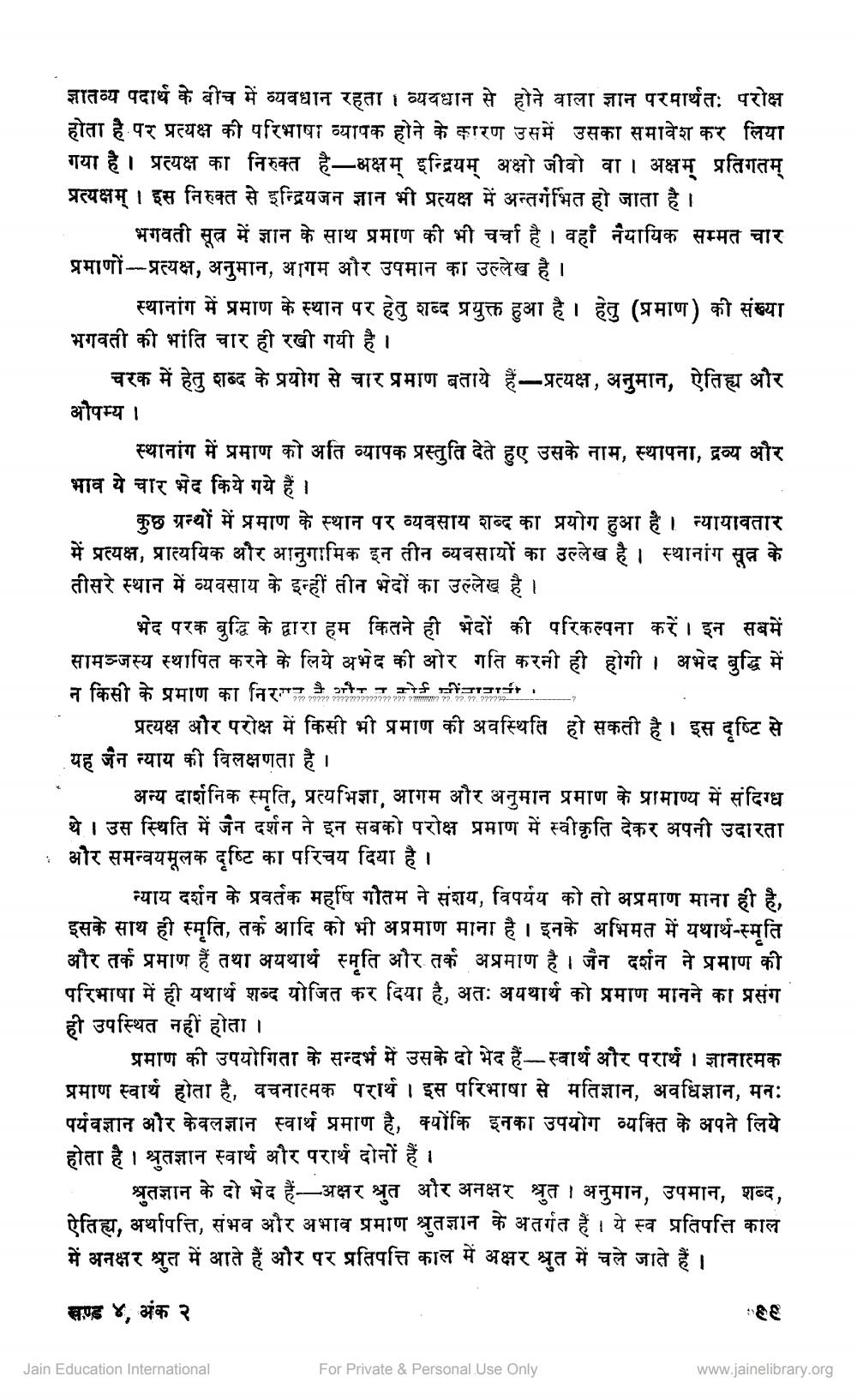________________
ज्ञातव्य पदार्थ के बीच में व्यवधान रहता । व्यवधान से होने वाला ज्ञान परमार्थत: परोक्ष होता है पर प्रत्यक्ष की परिभाषा व्यापक होने के कारण उसमें उसका समावेश कर लिया गया है। प्रत्यक्ष का निरुक्त है—अक्षम् इन्द्रियम् अक्षो जीवो वा। अक्षम् प्रतिगतम् प्रत्यक्षम् । इस निरुक्त से इन्द्रियजन ज्ञान भी प्रत्यक्ष में अन्तर्गभित हो जाता है।
भगवती सूत्र में ज्ञान के साथ प्रमाण की भी चर्चा है। वहाँ नैयायिक सम्मत चार प्रमाणों--प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और उपमान का उल्लेख है ।
स्थानांग में प्रमाण के स्थान पर हेतु शब्द प्रयुक्त हुआ है। हेतु (प्रमाण) की संख्या भगवती की भांति चार ही रखी गयी है।
चरक में हेतु शब्द के प्रयोग से चार प्रमाण बताये हैं-प्रत्यक्ष, अनुमान, ऐतिह्य और औपम्य ।
___ स्थानांग में प्रमाण को अति व्यापक प्रस्तुति देते हुए उसके नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव ये चार भेद किये गये हैं।
कुछ ग्रन्थों में प्रमाण के स्थान पर व्यवसाय शब्द का प्रयोग हुआ है। न्यायावतार में प्रत्यक्ष, प्रात्ययिक और आनुगामिक इन तीन व्यवसायों का उल्लेख है। स्थानांग सूत्र के तीसरे स्थान में व्यवसाय के इन्हीं तीन भेदों का उल्लेख है।
भेद परक बुद्धि के द्वारा हम कितने ही भेदों की परिकल्पना करें। इन सबमें सामञ्जस्य स्थापित करने के लिये अभेद की ओर गति करनी ही होगी। अभेद बुद्धि में न किसी के प्रमाण का निर से भी - कोई मानी।
प्रत्यक्ष और परोक्ष में किसी भी प्रमाण की अवस्थिति हो सकती है। इस दृष्टि से यह जैन न्याय की विलक्षणता है। - अन्य दार्शनिक स्मृति, प्रत्यभिज्ञा, आगम और अनुमान प्रमाण के प्रामाण्य में संदिग्ध
थे। उस स्थिति में जैन दर्शन ने इन सबको परोक्ष प्रमाण में स्वीकृति देकर अपनी उदारता . और समन्वयमूलक दृष्टि का परिचय दिया है।
__न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम ने संशय, विपर्यय को तो अप्रमाण माना ही है, इसके साथ ही स्मृति, तर्क आदि को भी अप्रमाण माना है । इनके अभिमत में यथार्थ-स्मृति
और तर्क प्रमाण हैं तथा अयथार्थ स्मृति और तर्क अप्रमाण है । जैन दर्शन ने प्रमाण की परिभाषा में ही यथार्थ शब्द योजित कर दिया है, अतः अयथार्थ को प्रमाण मानने का प्रसंग ही उपस्थित नहीं होता।
प्रमाण की उपयोगिता के सन्दर्भ में उसके दो भेद हैं- स्वार्थ और परार्थ । ज्ञानात्मक प्रमाण स्वार्थ होता है, वचनात्मक परार्थ । इस परिभाषा से मतिज्ञान, अवधिज्ञान, मनः पर्यवज्ञान और केवलज्ञान स्वार्थ प्रमाण है, क्योंकि इनका उपयोग व्यक्ति के अपने लिये होता है । श्रुतज्ञान स्वार्थ और परार्थ दोनों हैं ।
श्रतज्ञान के दो भेद हैं—अक्षर श्रुत और अनक्षर श्रुत । अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव प्रमाण श्रुतज्ञान के अतर्गत हैं । ये स्व प्रतिपत्ति काल में अनक्षर श्रुत में आते हैं और पर प्रतिपत्ति काल में अक्षर श्रुत में चले जाते हैं।
खण्ड ४, अंक २
Jain Education International
For Private & Personal.Use Only
www.jainelibrary.org