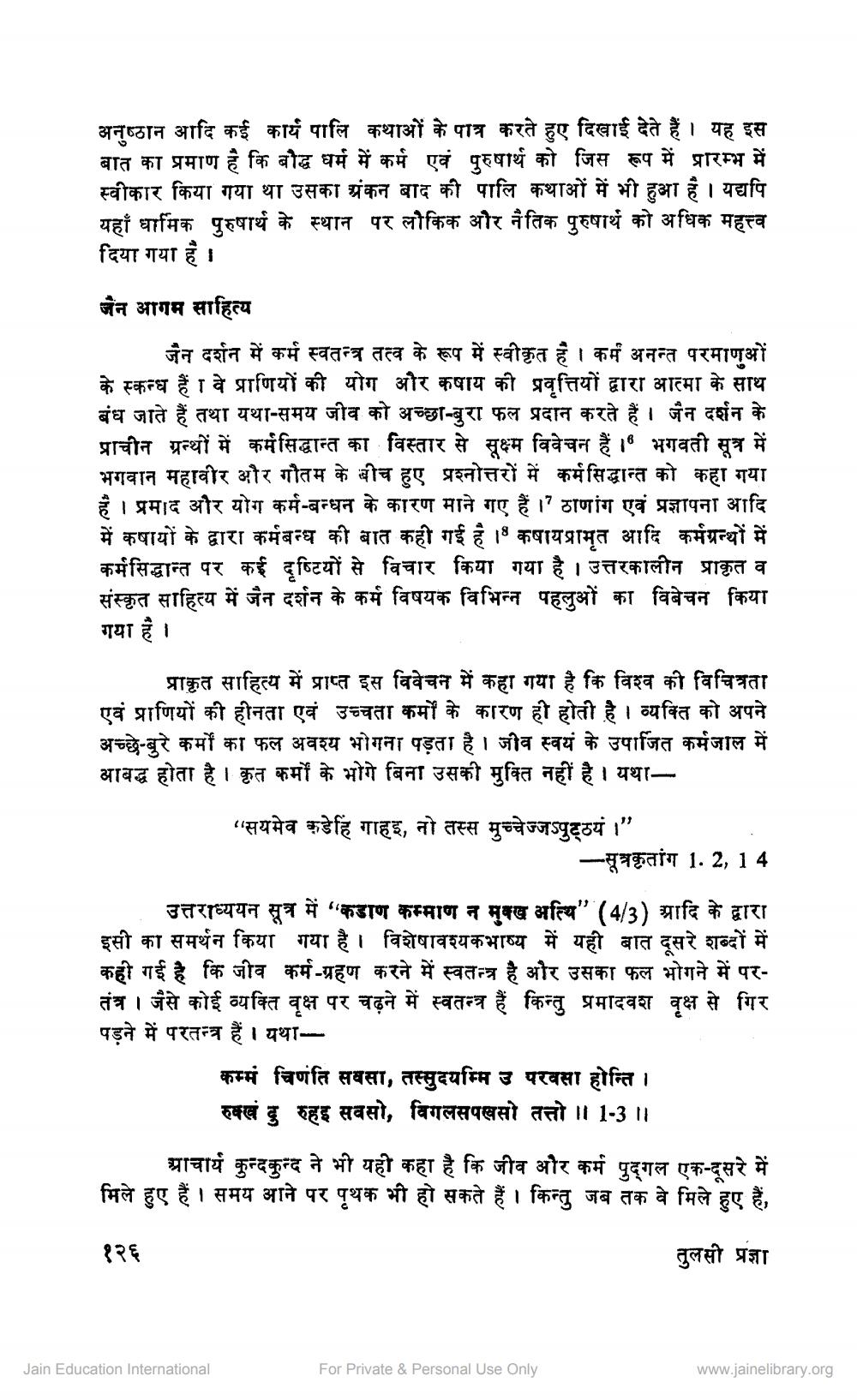________________
अनुष्ठान आदि कई कार्य पालि कथाओं के पात्र करते हुए दिखाई देते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि बौद्ध धर्म में कर्म एवं पुरुषार्थ को जिस रूप में प्रारम्भ में स्वीकार किया गया था उसका अंकन बाद की पालि कथाओं में भी हुआ है । यद्यपि यहाँ धार्मिक पुरुषार्थ के स्थान पर लौकिक और नैतिक पुरुषार्थ को अधिक महत्त्व दिया गया है।
जैन आगम साहित्य
जैन दर्शन में कर्म स्वतन्त्र तत्व के रूप में स्वीकृत है। कर्म अनन्त परमाणुओं के स्कन्ध हैं । वे प्राणियों की योग और कषाय की प्रवृत्तियों द्वारा आत्मा के साथ बंध जाते हैं तथा यथा-समय जीव को अच्छा-बुरा फल प्रदान करते हैं। जैन दर्शन के प्राचीन ग्रन्थों में कर्मसिद्धान्त का विस्तार से सूक्ष्म विवेचन हैं। भगवती सूत्र में भगवान महावीर और गौतम के बीच हुए प्रश्नोत्तरों में कर्म सिद्धान्त को कहा गया है । प्रमाद और योग कर्म-बन्धन के कारण माने गए हैं ।' ठाणांग एवं प्रज्ञापना आदि में कषायों के द्वारा कर्मबन्ध की बात कही गई है । कषायप्रामृत आदि कर्मग्रन्थों में कर्मसिद्धान्त पर कई दृष्टियों से विचार किया गया है । उत्तरकालीन प्राकृत व संस्कृत साहित्य में जैन दर्शन के कर्म विषयक विभिन्न पहलुओं का विबेचन किया गया है।
प्राकृत साहित्य में प्राप्त इस विवेचन में कहा गया है कि विश्व की विचित्रता एवं प्राणियों की हीनता एवं उच्चता कर्मों के कारण ही होती है। व्यक्ति को अपने अच्छे-बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। जीव स्वयं के उपाजित कर्मजाल में आबद्ध होता है । कृत कर्मों के भोगे बिना उसकी मुक्ति नहीं है। यथा
"सयमेव कडेहिं गाहइ, नो तस्स मुच्चेज्जपुठ्ठयं ।"
-सूत्रकृतांग 1. 2, 14
उत्तराध्ययन सूत्र में "कडाण कम्माण न मुक्ख अत्यि" (4/3) आदि के द्वारा इसी का समर्थन किया गया है। विशेषावश्यकभाष्य में यही बात दूसरे शब्दों में कही गई है कि जीव कर्म-ग्रहण करने में स्वतन्त्र है और उसका फल भोगने में परतंत्र । जैसे कोई व्यक्ति वृक्ष पर चढ़ने में स्वतन्त्र हैं किन्तु प्रमादवश वृक्ष से गिर पड़ने में परतन्त्र हैं । यथा
कम्मं चिणंति सवसा, तस्सुदयम्मि उ परवसा होन्ति । रुक्खं दु रुहइ सवसो, विगलसपखसो तत्तो ।। 1-3 ।।
प्राचार्य कुन्दकुन्द ने भी यही कहा है कि जीव और कर्म पुद्गल एक-दूसरे में मिले हुए हैं । समय आने पर पृथक भी हो सकते हैं। किन्तु जब तक वे मिले हुए हैं,
१२६
तुलसी प्रज्ञा
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org