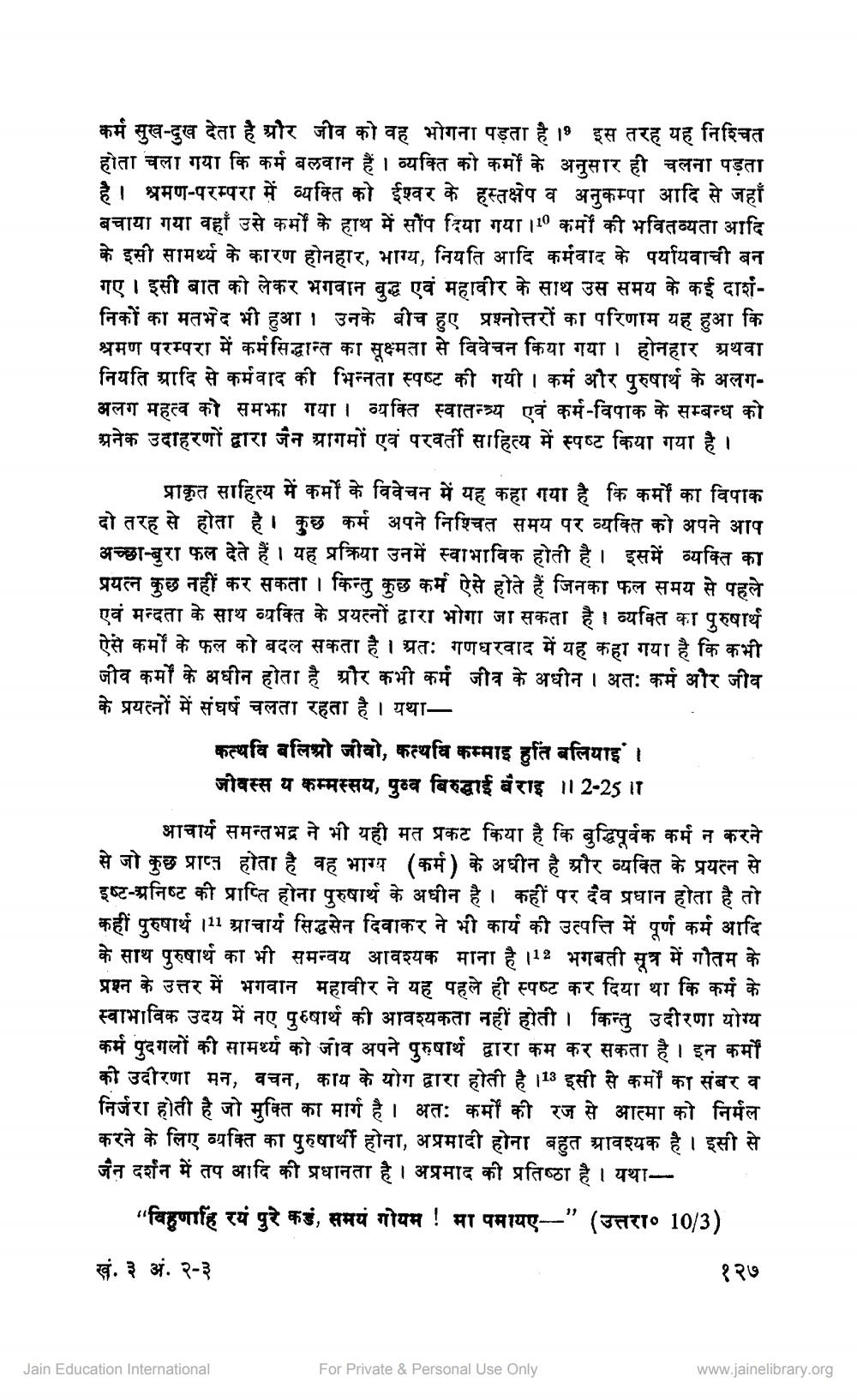________________
।"
इस तरह यह निश्चित अनुसार ही चलना पड़ता
कर्म सुख-दुख देता है और जीव को वह भोगना पड़ता है होता चला गया कि कर्म बलवान हैं । व्यक्ति को कर्मों के है । श्रमण परम्परा में व्यक्ति को ईश्वर के हस्तक्षेप व अनुकम्पा आदि से जहाँ बचाया गया वहाँ उसे कर्मों के हाथ में सौंप दिया गया । 10 कर्मों की भवितव्यता आदि के इसी सामर्थ्य के कारण होनहार, भाग्य, नियति आदि कर्मवाद के पर्यायवाची बन गए । इसी बात को लेकर भगवान बुद्ध एवं महावीर के साथ उस समय के कई दार्शनिकों का मतभेद भी हुआ। उनके बीच हुए प्रश्नोत्तरों का परिणाम यह हुआ कि श्रमण परम्परा में कर्मसिद्धान्त का सूक्ष्मता से विवेचन किया गया । होनहार अथवा नियति आदि से कर्मवाद की भिन्नता स्पष्ट की गयी । कर्म और पुरुषार्थ के अलगअलग महत्व को समझा गया । व्यक्ति स्वातन्त्र्य एवं कर्म विपाक के सम्बन्ध को अनेक उदाहरणों द्वारा जैन आगमों एवं परवर्ती साहित्य में स्पष्ट किया गया है ।
प्राकृत साहित्य में कर्मों के विवेचन में यह कहा गया है कि कर्मों का विपाक दो तरह से होता है । कुछ कर्म अपने निश्चित समय पर व्यक्ति को अपने आप अच्छा-बुरा फल देते हैं । यह प्रक्रिया उनमें स्वाभाविक होती है । इसमें व्यक्ति का प्रयत्न कुछ नहीं कर सकता । किन्तु कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल समय से पहले एवं मन्दता के साथ व्यक्ति के प्रयत्नों द्वारा भोगा जा सकता है । व्यक्ति का पुरुषार्थं ऐसे कर्मों के फल को बदल सकता है । अतः गणधरवाद में यह कहा गया है कि कभी जीव कर्मों के अधीन होता है और कभी कर्म जीव के अधीन । अतः कर्म और जीव के प्रयत्नों में संघर्ष चलता रहता है । यथा—
आचार्य समन्तभद्र ने भी यही मत प्रकट किया है कि बुद्धिपूर्वक कर्म न करने से जो कुछ प्राप्त होता है वह भाग्य (कर्म) के अधीन है और व्यक्ति के प्रयत्न इष्ट-अनिष्ट की प्राप्ति होना पुरुषार्थ के अधीन है । कहीं पर देव प्रधान होता है तो कहीं पुरुषार्थ | 211 प्राचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने भी कार्य की उत्पत्ति में पूर्ण कर्म आदि के साथ पुरुषार्थ का भी समन्वय आवश्यक माना है । 12 भगबती सूत्र में गौतम के प्रश्न के उत्तर में भगवान महावीर ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि कर्म के स्वाभाविक उदय में नए पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होती । किन्तु उदीरणा योग्य कर्म पुदगलों की सामर्थ्य को जीव अपने पुरुषार्थ द्वारा कम कर सकता है । इन कर्मों की उदीरणा मन, वचन, काय के योग द्वारा होती है । 13 इसी से कर्मों का संबर व निर्जरा होती है जो मुक्ति का मार्ग है । अतः कर्मों की रज से आत्मा को निर्मल करने के लिए व्यक्ति का पुरुषार्थी होना, अप्रमादी होना बहुत आवश्यक है । इसी से जैन दर्शन तप आदि की प्रधानता है । अप्रमाद की प्रतिष्ठा है । यथा
"विणाहि रयं पुरे कडं, समयं गोयम ! मा पमायए
खं. ३ अं. २-३
कत्थवि बलिनो जीवो, कत्थवि कम्माइ हुति बलियाई । जीवरस य कम्मस्य, पुण्व बिरुद्धाई बैराइ 11 2-25 17
Jain Education International
31
-
For Private & Personal Use Only
( उत्तरा० 10 / 3 )
१२७
www.jainelibrary.org