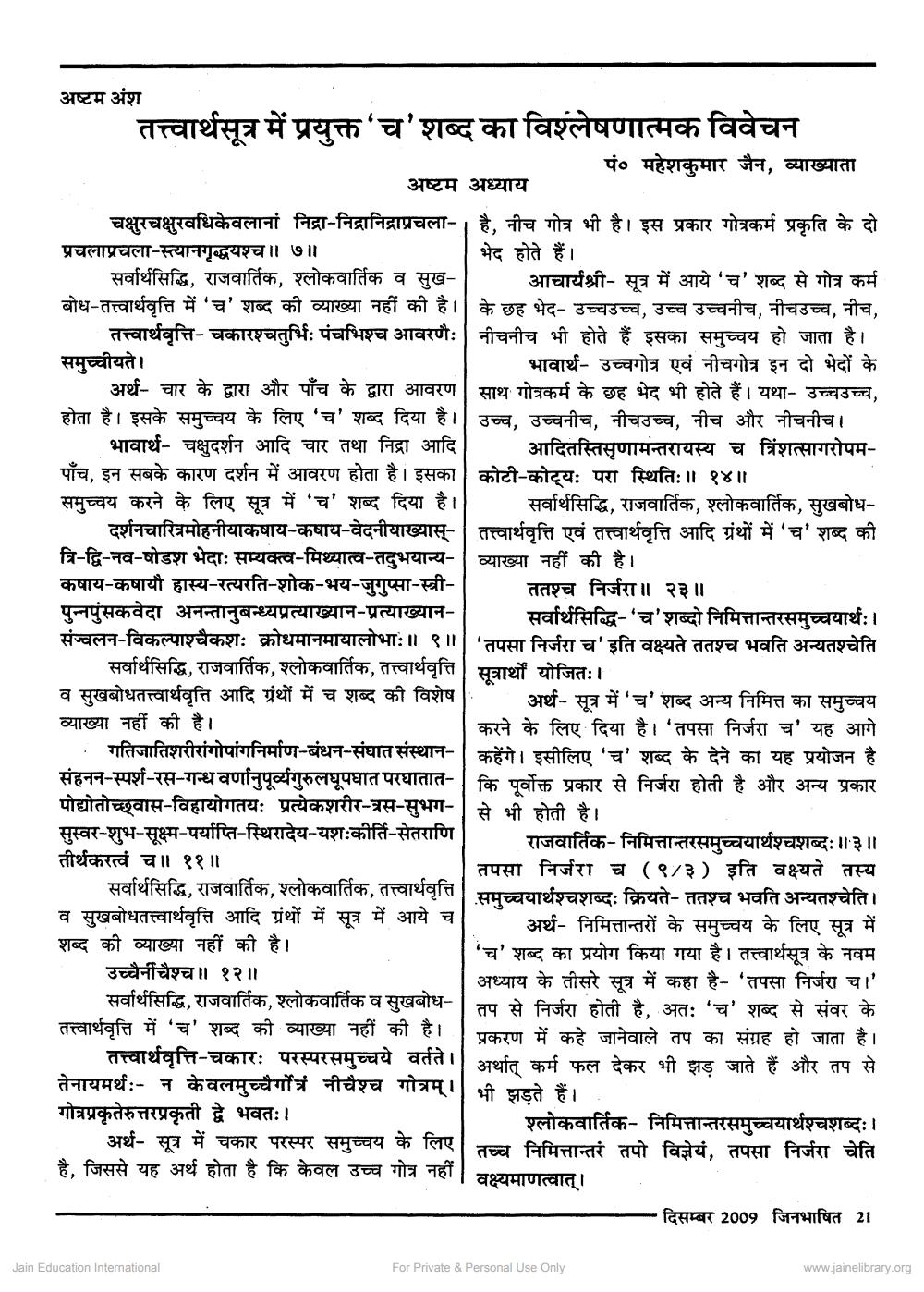________________
अष्टम अंश
तत्त्वार्थसूत्र में प्रयुक्त 'च' शब्द का विश्लेषणात्मक विवेचन
पं० महेशकुमार जैन, व्याख्याता
अष्टम अध्याय
चक्षुरचक्षुरवधिकेवलानां निद्रा-निद्रानिद्राप्रचला प्रचलाप्रचला - स्त्यानगृद्धयश्च ॥ ७॥
सर्वार्थसिद्धि, राजवार्तिक, श्लोकवार्तिक व सुखबोध- तत्त्वार्थवृत्ति में 'च' शब्द की व्याख्या नहीं की है। तत्त्वार्थवृत्ति - चकारश्चतुर्भिः पंचभिश्च आवरणैः समुच्चीयते ।
अर्थ- चार के द्वारा और पाँच के द्वारा आवरण होता है। इसके समुच्चय के लिए 'च' शब्द दिया है।
भावार्थ- चक्षुदर्शन आदि चार तथा निद्रा आदि पाँच, इन सबके कारण दर्शन में आवरण होता है। इसका समुच्चय करने के लिए सूत्र में 'च' शब्द दिया है। दर्शनचारित्रमोहनीयाकषाय- कषाय- वेदनीयाख्यास्त्रि-द्वि-नव - षोडश भेदाः सम्यक्त्व-मिथ्यात्व-तदुभयान्यकषाय- कषायौ हास्य- रत्यरति-शोक-भय- जुगुप्सा - स्त्रीपुन्नपुंसकवेदा अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यान- प्रत्याख्यानसंज्वलन - विकल्पाश्चैकशः क्रोधमानमायालोभाः ॥ ९ ॥ सर्वार्थसिद्धि, राजवार्तिक, श्लोकवार्तिक, तत्त्वार्थवृत्ति व सुखबोधतत्त्वार्थवृत्ति आदि ग्रंथों में च शब्द की विशेष व्याख्या नहीं की है।
गतिजातिशरीरांगोपांगनिर्माण- बंधन- संघात संस्थानसंहनन-स्पर्श-रस-गन्ध वर्णानुपूर्व्यगुरुलघूपघात परघातातपोद्योतोच्छ्वास-विहायोगतयः प्रत्येकशरीर - त्रस - सुभगसुस्वर - शुभ-सूक्ष्म-पर्याप्ति-स्थिरादेय-यशः कीर्ति- सेतराणि तीर्थकरत्वं च ॥ ११॥
सर्वार्थसिद्धि, राजवार्तिक, श्लोकवार्तिक, तत्त्वार्थवृत्ति व सुखबोधतत्त्वार्थवृत्ति आदि ग्रंथों में सूत्र में आये च शब्द की व्याख्या नहीं की है।
उच्चैर्नीचैश्च ॥ १२ ॥
सर्वार्थसिद्धि, राजवार्तिक, श्लोकवार्तिक व सुखबोधतत्त्वार्थवृत्ति में 'च' शब्द की व्याख्या नहीं की है। तत्त्वार्थवृत्ति-चकारः परस्परसमुच्चये वर्तते । तेनायमर्थः- न केवलमुच्चैर्गोत्रं नीचैश्च गोत्रम् गोत्रप्रकृतेरुत्तरप्रकृती द्वे भवतः ।
।
अर्थ- सूत्र में चकार परस्पर समुच्चय के लिए है, जिससे यह अर्थ होता है कि केवल उच्च गोत्र नहीं
Jain Education International
है, नीच गोत्र भी है। इस प्रकार गोत्रकर्म प्रकृति के दो भेद होते हैं।
आचार्यश्री - सूत्र में आये 'च' शब्द से गोत्र कर्म के छह भेद- उच्चउच्च, उच्च उच्चनीच, नीचउच्च, नीच, नीचनीच भी होते हैं इसका समुच्चय हो जाता है।
भावार्थ- उच्चगोत्र एवं नीचगोत्र इन दो भेदों के साथ गोत्रकर्म के छह भेद भी होते हैं। यथा- उच्चउच्च, उच्च, उच्चनीच, नीचउच्च नीच और नीचनीच ।
आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च त्रिंशत्सागरोपमकोटी-कोट्यः परा स्थितिः ॥ १४ ॥
सर्वार्थसिद्धि, राजवार्तिक, श्लोकवार्तिक, सुखबोधतत्त्वार्थवृत्ति एवं तत्त्वार्थवृत्ति आदि ग्रंथों में 'च' शब्द की व्याख्या नहीं की है।
ततश्च निर्जरा ॥ २३ ॥
सर्वार्थसिद्धि - 'च' शब्दो निमित्तान्तरसमुच्चयार्थः । 'तपसा निर्जरा च' इति वक्ष्यते ततश्च भवति अन्यतश्चेति सूत्रार्थों योजितः ।
अर्थ- सूत्र में 'च' शब्द अन्य निमित्त का समुच्चय करने के लिए दिया है। 'तपसा निर्जरा च' यह आगे कहेंगे । इसीलिए 'च' शब्द के देने का यह प्रयोजन है कि पूर्वोक्त प्रकार से निर्जरा होती है और अन्य प्रकार से भी होती है।
राजवार्तिक- निमित्तान्तरसमुच्चयार्थश्चशब्दः ॥ ३॥ तपसा निर्जरा च (९ / ३ ) इति वक्ष्यते तस्य समुच्चयार्थश्चशब्दः क्रियते - ततश्च भवति अन्यतश्चेति।
अर्थ- निमित्तान्तरों के समुच्चय के लिए सूत्र में 'च' शब्द का प्रयोग किया गया है। तत्त्वार्थसूत्र के नवम अध्याय के तीसरे सूत्र में कहा है- 'तपसा निर्जरा च । ' तप से निर्जरा होती है, अतः 'च' शब्द से संवर के प्रकरण में कहे जानेवाले तप का संग्रह हो जाता है। अर्थात् कर्म फल देकर भी झड़ जाते हैं और तप से भी झड़ते हैं।
श्लोकवार्तिक- निमित्तान्तरसमुच्चयार्थश्चशब्दः । तच्च निमित्तान्तरं तपो विज्ञेयं, तपसा निर्जरा चेति वक्ष्यमाणत्वात् ।
For Private & Personal Use Only
दिसम्बर 2009 जिनभाषित 21
www.jainelibrary.org