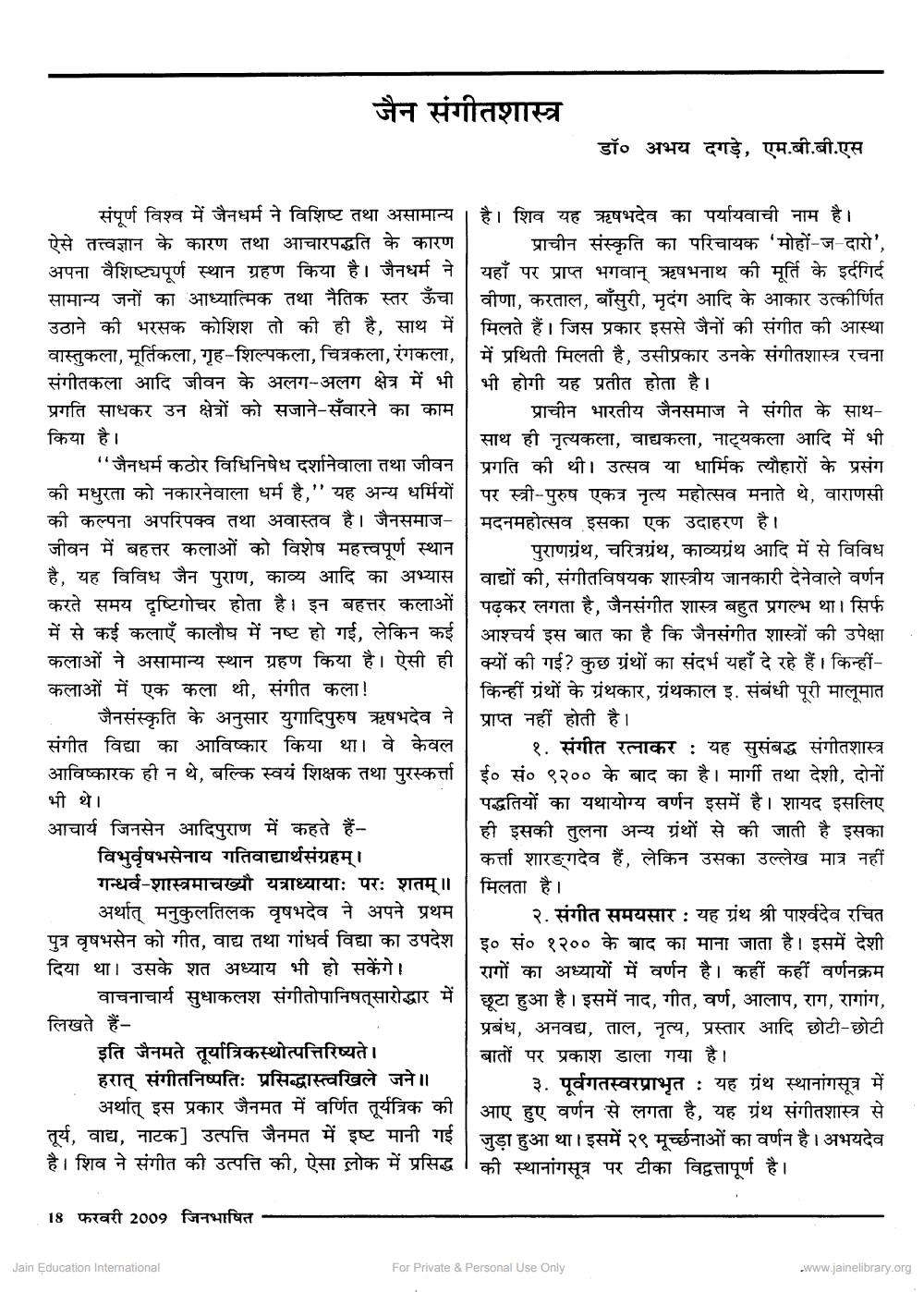________________
संपूर्ण विश्व में जैनधर्म ने विशिष्ट तथा असामान्य ऐसे तत्त्वज्ञान के कारण तथा आचारपद्धति के कारण अपना वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान ग्रहण किया है। जैनधर्म ने सामान्य जनों का आध्यात्मिक तथा नैतिक स्तर ऊँचा उठाने की भरसक कोशिश तो की ही है, साथ में वास्तुकला, मूर्तिकला, गृह- शिल्पकला, चित्रकला, रंगकला संगीतकला आदि जीवन के अलग-अलग क्षेत्र में भी प्रगति साधकर उन क्षेत्रों को सजाने-सँवारने का काम किया है।
जैन संगीतशास्त्र
" जैनधर्म कठोर विधिनिषेध दर्शानेवाला तथा जीवन की मधुरता को नकारनेवाला धर्म है, " यह अन्य धर्मियों की कल्पना अपरिपक्व तथा अवास्तव है। जैनसमाजजीवन में बहत्तर कलाओं को विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान है, यह विविध जैन पुराण, काव्य आदि का अभ्यास करते समय दृष्टिगोचर होता है। इन बहत्तर कलाओं में से कई कलाएँ कालौघ में नष्ट हो गई, लेकिन कई कलाओं ने असामान्य स्थान ग्रहण किया है। ऐसी ही कलाओं में एक कला थी, संगीत कला !
जैनसंस्कृति के अनुसार युगादिपुरुष ऋषभदेव ने संगीत विद्या का आविष्कार किया था। वे केवल आविष्कारक ही न थे, बल्कि स्वयं शिक्षक तथा पुरस्कर्त्ता भी थे।
आचार्य जिनसेन आदिपुराण में कहते हैंविभुर्वृषभसेनाय गतिवाद्यार्थसंग्रहम् ।
गन्धर्व - शास्त्रमाचख्यौ यत्राध्यायाः परः शतम् ॥ अर्थात् मनुकुलतिलक वृषभदेव ने अपने प्रथम पुत्र वृषभसेन को गीत, वाद्य तथा गांधर्व विद्या का उपदेश दिया था। उसके शत अध्याय भी हो सकेंगे।
वाचनाचार्य सुधाकलश संगीतोपानिषत्सारोद्धार में लिखते हैं
इति जैनमते तूर्यात्रिकस्थोत्पत्तिरिष्यते । हरात् संगीतनिष्पतिः प्रसिद्धास्त्वखिले जने ॥ अर्थात् इस प्रकार जैनमत में वर्णित तूर्यत्रिक की सूर्य, वाद्य, नाटक ] उत्पत्ति जैनमत में इष्ट मानी गई है। शिव ने संगीत की उत्पत्ति की, ऐसा लोक में प्रसिद्ध
18 फरवरी 2009 जिनभाषित
Jain Education International
डॉ० अभय दगड़े, एम.बी.बी.एस
है। शिव यह ऋषभदेव का पर्यायवाची नाम है।
प्राचीन संस्कृति का परिचायक 'मोहों-ज- दारो', यहाँ पर प्राप्त भगवान् ऋषभनाथ की मूर्ति के इर्दगिर्द वीणा, करताल, बाँसुरी, मृदंग आदि के आकार उत्कीर्णित मिलते हैं। जिस प्रकार इससे जैनों की संगीत की आस्था में प्रथिती मिलती है, उसीप्रकार उनके संगीतशास्त्र रचना भी होगी यह प्रतीत होता है।
प्राचीन भारतीय जैनसमाज ने संगीत के साथसाथ ही नृत्यकला, वाद्यकला, नाट्यकला आदि में भी प्रगति की थी । उत्सव या धार्मिक त्यौहारों के प्रसंग पर स्त्री-पुरुष एकत्र नृत्य महोत्सव मनाते थे, वाराणसी मदनमहोत्सव इसका एक उदाहरण है।
पुराणग्रंथ, चरित्रग्रंथ, काव्यग्रंथ आदि में से विविध वाद्यों की, संगीतविषयक शास्त्रीय जानकारी देनेवाले वर्णन पढ़कर लगता है, जैनसंगीत शास्त्र बहुत प्रगल्भ था। सिर्फ । आश्चर्य इस बात का है कि जैनसंगीत शास्त्रों की उपेक्षा क्यों की गई? कुछ ग्रंथों का संदर्भ यहाँ दे रहे हैं। किन्हींकिन्हीं ग्रंथों के ग्रंथकार, ग्रंथकाल इ. संबंधी पूरी मालूमात प्राप्त नहीं होती है।
१. संगीत रत्नाकर : यह सुसंबद्ध संगीतशास्त्र ई० सं० १२०० के बाद का है। मार्गी तथा देशी, दोनों पद्धतियों का यथायोग्य वर्णन इसमें है । शायद इसलिए ही इसकी तुलना अन्य ग्रंथों से की जाती है इसका कर्त्ता शारङ्गदेव हैं, लेकिन उसका उल्लेख मात्र नहीं मिलता है।
२. संगीत समयसार यह ग्रंथ श्री पार्श्वदेव रचित इ० सं० १२०० के बाद का माना जाता है। इसमें देशी रागों का अध्यायों में वर्णन है। कहीं कहीं वर्णनक्रम छूटा हुआ है। इसमें नाद, गीत, वर्ण, आलाप, राग, रागांग, प्रबंध, अनवद्य, ताल, नृत्य, प्रस्तार आदि छोटी-छोटी बातों पर प्रकाश डाला गया है।
३. पूर्वगतस्वरप्राभृत: यह ग्रंथ स्थानांगसूत्र में आए हुए वर्णन से लगता है, यह ग्रंथ संगीतशास्त्र से जुड़ा हुआ था। इसमें २९ मूर्च्छनाओं का वर्णन है। अभयदेव की स्थानांगसूत्र पर टीका विद्वत्तापूर्ण है।
।
For Private & Personal Use Only
.www.jainelibrary.org