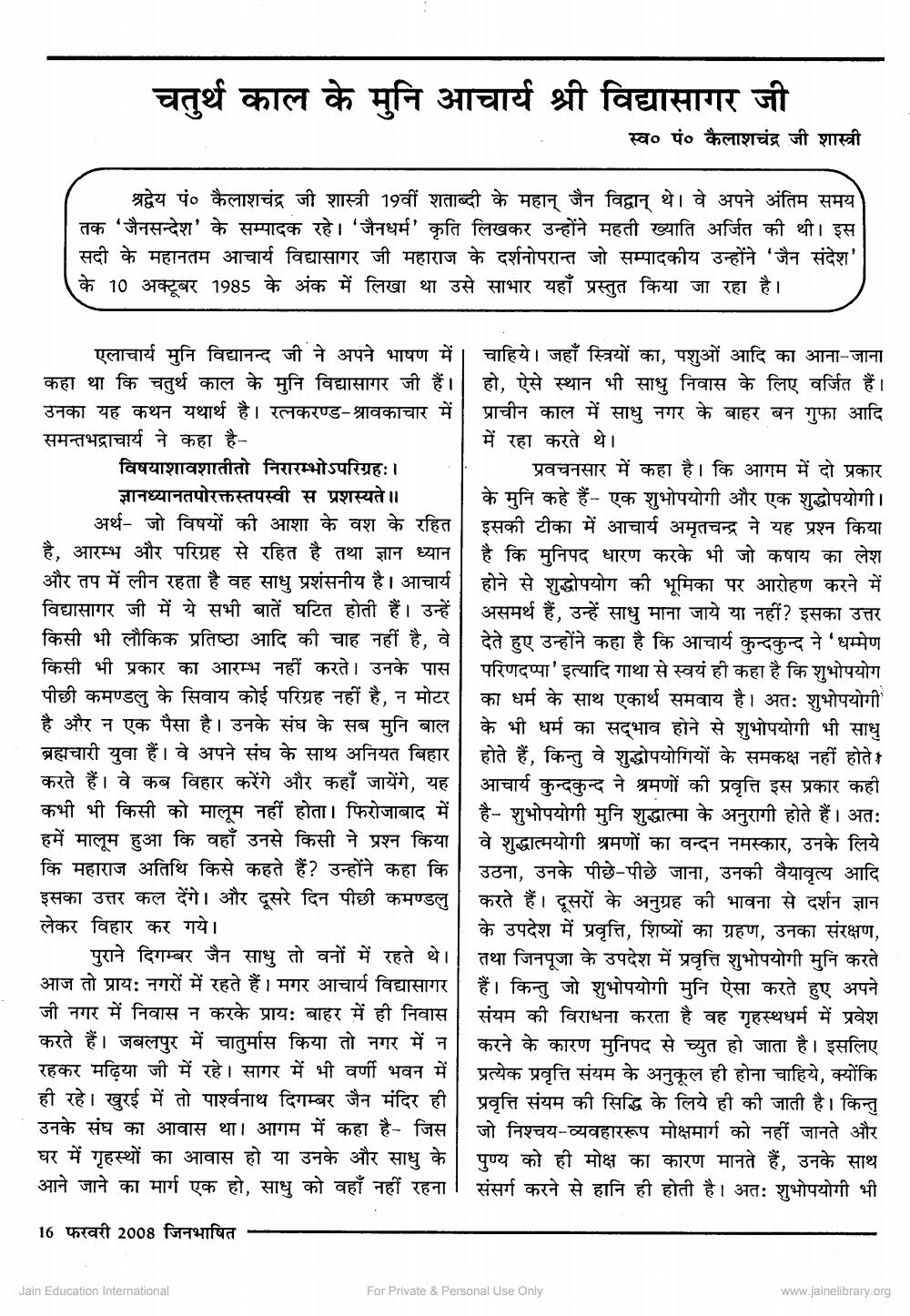________________
चतुर्थ काल के मुनि आचार्य श्री विद्यासागर जी
श्रद्वेय पं० कैलाशचंद्र जी शास्त्री 19वीं शताब्दी के महान् जैन विद्वान् थे । वे अपने अंतिम समय तक 'जैनसन्देश' के सम्पादक रहे। 'जैनधर्म' कृति लिखकर उन्होंने महती ख्याति अर्जित की थी। इस सदी के महानतम आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शनोपरान्त जो सम्पादकीय उन्होंने 'जैन संदेश' के 10 अक्टूबर 1985 के अंक में लिखा था उसे साभार यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा I
एलाचार्य मुनि विद्यानन्द जी ने अपने भाषण में । कहा था कि चतुर्थ काल के मुनि विद्यासागर जी हैं। उनका यह कथन यथार्थ है । रत्नकरण्ड श्रावकाचार में समन्तभद्राचार्य ने कहा है
विषयाशावशातीतो निरारम्भोऽपरिग्रहः । ज्ञानध्यानतपोरक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥
अर्थ- जो विषयों की आशा के वश के रहित है, आरम्भ और परिग्रह से रहित है तथा ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहता है वह साधु प्रशंसनीय है। आचार्य विद्यासागर जी में ये सभी बातें घटित होती हैं। उन्हें किसी भी लौकिक प्रतिष्ठा आदि की चाह नहीं है, वे किसी भी प्रकार का आरम्भ नहीं करते। उनके पास पीछी कमण्डलु के सिवाय कोई परिग्रह नहीं है, न मोटर है और न एक पैसा है। उनके संघ के सब मुनि बाल ब्रह्मचारी युवा हैं। वे अपने संघ के साथ अनियत बिहार करते हैं। वे कब विहार करेंगे और कहाँ जायेंगे, यह कभी भी किसी को मालूम नहीं होता। फिरोजाबाद में हमें मालूम हुआ कि वहाँ उनसे किसी ने प्रश्न किया कि महाराज अतिथि किसे कहते हैं? उन्होंने कहा कि इसका उत्तर कल देंगे । और दूसरे दिन पीछी कमण्डलु लेकर विहार कर गये ।
पुराने दिगम्बर जैन साधु तो वनों में रहते थे । आज तो प्रायः नगरों में रहते हैं। मगर आचार्य विद्यासागर जी नगर में निवास न करके प्रायः बाहर में ही निवास करते हैं। जबलपुर में चातुर्मास किया तो नगर में न रहकर मढ़िया जी में रहे। सागर में भी वर्णी भवन में ही रहे । खुरई में तो पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर ही उनके संघ का आवास था । आगम में कहा है- जिस घर में गृहस्थों का आवास हो या उनके और साधु के आने जाने का मार्ग एक हो, साधु को वहाँ नहीं रहना
16 फरवरी 2008 जिनभाषित
Jain Education International
स्व० पं० कैलाशचंद्र जी शास्त्री
चाहिये । जहाँ स्त्रियों का, पशुओं आदि का आना-जाना हो, ऐसे स्थान भी साधु निवास के लिए वर्जित हैं । प्राचीन काल में साधु नगर के बाहर बन गुफा आदि में रहा करते थे ।
प्रवचनसार में कहा है। कि आगम में दो प्रकार के मुनि कहे हैं- एक शुभोपयोगी और एक शुद्धोपयोगी । इसकी टीका में आचार्य अमृतचन्द्र ने यह प्रश्न किया है कि मुनिपद धारण करके भी जो कषाय का लेश होने से शुद्धोपयोग की भूमिका पर आरोहण करने में असमर्थ हैं, उन्हें साधु माना जाये या नहीं? इसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा है कि आचार्य कुन्दकुन्द ने 'धम्मेण परिणदप्पा' इत्यादि गाथा से स्वयं ही कहा है कि शुभोपयोग का धर्म के साथ एकार्थ समवाय है। अतः शुभोपयोगी के भी धर्म का सद्भाव होने से शुभोपयोगी भी साधु होते हैं, किन्तु वे शुद्धोपयोगियों के समकक्ष नहीं होते। आचार्य कुन्दकुन्द ने श्रमणों की प्रवृत्ति इस प्रकार कही है- शुभोपयोगी मुनि शुद्धात्मा के अनुरागी होते हैं । अतः वे शुद्धात्मयोगी श्रमणों का वन्दन नमस्कार, उनके लिये उठना, उनके पीछे-पीछे जाना, उनकी वैयावृत्य आदि करते हैं। दूसरों के अनुग्रह की भावना से दर्शन ज्ञान के उपदेश में प्रवृत्ति, शिष्यों का ग्रहण, उनका संरक्षण, तथा जिनपूजा के उपदेश में प्रवृत्ति शुभोपयोगी मुनि करते हैं । किन्तु जो शुभोपयोगी मुनि ऐसा करते हुए अपने संयम की विराधना करता है वह गृहस्थधर्म में प्रवेश करने के कारण मुनिपद से च्युत हो जाता है । इसलिए प्रत्येक प्रवृत्ति संयम के अनुकूल ही होना चाहिये, क्योंकि प्रवृत्ति संयम की सिद्धि के लिये ही की जाती है। किन्तु जो निश्चय - व्यवहाररूप मोक्षमार्ग को नहीं जानते और पुण्य को ही मोक्ष का कारण मानते हैं, उनके साथ संसर्ग करने से हानि ही होती है। अतः शुभोपयोगी भी
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org