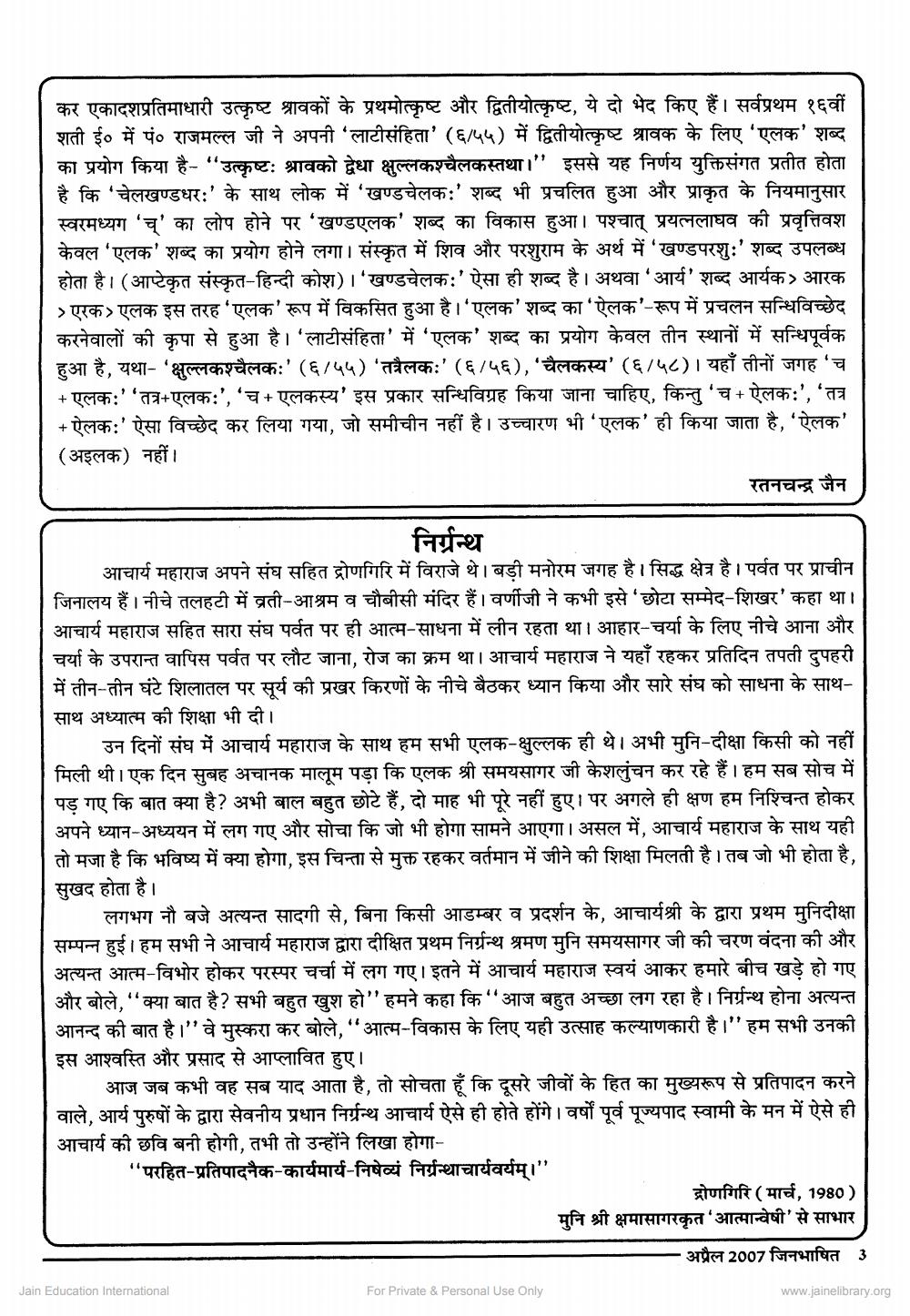________________
कर एकादशप्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावकों के प्रथमोत्कृष्ट और द्वितीयोत्कृष्ट, ये दो भेद किए हैं। सर्वप्रथम १६वीं शती ई० में पं० राजमल्ल जी ने अपनी 'लाटीसंहिता' (६/५५) में द्वितीयोत्कृष्ट श्रावक के लिए 'एलक' शब्द का प्रयोग किया है- "उत्कृष्टः श्रावको द्वेधा क्षुल्लकश्चैलकस्तथा । ' " इससे यह निर्णय युक्तिसंगत प्रतीत होता है कि 'चेलखण्डधरः' के साथ लोक में 'खण्डचेलक : ' शब्द भी प्रचलित हुआ और प्राकृत के नियमानुसार स्वरमध्यग 'च्' का लोप होने पर 'खण्डएलक' शब्द का विकास हुआ। पश्चात् प्रयत्नलाघव की प्रवृत्तिवश केवल 'एलक' शब्द का प्रयोग होने लगा। संस्कृत में शिव और परशुराम के अर्थ में 'खण्डपरशुः' शब्द उपलब्ध होता है । (आप्टेकृत संस्कृत-हिन्दी कोश) । 'खण्डचेलक : ' ऐसा ही शब्द है । अथवा 'आर्य' शब्द आर्यक > आरक > एरक > एलक इस तरह 'एलक' रूप में विकसित हुआ है। 'एलक' शब्द का 'ऐलक' रूप में प्रचलन सन्धिविच्छेद करनेवालों की कृपा से हुआ है । 'लाटीसंहिता' में 'एलक' शब्द का प्रयोग केवल तीन स्थानों में सन्धिपूर्वक हुआ है, यथा- 'क्षुल्लकश्चैलकः' (६/५५) 'तत्रैलकः' (६/५६), 'चैलकस्य' (६/५८) । यहाँ तीनों जगह 'च -एलकः ' 'तत्र+एलकः', 'च + एलकस्य' इस प्रकार सन्धिविग्रह किया जाना चाहिए, किन्तु 'च + ऐलक:', 'तत्र + ऐलक:' ऐसा विच्छेद कर लिया गया, जो समीचीन नहीं है। उच्चारण भी 'एलक' ही किया जाता है, 'ऐलक' (अइलक) नहीं।
+
निर्ग्रन्थ
आचार्य महाराज अपने संघ सहित द्रोणगिरि में विराजे थे। बड़ी मनोरम जगह है। सिद्ध क्षेत्र है । पर्वत पर प्राचीन जिनालय हैं। नीचे तलहटी में व्रती आश्रम व चौबीसी मंदिर हैं। वर्णीजी ने कभी इसे 'छोटा सम्मेद शिखर' कहा था । आचार्य महाराज सहित सारा संघ पर्वत पर ही आत्म-साधना में लीन रहता था । आहार चर्या के लिए नीचे आना और चर्या के उपरान्त वापिस पर्वत पर लौट जाना, रोज का क्रम था । आचार्य महाराज ने यहाँ रहकर प्रतिदिन तपती दुपहरी में तीन-तीन घंटे शिलातल पर सूर्य की प्रखर किरणों के नीचे बैठकर ध्यान किया और सारे संघ को साधना के साथसाथ अध्यात्म की शिक्षा भी दी।
रतनचन्द्र जैन
उन दिनों संघ में आचार्य महाराज के साथ हम सभी एलक- क्षुल्लक ही थे। अभी मुनि दीक्षा किसी को नहीं मिली थी। एक दिन सुबह अचानक मालूम पड़ा कि एलक श्री समयसागर जी केशलुंचन कर रहे हैं। हम सब सोच में पड़ गए कि बात क्या है? अभी बाल बहुत छोटे हैं, दो माह भी पूरे नहीं हुए। पर अगले ही क्षण हम निश्चिन्त होकर अपने ध्यान- अध्ययन में लग गए और सोचा कि जो भी होगा सामने आएगा। असल में, आचार्य महाराज के साथ यही तो मजा है कि भविष्य में क्या होगा, इस चिन्ता से मुक्त रहकर वर्तमान में जीने की शिक्षा मिलती है। तब जो भी होता है, सुखद होता है।
लगभग नौ बजे अत्यन्त सादगी से बिना किसी आडम्बर व प्रदर्शन के, आचार्य श्री के द्वारा प्रथम मुनिदीक्षा सम्पन्न हुई। हम सभी ने आचार्य महाराज द्वारा दीक्षित प्रथम निर्ग्रन्थ श्रमण मुनि समयसागर जी की चरण वंदना की और अत्यन्त आत्म-विभोर होकर परस्पर चर्चा में लग गए। इतने में आचार्य महाराज स्वयं आकर हमारे बीच खड़े हो गए और बोले, "क्या बात है ? सभी बहुत खुश हो" हमने कहा कि " आज बहुत अच्छा लग रहा है। निर्ग्रन्थ होना अत्यन्त आनन्द की बात है ।" वे मुस्करा कर बोले, "आत्म-विकास के लिए यही उत्साह कल्याणकारी है।" हम सभी उनकी इस आश्वस्ति और प्रसाद से आप्लावित हुए ।
आज जब कभी वह सब याद आता है, तो सोचता हूँ कि दूसरे जीवों के हित का मुख्यरूप से प्रतिपादन करने वाले, आर्य पुरुषों के द्वारा सेवनीय प्रधान निर्ग्रन्थ आचार्य ऐसे ही होते होंगे। वर्षों पूर्व पूज्यपाद स्वामी के मन में ऐसे ही आचार्य की छवि बनी होगी, तभी तो उन्होंने लिखा होगा
"परहित प्रतिपादनैक-कार्यमार्य-निषेव्यं निर्ग्रन्थाचार्यवर्यम् ।"
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
द्रोणगिरि ( मार्च, 1980 )
मुनि श्री क्षमासागरकृत 'आत्मान्वेषी' से साभार
अप्रैल 2007 जिनभाषित 3
www.jainelibrary.org