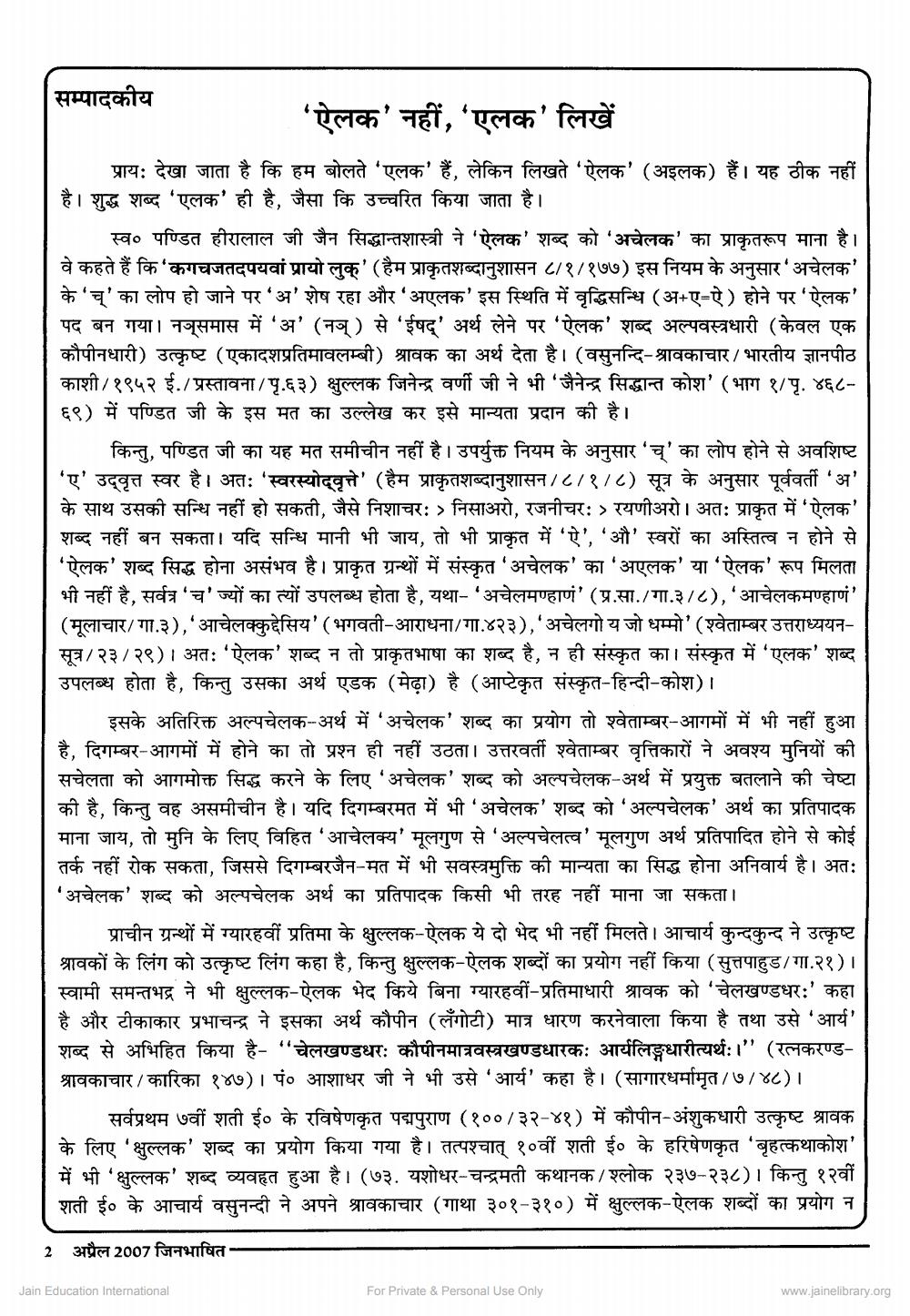________________
सम्पादकीय
'ऐलक' नहीं, 'एलक' लिखें
प्रायः देखा जाता है कि हम बोलते 'एलक' हैं, लेकिन लिखते 'ऐलक' (अइलक) हैं। यह ठीक नहीं है। शुद्ध शब्द 'एलक' ही है, जैसा कि उच्चरित किया जाता है।
___ स्व० पण्डित हीरालाल जी जैन सिद्धान्तशास्त्री ने 'ऐलक' शब्द को 'अचेलक' का प्राकृतरूप माना है। वे कहते हैं कि 'कगचजतदपयवां प्रायो लुक्' (हैम प्राकृतशब्दानुशासन ८/१/१७७) इस नियम के अनुसार 'अचेलक' के 'च' का लोप हो जाने पर 'अ' शेष रहा और 'अएलक' इस स्थिति में वृद्धिसन्धि (अ+ए-ऐ) होने पर 'ऐलक' पद बन गया। नसमास में 'अ' (नञ् ) से 'ईषद्' अर्थ लेने पर 'ऐलक' शब्द अल्पवस्त्रधारी (केवल एक कौपीनधारी) उत्कृष्ट (एकादशप्रतिमावलम्बी) श्रावक का अर्थ देता है। (वसुनन्दि-श्रावकाचार | भारतीय ज्ञानपीठ काशी/१९५२ ई./प्रस्तावना / पृ.६३) क्षुल्लक जिनेन्द्र वर्णी जी ने भी 'जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश' (भाग १/पृ. ४६८६९) में पण्डित जी के इस मत का उल्लेख कर इसे मान्यता प्रदान की है।
किन्तु, पण्डित जी का यह मत समीचीन नहीं है। उपर्युक्त नियम के अनुसार 'च' का लोप होने से अवशिष्ट 'ए' उद्वृत्त स्वर है। अतः 'स्वरस्योवृत्ते' (हैम प्राकृतशब्दानुशासन / ८/१/८) सूत्र के अनुसार पूर्ववर्ती 'अ' के साथ उसकी सन्धि नहीं हो सकती, जैसे निशाचरः > निसाअरो, रजनीचरः > रयणीअरो। अतः प्राकृत में 'ऐलक' शब्द नहीं बन सकता। यदि सन्धि मानी भी जाय, तो भी प्राकृत में 'ऐ', 'औ' स्वरों का अस्तित्व न होने से 'ऐलक' शब्द सिद्ध होना असंभव है। प्राकृत ग्रन्थों में संस्कृत 'अचेलक' का 'अएलक' या 'ऐलक' रूप मिलता भी नहीं है, सर्वत्र 'च' ज्यों का त्यों उपलब्ध होता है, यथा- 'अचेलमण्हाणं' (प्र.सा./गा.३/८), 'आचेलकमण्हाणं' (मूलाचार/ गा.३), 'आचेलक्कुद्देसिय' (भगवती-आराधना/गा.४२३), 'अचेलगो य जो धम्मो' (श्वेताम्बर उत्तराध्ययनसूत्र / २३/२९)। अतः 'ऐलक' शब्द न तो प्राकृतभाषा का शब्द है, न ही संस्कृत का। संस्कृ उपलब्ध होता है, किन्तु उसका अर्थ एडक (मेढ़ा) है (आप्टेकृत संस्कृत-हिन्दी-कोश)। ____ इसके अतिरिक्त अल्पचेलक-अर्थ में 'अचेलक' शब्द का प्रयोग तो श्वेताम्बर-आगमों में भी नहीं हुआ है. दिगम्बर-आगमों में होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उत्तरवर्ती श्वेताम्बर वत्तिकारों ने अवश्य मनियों की सचेलता को आगमोक्त सिद्ध करने के लिए 'अचेलक' शब्द को अल्पचेलक-अर्थ में प्रयुक्त बतलाने की चेष्टा की है, किन्तु वह असमीचीन है। यदि दिगम्बरमत में भी 'अचेलक' शब्द को 'अल्पचेलक' अर्थ का प्रतिपादक माना जाय, तो मुनि के लिए विहित 'आचेलक्य' मूलगुण से 'अल्पचेलत्व' मूलगुण अर्थ प्रतिपादित होने से कोई तर्क नहीं रोक सकता, जिससे दिगम्बरजैन-मत में भी सवस्त्रमुक्ति की मान्यता का सिद्ध होना अनिवार्य है। अतः 'अचेलक' शब्द को अल्पचेलक अर्थ का प्रतिपादक किसी भी तरह नहीं माना जा सकता।
प्राचीन ग्रन्थों में ग्यारहवीं प्रतिमा के क्षुल्लक-ऐलक ये दो भेद भी नहीं मिलते। आचार्य कुन्दकुन्द ने उत्कृष्ट श्रावकों के लिंग को उत्कृष्ट लिंग कहा है, किन्तु क्षुल्लक-ऐलक शब्दों का प्रयोग नहीं किया (सुत्तपाहुड/गा.२१)। स्वामी समन्तभद्र ने भी क्षुल्लक-ऐलक भेद किये बिना ग्यारहवीं-प्रतिमाधारी श्रावक को 'चेलखण्डधरः' कहा है और टीकाकार प्रभाचन्द्र ने इसका अर्थ कौपीन (लँगोटी) मात्र धारण करनेवाला किया है तथा उसे 'आर्य' शब्द से अभिहित किया है- "चेलखण्डधरः कौपीनमात्रवस्त्रखण्डधारकः आर्यलिङ्गधारीत्यर्थः।" (रत्नकरण्डश्रावकाचार / कारिका १४७)। पं० आशाधर जी ने भी उसे 'आर्य' कहा है। (सागारधर्मामृत /७/४८)।
सर्वप्रथम ७वीं शती ई० के रविषेणकृत पद्मपुराण (१०० / ३२-४१) में कौपीन-अंशुकधारी उत्कृष्ट श्रावक के लिए 'क्षुल्लक' शब्द का प्रयोग किया गया है। तत्पश्चात् १०वीं शती ई० के हरिषेणकृत 'बृहत्कथाकोश' में भी 'क्षुल्लक' शब्द व्यवहृत हुआ है। (७३. यशोधर-चन्द्रमती कथानक / श्लोक २३७-२३८)। किन्तु १२वीं शती ई० के आचार्य वसुनन्दी ने अपने श्रावकाचार (गाथा ३०१-३१०) में क्षुल्लक-ऐलक शब्दों का प्रयोग न
2 अप्रैल 2007 जिनभाषित
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org