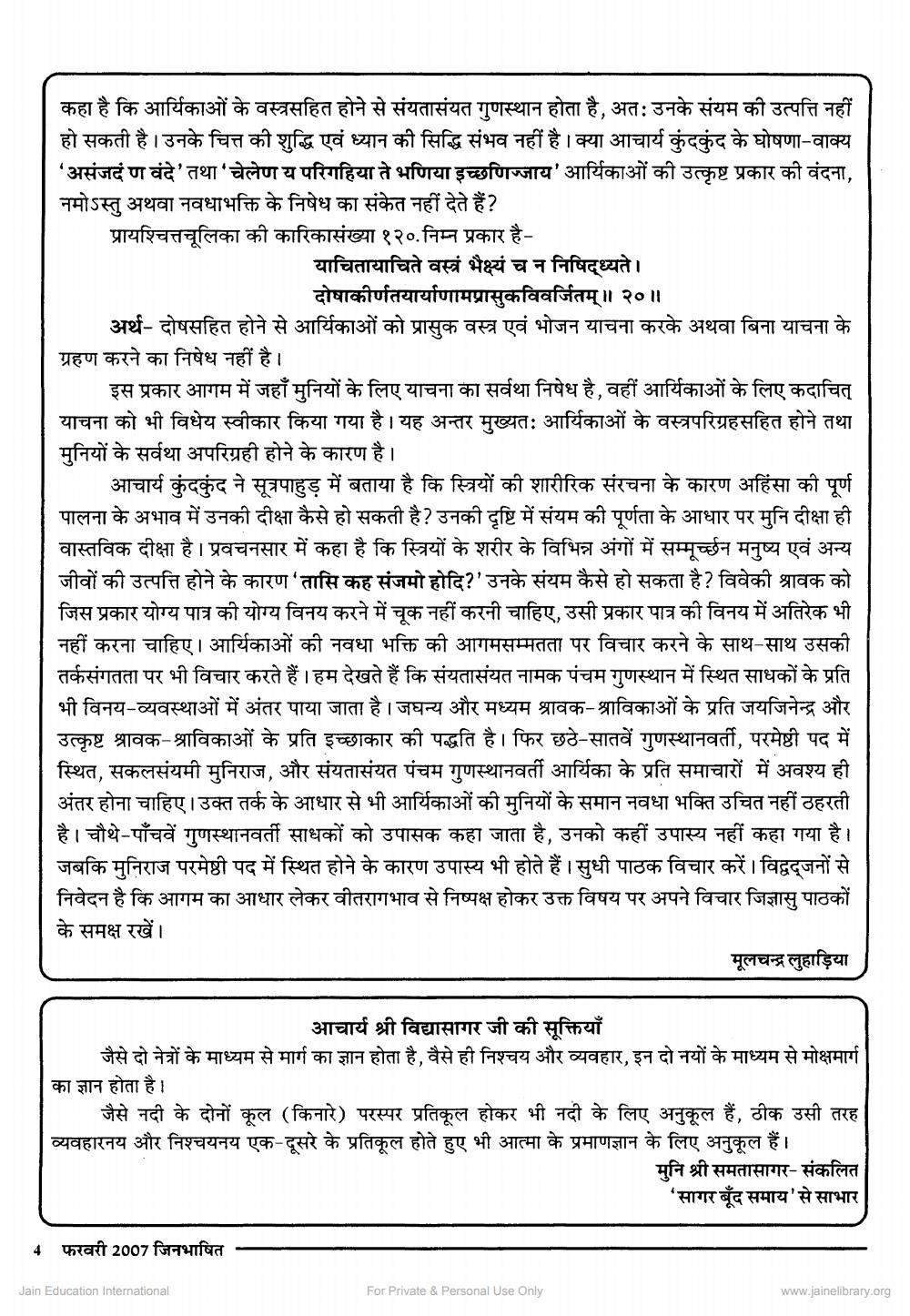________________
कहा है कि आर्यिकाओं के वस्त्रसहित होने से संयतासंयत गुणस्थान होता है, अत: उनके संयम की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। उनके चित्त की शुद्धि एवं ध्यान की सिद्धि संभव नहीं है। क्या आचार्य कुंदकुंद के घोषणा-वाक्य 'असंजदंण वंदे' तथा 'चेलेण य परिगहिया ते भणिया इच्छणिज्जाय' आर्यिकाओं की उत्कृष्ट प्रकार की वंदना, नमोऽस्तु अथवा नवधाभक्ति के निषेध का संकेत नहीं देते हैं? प्रायश्चित्तचूलिका की कारिकासंख्या १२०.निम्न प्रकार है
याचितायाचिते वस्त्रं भैक्ष्यं च न निषिध्यते।
दोषाकीर्णतयार्याणामप्रासुकविवर्जितम्॥ २०॥ अर्थ- दोषसहित होने से आर्यिकाओं को प्रासुक वस्त्र एवं भोजन याचना करके अथवा बिना याचना के ग्रहण करने का निषेध नहीं है।
इस प्रकार आगम में जहाँ मुनियों के लिए याचना का सर्वथा निषेध है, वहीं आर्यिकाओं के लिए कदाचित् याचना को भी विधेय स्वीकार किया गया है। यह अन्तर मुख्यतः आर्यिकाओं के वस्त्रपरिग्रहसहित होने तथा मुनियों के सर्वथा अपरिग्रही होने के कारण है। ___आचार्य कुंदकुंद ने सूत्रपाहुड़ में बताया है कि स्त्रियों की शारीरिक संरचना के कारण अहिंसा की पूर्ण पालना के अभाव में उनकी दीक्षा कैसे हो सकती है? उनकी दृष्टि में संयम की पूर्णता के आधार पर मुनि दीक्षा ही वास्तविक दीक्षा है। प्रवचनसार में कहा है कि स्त्रियों के शरीर के विभिन्न अंगों में सम्मूर्च्छन मनुष्य एवं अन्य जीवों की उत्पत्ति होने के कारण 'तासि कह संजमो होदि?' उनके संयम कैसे हो सकता है? विवेकी श्रावक को जिस प्रकार योग्य पात्र की योग्य विनय करने में चूक नहीं करनी चाहिए, उसी प्रकार पात्र की विनय में अतिरेक भी नहीं करना चाहिए। आर्यिकाओं की नवधा भक्ति की आगमसम्मतता पर विचार करने के साथ-साथ उसकी तर्कसंगतता पर भी विचार करते हैं। हम देखते हैं कि संयतासंयत नामक पंचम गुणस्थान में स्थित साधकों के प्रति भी विनय-व्यवस्थाओं में अंतर पाया जाता है । जघन्य और मध्यम श्रावक-श्राविकाओं के प्रति जयजिनेन्द्र और उत्कृष्ट श्रावक-श्राविकाओं के प्रति इच्छाकार की पद्धति है। फिर छठे-सातवें गुणस्थानवर्ती, परमेष्ठी पद में स्थित, सकलसंयमी मुनिराज, और संयतासंयत पंचम गुणस्थानवर्ती आर्यिका के प्रति समाचारों में अवश्य ही अंतर होना चाहिए। उक्त तर्क के आधार से भी आर्यिकाओं की मुनियों के समान नवधा भक्ति उचित नहीं ठहरती है। चौथे-पाँचवें गुणस्थानवर्ती साधकों को उपासक कहा जाता है, उनको कहीं उपास्य नहीं कहा गया है। जबकि मुनिराज परमेष्ठी पद में स्थित होने के कारण उपास्य भी होते हैं । सुधी पाठक विचार करें। विद्वद्जनों से निवेदन है कि आगम का आधार लेकर वीतरागभाव से निष्पक्ष होकर उक्त विषय पर अपने विचार जिज्ञासु पाठकों के समक्ष रखें।
मूलचन्द्र लुहाड़िया
आचार्य श्री विद्यासागर जी की सूक्तियाँ जैसे दो नेत्रों के माध्यम से मार्ग का ज्ञान होता है, वैसे ही निश्चय और व्यवहार, इन दो नयों के माध्यम से मोक्षमार्ग का ज्ञान होता है।
जैसे नदी के दोनों कूल (किनारे) परस्पर प्रतिकूल होकर भी नदी के लिए अनुकूल हैं, ठीक उसी तरह | व्यवहारनय और निश्चयनय एक-दूसरे के प्रतिकूल होते हुए भी आत्मा के प्रमाणज्ञान के लिए अनुकूल हैं।
मुनि श्री समतासागर-संकलित | 'सागर द समाय' से साभार |
4 फरवरी 2007 जिनभाषित
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org