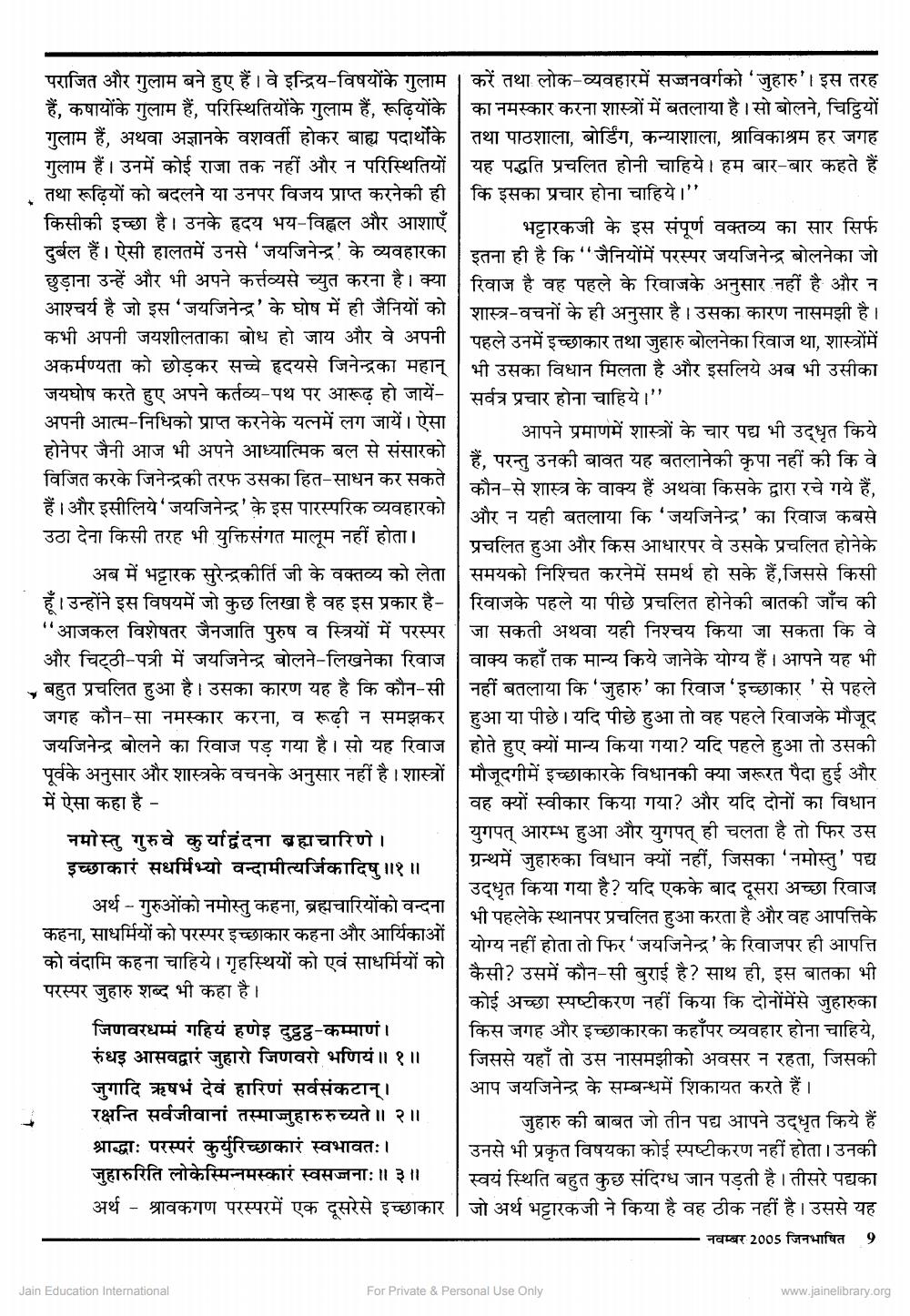________________
+
का नमस्कार करना शास्त्रों में बतलाया है। सो बोलने, चिट्ठियों तथा पाठशाला, बोर्डिंग, कन्याशाला, श्राविकाश्रम हर जगह यह पद्धति प्रचलित होनी चाहिये । हम बार-बार कहते हैं कि इसका प्रचार होना चाहिये । "
पराजित और गुलाम बने हुए हैं। वे इन्द्रिय-विषयोंके गुलाम | करें तथा लोक - व्यवहारमें सज्जनवर्गको 'जुहारु'। इस तरह हैं, कषायोंके गुलाम हैं, परिस्थितियोंके गुलाम हैं, रूढ़ियोंके गुलाम हैं, अथवा अज्ञानके वशवर्ती होकर बाह्य पदार्थोंके गुलाम हैं। उनमें कोई राजा तक नहीं और न परिस्थितियों तथा रूढ़ियों को बदलने या उनपर विजय प्राप्त करनेकी ही किसीकी इच्छा है। उनके हृदय भय-विह्वल और आशाएँ दुर्बल हैं। ऐसी हालत में उनसे 'जयजिनेन्द्र' के व्यवहारका छुड़ाना उन्हें और भी अपने कर्त्तव्यसे च्युत करना है। क्या आश्चर्य है जो इस 'जयजिनेन्द्र' के घोष में ही जैनियों को कभी अपनी जयशीलताका बोध हो जाय और वे अपनी अकर्मण्यता को छोड़कर सच्चे हृदयसे जिनेन्द्रका महान् जयघोष करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ हो जायेंअपनी आत्म-निधिको प्राप्त करनेके यत्नमें लग जायें। ऐसा होनेपर जैनी आज भी अपने आध्यात्मिक बल से संसारको विजित करके जिनेन्द्रकी तरफ उसका हित-साधन कर सकते हैं । और इसीलिये ‘जयजिनेन्द्र' के इस पारस्परिक व्यवहारको उठा देना किसी तरह भी युक्तिसंगत मालूम नहीं होता ।
""
अब में भट्टारक सुरेन्द्रकीर्ति जी के वक्तव्य को लेता हूँ। उन्होंने इस विषयमें जो कुछ लिखा है वह इस प्रकार है'आजकल विशेषतर जैनजाति पुरुष व स्त्रियों में परस्पर और चिट्ठी-पत्री में जयजिनेन्द्र बोलने-लिखनेका रिवाज → बहुत प्रचलित हुआ है। उसका कारण यह है कि कौन-सी जगह कौन-सा नमस्कार करना, व रूढ़ी न समझकर जयजिनेन्द्र बोलने का रिवाज पड़ गया है। सो यह रिवाज पूर्वके अनुसार और शास्त्रके वचनके अनुसार नहीं है। शास्त्रों में ऐसा कहा है -
नमोस्तु गुरुवे कुर्याद्वंदना ब्रह्मचारिणे । इच्छाकारं सधर्मिभ्यो वन्दामीत्यर्जिकादिषु ॥ १ ॥
अर्थ- गुरुओंको नमोस्तु कहना, ब्रह्मचारियोंको वन्दना कहना, साधर्मियों को परस्पर इच्छाकार कहना और आर्यिकाओं को वंदामि कहना चाहिये। गृहस्थियों को एवं साधर्मियों को परस्पर जुहारु शब्द भी कहा है।
जिणवरधम्मं गहियं हणेइ दुट्ठट्ठ-कम्माणं । रुंधइ आसवद्वारं जुहारो जिणवरो भणियं ॥ १ ॥ जुगादि ऋषभं देवं हारिणं सर्वसंकटान् । रक्षन्ति सर्वजीवानां तस्माज्जुहारुरुच्यते ॥ २॥ श्राद्धाः परस्परं कुर्युरिच्छाकारं स्वभावतः । जुहारुरिति लोकेस्मिन्नमस्कारं स्वसज्जनाः ॥ ३ ॥ अर्थ श्रावकगण परस्परमें एक दूसरेसे इच्छाकार
=
Jain Education International
भट्टारकजी के इस संपूर्ण वक्तव्य का सार सिर्फ इतना ही है कि " जैनियोंमें परस्पर जयजिनेन्द्र बोलनेका जो रिवाज है वह पहले के रिवाजके अनुसार नहीं है और न शास्त्र-वचनों के ही अनुसार है। उसका कारण नासमझी है। पहले उनमें इच्छाकार तथा जुहारु बोलनेका रिवाज था, शास्त्रोंमें भी उसका विधान मिलता है और इसलिये अब भी उसीका सर्वत्र प्रचार होना चाहिये।"
आपने प्रमाणमें शास्त्रों के चार पद्य भी उद्धृत किये हैं, परन्तु उनकी बावत यह बतलानेकी कृपा नहीं की कि वे कौन-से शास्त्र के वाक्य अथवा किसके द्वारा रचे गये हैं, और न यही बतलाया कि 'जयजिनेन्द्र' का रिवाज कबसे प्रचलित हुआ और किस आधारपर वे उसके प्रचलित होनेके समयको निश्चित करनेमें समर्थ हो सके हैं, जिससे किसी रिवाजके पहले या पीछे प्रचलित होनेकी बातकी जाँच की जा सकती अथवा यही निश्चय किया जा सकता कि वे वाक्य कहाँ तक मान्य किये जानेके योग्य हैं। आपने यह भी नहीं बतलाया कि 'जुहारु' का रिवाज 'इच्छाकार ' से पहले हुआ या पीछे। यदि पीछे हुआ तो वह पहले रिवाजके मौजूद होते हुए क्यों मान्य किया गया ? यदि पहले हुआ तो उसकी मौजूदगीमें इच्छाकारके विधानकी क्या जरूरत पैदा हुई और वह क्यों स्वीकार किया गया? और यदि दोनों का विधान युगपत् आरम्भ हुआ और युगपत् ही चलता है तो फिर उस ग्रन्थमें जुहारुका विधान क्यों नहीं, जिसका 'नमोस्तु' पद्य उद्धृत किया गया है? यदि एकके बाद दूसरा अच्छा रिवाज भी पहलेके स्थानपर प्रचलित हुआ करता है और वह आपत्ति योग्य नहीं होता तो फिर 'जयजिनेन्द्र' के रिवाजपर ही आपत्ि कैसी? उसमें कौन-सी बुराई है? साथ ही, इस बात का भी कोई अच्छा स्पष्टीकरण नहीं किया कि दोनोंमेंसे जुहारुका किस जगह और इच्छाकारका कहाँपर व्यवहार होना चाहिये, जिससे यहाँ तो उस नासमझीको अवसर न रहता, जिसकी आप जयजिनेन्द्र के सम्बन्धमें शिकायत करते हैं।
जुहा की बाबत जो तीन पद्य आपने उद्धृत किये हैं उनसे भी प्रकृत विषयका कोई स्पष्टीकरण नहीं होता। उनकी स्वयं स्थिति बहुत कुछ संदिग्ध जान पड़ती है। तीसरे पद्यका | जो अर्थ भट्टारकजी ने किया है वह ठीक नहीं है। उससे यह
नवम्बर 2005 जिनभाषित
9
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org