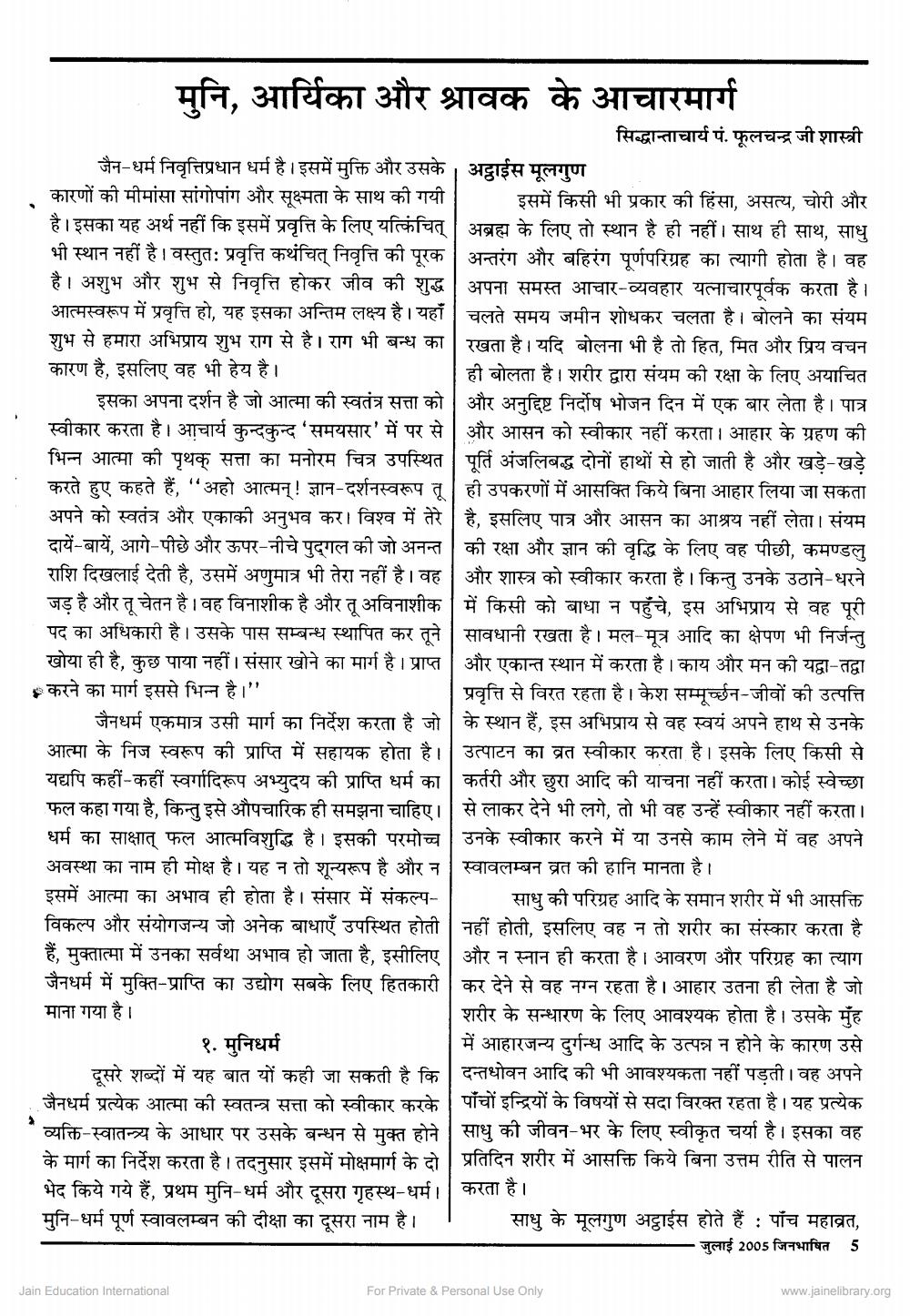________________
"
मुनि, आर्यिका और श्रावक के आचारमार्ग
जैन-धर्म निवृत्तिप्रधान धर्म है। इसमें मुक्ति और उसके । अट्ठाईस मूलगुण कारणों की मीमांसा सांगोपांग और सूक्ष्मता के साथ की गयी है । इसका यह अर्थ नहीं कि इसमें प्रवृत्ति के लिए यत्किंचित् भी स्थान नहीं है। वस्तुतः प्रवृत्ति कथंचित् निवृत्ति की पूरक है। अशुभ और शुभ से निवृत्ति होकर जीव की शुद्ध आत्मस्वरूप में प्रवृत्ति हो, यह इसका अन्तिम लक्ष्य है। यहाँ शुभ से हमारा अभिप्राय शुभ राग से है। राग भी बन्ध का कारण है, इसलिए वह भी हेय है।
इसका अपना दर्शन है जो आत्मा की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार करता है। आचार्य कुन्दकुन्द 'समयसार' में पर से भिन्न आत्मा की पृथक् सत्ता का मनोरम चित्र उपस्थित करते हुए कहते हैं, "अहो आत्मन्! ज्ञान दर्शनस्वरूप तू अपने को स्वतंत्र और एकाकी अनुभव कर । विश्व में तेरे दायें-बायें, आगे-पीछे और ऊपर-नीचे पुद्गल की जो अनन्त राशि दिखलाई देती है, उसमें अणुमात्र भी तेरा नहीं है। वह जड़ है और तू चेतन है। वह विनाशीक है और तू अविनाशीक पद का अधिकारी है। उसके पास सम्बन्ध स्थापित कर तूने खोया ही है, कुछ पाया नहीं। संसार खोने का मार्ग है। प्राप्त * करने का मार्ग इससे भिन्न है । "
जैनधर्म एकमात्र उसी मार्ग का निर्देश करता जो आत्मा के निज स्वरूप की प्राप्ति में सहायक होता है । यद्यपि कहीं-कहीं स्वर्गादिरूप अभ्युदय की प्राप्ति धर्म का फल कहा गया है, किन्तु इसे औपचारिक ही समझना चाहिए। धर्म का साक्षात् फल आत्मविशुद्धि है। इसकी परमोच्च अवस्था का नाम ही मोक्ष है। यह न तो शून्यरूप है और न इसमें आत्मा का अभाव ही होता है। संसार में संकल्पविकल्प और संयोगजन्य जो अनेक बाधाएँ उपस्थित होती हैं, मुक्तात्मा में उनका सर्वथा अभाव हो जाता है, इसीलिए जैनधर्म में मुक्ति - प्राप्ति का उद्योग सबके लिए हितकारी माना गया है।
१. मुनिधर्म
·
दूसरे शब्दों में यह बात यों कही जा सकती है कि . जैनधर्म प्रत्येक आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार करके व्यक्ति-स्वातन्त्र्य के आधार पर उसके बन्धन से मुक्त होने के मार्ग का निर्देश करता है। तदनुसार इसमें मोक्षमार्ग के दो भेद किये गये हैं, प्रथम मुनि-धर्म और दूसरा गृहस्थ-धर्म मुनि-धर्म पूर्ण स्वावलम्बन की दीक्षा का दूसरा नाम है।
Jain Education International
सिद्धान्ताचार्य पं. फूलचन्द्र जी शास्त्री
इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा, असत्य, चोरी और अब्रह्म के लिए तो स्थान है ही नहीं। साथ ही साथ, साधु अन्तरंग और बहिरंग पूर्णपरिग्रह का त्यागी होता है। वह अपना समस्त आचार-व्यवहार यत्नाचारपूर्वक करता है । चलते समय जमीन शोधकर चलता है। बोलने का संयम रखता है। यदि बोलना भी है तो हित, मित और प्रिय वचन ही बोलता है। शरीर द्वारा संयम की रक्षा के लिए अयाचित और अनुद्दिष्ट निर्दोष भोजन दिन में एक बार लेता है। पात्र और आसन को स्वीकार नहीं करता। आहार के ग्रहण की पूर्ति अंजलिबद्ध दोनों हाथों से हो जाती है और खड़े-खड़े ही उपकरणों में आसक्ति किये बिना आहार लिया जा सकता है, इसलिए पात्र और आसन का आश्रय नहीं लेता। संयम की रक्षा और ज्ञान की वृद्धि के लिए वह पीछी, कमण्डलु और शास्त्र को स्वीकार करता है। किन्तु उनके उठाने धरने में किसी को बाधा न पहुँचे, इस अभिप्राय से वह पूरी सावधानी रखता है। मल-मूत्र आदि का क्षेपण भी निर्जन्तु और एकान्त स्थान में करता है। काय और मन की यद्वा-तद्वा प्रवृत्ति से विरत रहता है। केश सम्मूर्च्छन- जीवों की उत्पत्ति के स्थान हैं, इस अभिप्राय से वह स्वयं अपने हाथ से उनके उत्पाटन का व्रत स्वीकार करता है। इसके लिए किसी से कर्तरी और छुरा आदि की याचना नहीं करता। कोई स्वेच्छा से लाकर देने भी लगे, तो भी वह उन्हें स्वीकार नहीं करता । उनके स्वीकार करने में या उनसे काम लेने में वह अपने स्वावलम्बन व्रत की हानि मानता है 1
साधु की परिग्रह आदि के समान शरीर में भी आसक्ति नहीं होती, इसलिए वह न तो शरीर का संस्कार करता है। और न स्नान ही करता है। आवरण और परिग्रह का त्याग कर देने से वह नग्न रहता है। आहार उतना ही लेता है जो शरीर के सन्धारण के लिए आवश्यक होता है। उसके मुँह में आहारजन्य दुर्गन्ध आदि के उत्पन्न न होने के कारण उसे दन्तधोवन आदि की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। वह अपने पाँचों इन्द्रियों के विषयों से सदा विरक्त रहता है। यह प्रत्येक साधु की जीवन-भर के लिए स्वीकृत चर्या है। इसका वह प्रतिदिन शरीर में आसक्ति किये बिना उत्तम रीति से पालन करता है।
साधु के मूलगुण अट्ठाईस होते हैं : पाँच महाव्रत, जुलाई 2005 जिनभाषित
5
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org