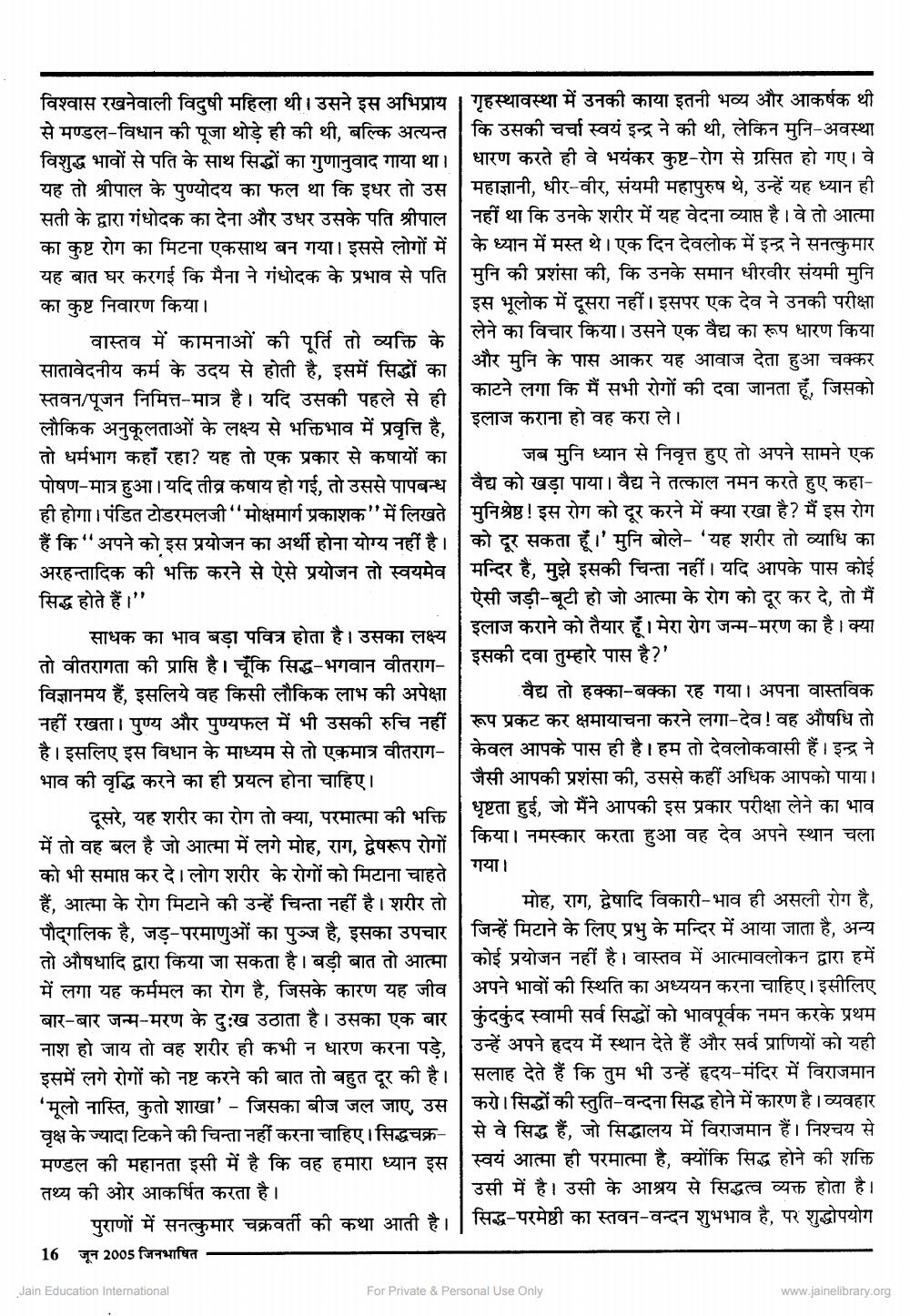________________
विश्वास रखनेवाली विदुषी महिला थी। उसने इस अभिप्राय । गृहस्थावस्था में उनकी काया इतनी भव्य और आकर्षक थी
कि उसकी चर्चा स्वयं इन्द्र ने की थी, लेकिन मुनि अवस्था धारण करते ही वे भयंकर कुष्ट रोग से ग्रसित हो गए। वे महाज्ञानी, धीर-वीर, संयमी महापुरुष थे, उन्हें यह ध्यान नहीं था कि उनके शरीर में यह वेदना व्याप्त है। वे तो आत्मा के ध्यान में मस्त थे। एक दिन देवलोक में इन्द्र ने सनत्कुमार मुनि की प्रशंसा की, कि उनके समान धीरवीर संयमी मुनि इस भूलोक में दूसरा नहीं। इसपर एक देव ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। उसने एक वैद्य का रूप धारण किया और मुनि के पास आकर यह आवाज देता हुआ चक्कर काटने लगा कि मैं सभी रोगों की दवा जानता हूँ, जिसको इलाज कराना हो वह करा ले।
से मण्डल -विधान की पूजा थोड़े ही की थी, बल्कि अत्यन्त विशुद्ध भावों से पति के साथ सिद्धों का गुणानुवाद गाया था। यह तो श्रीपाल के पुण्योदय का फल था कि इधर तो उस सती के द्वारा गंधोदक का देना और उधर उसके पति श्रीपाल काकुष्ट रोग का मिटना एकसाथ बन गया। इससे लोगों में यह बात घर करगई कि मैना ने गंधोदक के प्रभाव से पति का कुष्ट निवारण किया।
वास्तव में कामनाओं की पूर्ति तो व्यक्ति के सातावेदनीय कर्म के उदय से होती है, इसमें सिद्धों का स्तवन / पूजन निमित्त मात्र है । यदि उसकी पहले से ही लौकिक अनुकूलताओं के लक्ष्य से भक्तिभाव में प्रवृत्ति है, तो धर्मभाग कहाँ रहा? यह तो एक प्रकार से कषायों का पोषण - मात्र हुआ। यदि तीव्र कषाय हो गई, तो उससे पापबन्ध ही होगा। पंडित टोडरमलजी "मोक्षमार्ग प्रकाशक" में लिखते हैं कि " अपने को इस प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं है । अरहन्तादिक की भक्ति करने से ऐसे प्रयोजन तो स्वयमेव सिद्ध होते हैं। "
साधक का भाव बड़ा पवित्र होता है । उसका लक्ष्य तो वीतरागता की प्राप्ति है। चूँकि सिद्ध-भगवान वीतरागविज्ञानमय हैं, इसलिये वह किसी लौकिक लाभ की अपेक्षा नहीं रखता। पुण्य और पुण्यफल में भी उसकी रुचि नहीं है । इसलिए इस विधान के माध्यम से तो एकमात्र वीतरागभाव की वृद्धि करने का ही प्रयत्न होना चाहिए ।
दूसरे, यह शरीर का रोग तो क्या, परमात्मा की भक्ति तो वह बल है जो आत्मा में लगे मोह, राग, द्वेषरूप रोगों को भी समाप्त कर दे। लोग शरीर के रोगों को मिटाना चाहते हैं, आत्मा के रोग मिटाने की उन्हें चिन्ता नहीं है। शरीर तो पौद्गलिक है, जड़ - परमाणुओं का पुञ्ज है, इसका उपचार तो औषधादि द्वारा किया जा सकता है। बड़ी बात तो आत्मा में लगा यह कर्ममल का रोग है, जिसके कारण यह जीव बार-बार जन्म-मरण के दुःख उठाता है। उसका एक बार नाश हो जाय तो वह शरीर ही कभी न धारण करना पड़े, इसमें लगे रोगों को नष्ट करने की बात तो बहुत दूर की है। 'मूलो नास्ति, कुतो शाखा' - जिसका बीज जल जाए, उस वृक्ष के ज्यादा टिकने की चिन्ता नहीं करना चाहिए। सिद्धचक्रमण्डल की महानता इसी में है कि वह हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करता है ।
पुराणों में सनत्कुमार चक्रवर्ती की कथा आती है। 16 जून 2005 जिनभाषित
Jain Education International
जब मुनि ध्यान से निवृत्त हुए तो अपने सामने एक वैद्य को खड़ा पाया। वैद्य ने तत्काल नमन करते हुए कहामुनिश्रेष्ठ ! इस रोग को दूर करने में क्या रखा है ? मैं इस रोग को दूर सकता हूँ।' मुनि बोले- 'यह शरीर तो व्याधि का मन्दिर हैं, मुझे इसकी चिन्ता नहीं। यदि आपके पास कोई ऐसी जड़ी-बूटी हो जो आत्मा के रोग को दूर कर दे, तो मैं इलाज कराने को तैयार हूँ। मेरा रोग जन्म-मरण का है। क्या इसकी दवा तुम्हारे पास है ? '
वैद्य तो हक्का-बक्का रह गया। अपना वास्तविक रूप प्रकट कर क्षमायाचना करने लगा-देव ! वह औषधि तो केवल आपके पास ही है। हम तो देवलोकवासी हैं । इन्द्र ने जैसी आपकी प्रशंसा की, उससे कहीं अधिक आपको पाया। धृष्टता हुई, जो मैंने आपकी इस प्रकार परीक्षा लेने का भाव किया । नमस्कार करता हुआ वह देव अपने स्थान चला
गया।
मोह, राग, द्वेषादि विकारी भाव ही असली रोग है, जिन्हें मिटाने के लिए प्रभु के मन्दिर में आया जाता है, अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। वास्तव में आत्मावलोकन द्वारा हमें अपने भावों की स्थिति का अध्ययन करना चाहिए । इसीलिए कुंदकुंद स्वामी सर्व सिद्धों को भावपूर्वक नमन करके प्रथम उन्हें अपने हृदय में स्थान देते हैं और सर्व प्राणियों को यही सलाह देते हैं कि तुम भी उन्हें हृदय-मंदिर में विराजमान करो । सिद्धों की स्तुति-वन्दना सिद्ध होने में कारण है । व्यवहार से वे सिद्ध हैं, जो सिद्धालय में विराजमान हैं। निश्चय से स्वयं आत्मा ही परमात्मा है, क्योंकि सिद्ध होने की शक्ति उसी में है । उसी के आश्रय से सिद्धत्व व्यक्त होता है। सिद्ध-परमेष्ठी का स्तवन - वन्दन शुभभाव है, पर शुद्धोपयोग
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org