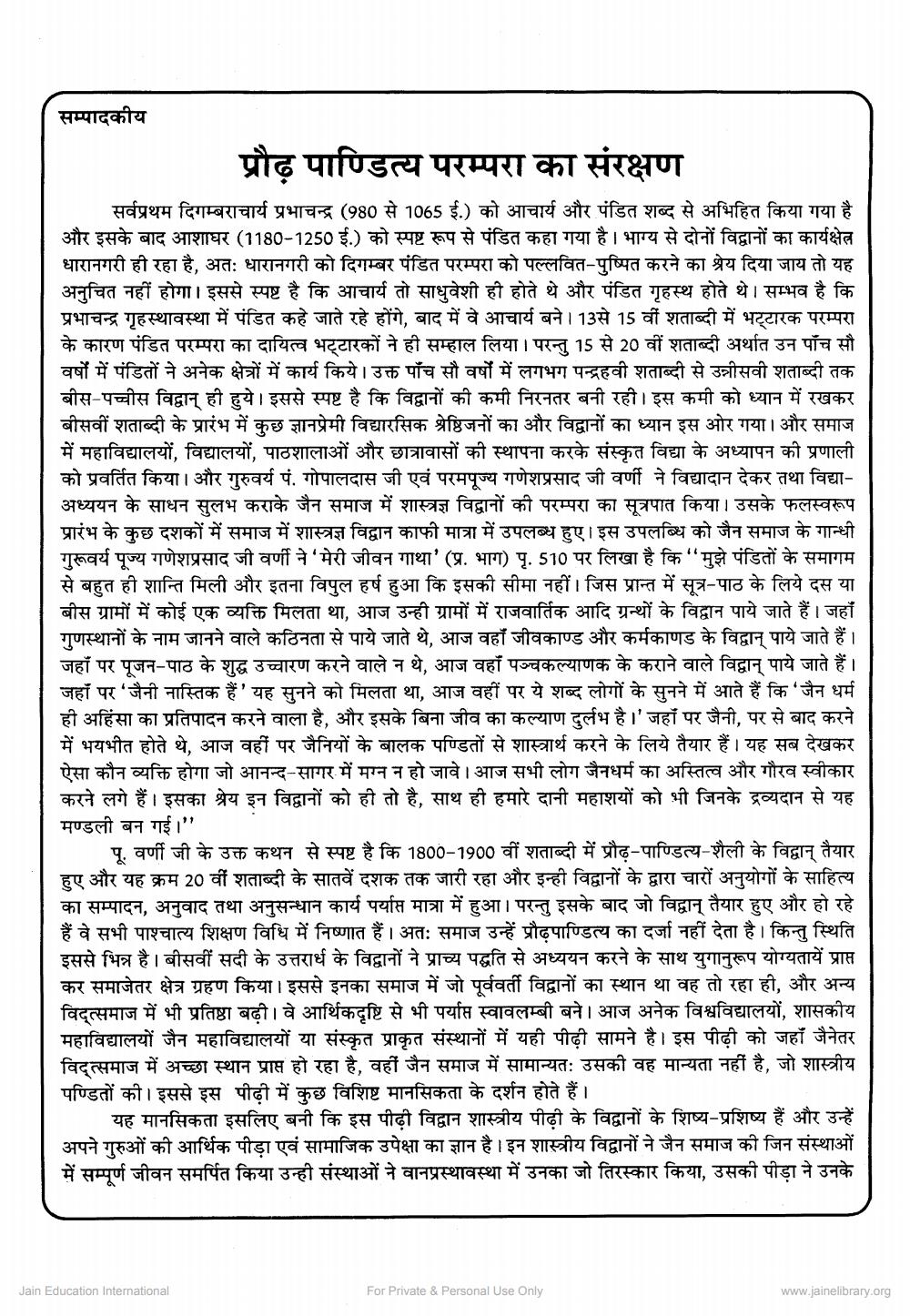________________
सम्पादकीय
प्रौढ़ पाण्डित्य परम्परा का संरक्षण
सर्वप्रथम दिगम्बराचार्य प्रभाचन्द्र (980 से 1065 ई.) को आचार्य और पंडित शब्द से अभिहित किया गया है और इसके बाद आशाघर (1180-1250 ई.) को स्पष्ट रूप से पंडित कहा गया है। भाग्य से दोनों विद्वानों का कार्यक्षेत्र धारानगरी ही रहा है, अत: धारानगरी को दिगम्बर पंडित परम्परा को पल्लवित-पुष्पित करने का श्रेय दिया जाय तो यह अनुचित नहीं होगा। इससे स्पष्ट है कि आचार्य तो साधुवेशी ही होते थे और पंडित गृहस्थ होते थे। सम्भव है कि प्रभाचन्द्र गृहस्थावस्था में पंडित कहे जाते रहे होंगे, बाद में वे आचार्य बने। 13से 15 वीं शताब्दी में भट्टारक परम्परा के कारण पंडित परम्परा का दायित्व भट्टारकों ने ही सम्हाल लिया। परन्तु 15 से 20 वीं शताब्दी अर्थात उन पाँच सौ वर्षों में पंडितों ने अनेक क्षेत्रों में कार्य किये। उक्त पाँच सौ वर्षों में लगभग पन्द्रहवी शताब्दी से उन्नीसवी शताब्दी तक बीस-पच्चीस विद्वान् ही हुये। इससे स्पष्ट है कि विद्वानों की कमी निरनतर बनी रही। इस कमी को ध्यान में रखकर बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ ज्ञानप्रेमी विद्यारसिक श्रेष्ठिजनों का और विद्वानों का ध्यान इस ओर गया। और समाज में महाविद्यालयों, विद्यालयों, पाठशालाओं और छात्रावासों की स्थापना करके संस्कृत विद्या के अध्यापन की प्रणाली को प्रवर्तित किया। और गुरुवर्य पं. गोपालदास जी एवं परमपूज्य गणेशप्रसाद जी वर्णी ने विद्यादान देकर तथा विद्याअध्ययन के साधन सुलभ कराके जैन समाज में शास्त्रज्ञ विद्वानों की परम्परा का सूत्रपात किया। उसके फलस्वरूप प्रारंभ के कुछ दशकों में समाज में शास्त्रज्ञ विद्वान काफी मात्रा में उपलब्ध हुए। इस उपलब्धि को जैन समाज के गान्धी गुरूवर्य पूज्य गणेशप्रसाद जी वर्णी ने 'मेरी जीवन गाथा' (प्र. भाग) पृ. 510 पर लिखा है कि "मुझे पंडितों के समागम से बहुत ही शान्ति मिली और इतना विपुल हर्ष हुआ कि इसकी सीमा नहीं। जिस प्रान्त में सूत्र-पाठ के लिये दस या बीस ग्रामों में कोई एक व्यक्ति मिलता था, आज उन्ही ग्रामों में राजवार्तिक आदि ग्रन्थों के विद्वान पाये जाते हैं। जहाँ गुणस्थानों के नाम जानने वाले कठिनता से पाये जाते थे, आज वहाँ जीवकाण्ड और कर्मकाणड के विद्वान् पाये जाते हैं। जहाँ पर पूजन-पाठ के शुद्ध उच्चारण करने वाले न थे, आज वहाँ पञ्चकल्याणक के कराने वाले विद्वान् पाये जाते हैं। जहाँ पर 'जैनी नास्तिक हैं' यह सुनने को मिलता था, आज वहीं पर ये शब्द लोगों के सुनने में आते हैं कि 'जैन धर्म ही अहिंसा का प्रतिपादन करने वाला है, और इसके बिना जीव का कल्याण दुर्लभ है।' जहाँ पर जैनी, पर से बाद करने में भयभीत होते थे, आज वहीं पर जैनियों के बालक पण्डितों से शास्त्रार्थ करने के लिये तैयार हैं। यह सब देखकर ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो आनन्द-सागर में मग्न न हो जावे। आज सभी लोग जैनधर्म का अस्तित्व और गौरव स्वीकार करने लगे हैं। इसका श्रेय इन विद्वानों को ही तो है, साथ ही हमारे दानी महाशयों को भी जिनके द्रव्यदान से यह मण्डली बन गई।"
पू. वर्णी जी के उक्त कथन से स्पष्ट है कि 1800-1900 वीं शताब्दी में प्रौढ़-पाण्डित्य-शैली के विद्वान् तैयार हुए और यह क्रम 20 वीं शताब्दी के सातवें दशक तक जारी रहा और इन्ही विद्वानों के द्वारा चारों अनुयोगों के साहित्य का सम्पादन, अनुवाद तथा अनुसन्धान कार्य पर्याप्त मात्रा में हुआ। परन्तु इसके बाद जो विद्वान् तैयार हुए और हो रहे हैं वे सभी पाश्चात्य शिक्षण विधि में निष्णात हैं। अतः समाज उन्हें प्रौढ़पाण्डित्य का दर्जा नहीं देता है। किन्तु स्थिति इससे भिन्न है। बीसवीं सदी के उत्तरार्ध के विद्वानों ने प्राच्य पद्धति से अध्ययन करने के साथ युगानुरूप योग्यतायें प्राप्त कर समाजेतर क्षेत्र ग्रहण किया। इससे इनका समाज में जो पूर्ववर्ती विद्वानों का स्थान था वह तो रहा ही, और अन्य विद्त्समाज में भी प्रतिष्ठा बढ़ी। वे आर्थिकदृष्टि से भी पर्याप्त स्वावलम्बी बने। आज अनेक विश्वविद्यालयों, शासकीय महाविद्यालयों जैन महाविद्यालयों या संस्कृत प्राकृत संस्थानों में यही पीढ़ी सामने है। इस पीढ़ी को जहाँ जैनेतर विद्त्समाज में अच्छा स्थान प्राप्त हो रहा है, वहीं जैन समाज में सामान्यतः उसकी वह मान्यता नहीं है, जो शास्त्रीय पण्डितों की। इससे इस पीढ़ी में कुछ विशिष्ट मानसिकता के दर्शन होते हैं।
यह मानसिकता इसलिए बनी कि इस पीढ़ी विद्वान शास्त्रीय पीढ़ी के विद्वानों के शिष्य-प्रशिष्य हैं और उन्हें अपने गरुओं की आर्थिक पीड़ा एवं सामाजिक उपेक्षा का ज्ञान है। इन शास्त्रीय विद्वानों ने जैन समाज की जिन संस्थाओं में सम्पूर्ण जीवन समर्पित किया उन्ही संस्थाओं ने वानप्रस्थावस्था में उनका जो तिरस्कार किया, उ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org