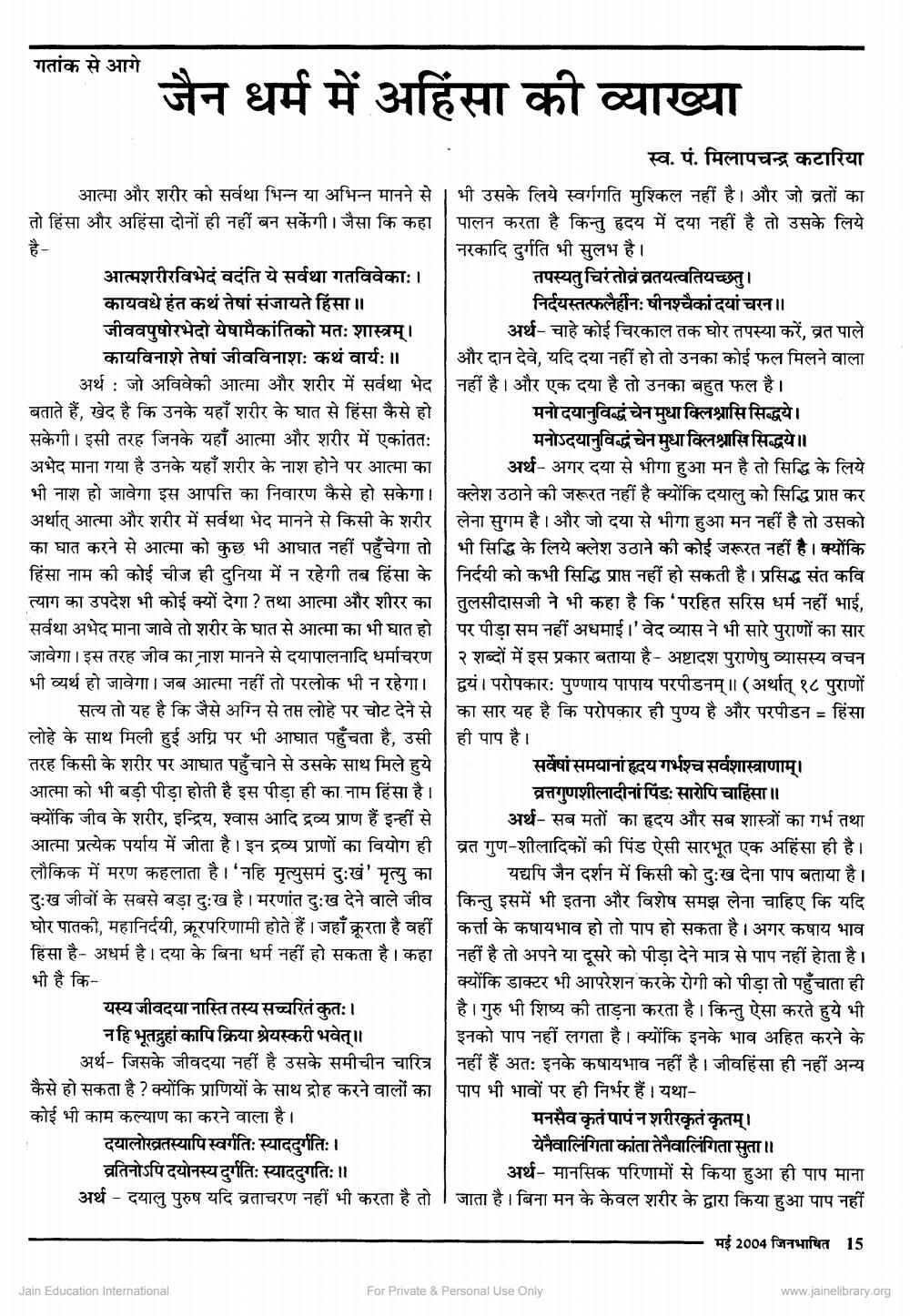________________
गतांक से आगे
जैन धर्म में अहिंसा की व्याख्या
आत्मा और शरीर को सर्वथा भिन्न या अभिन्न मानने से तो हिंसा और अहिंसा दोनों ही नहीं बन सकेंगी। जैसा कि कहा है
आत्मशरीरविभेदं वदंति ये सर्वथा गतविवेकाः । कायवधे हंत कथं तेषां संजायते हिंसा ॥ जीववपुषोरभेदो येषामैकांतिको मतः शास्त्रम् । कायविनाशे तेषां जीवविनाशः कथं वार्यः ॥ अर्थ : जो अविवेकी आत्मा और शरीर में सर्वथा भेद बताते हैं, खेद है कि उनके यहाँ शरीर के घात से हिंसा कैसे हो सकेगी। इसी तरह जिनके यहाँ आत्मा और शरीर में एकांततः अभेद माना गया है उनके यहाँ शरीर के नाश होने पर आत्मा का भी नाश हो जावेगा इस आपत्ति का निवारण कैसे हो सकेगा। अर्थात् आत्मा और शरीर में सर्वथा भेद मानने से किसी के शरीर का घात करने से आत्मा को कुछ भी आघात नहीं पहुँचेगा तो हिंसा नाम की कोई चीज ही दुनिया में न रहेगी तब हिंसा के त्याग का उपदेश भी कोई क्यों देगा ? तथा आत्मा और शीरर का सर्वथा अभेद माना जावे तो शरीर के घात से आत्मा का भी घात हो जावेगा। इस तरह जीव का नाश मानने से दयापालनादि धर्माचरण भी व्यर्थ हो जावेगा। जब आत्मा नहीं तो परलोक भी न रहेगा ।
सत्य तो यह है कि जैसे अग्नि से तप्त लोहे पर चोट देने से लोहे के साथ मिली हुई अग्नि पर भी आघात पहुँचता है, उसी तरह किसी के शरीर पर आघात पहुँचाने से उसके साथ मिले हुये आत्मा को भी बड़ी पीड़ा होती है इस पीड़ा ही का नाम हिंसा है। क्योंकि जीव के शरीर, इन्द्रिय, श्वास आदि द्रव्य प्राण हैं इन्हीं से आत्मा प्रत्येक पर्याय में जीता है। इन द्रव्य प्राणों का वियोग ही लौकिक में मरण कहलाता है। 'नहि मृत्युसमं दुःखं' मृत्यु का दुःख जीवों के सबसे बड़ा दुःख है । मरणांत दुःख देने वाले जीव घोर पातकी, महानिर्दयी, क्रूरपरिणामी होते हैं। जहाँ क्रूरता है वहीं हिंसा है- अधर्म है। दया के बिना धर्म नहीं हो सकता है। कहा भी है कि
यस्य जीवदया नास्ति तस्य सच्चरितं कुतः । भूत कापि क्रिया श्रेयस्करी भवेत् ॥ अर्थ- जिसके जीवदया नहीं है उसके समीचीन चारित्र कैसे हो सकता है ? क्योंकि प्राणियों के साथ द्रोह करने वालों का कोई भी काम कल्याण का करने वाला है ।
दयालोरव्रतस्यापि स्वर्गतिः स्याददुर्गतिः । व्रतिनोऽपि दयोनस्य दुर्गतिः स्याददुगतिः ॥ अर्थ - दयालु पुरुष यदि व्रताचरण नहीं भी करता है तो
Jain Education International
स्व. पं. मिलापचन्द्र कटारिया
भी उसके लिये स्वर्गगति मुश्किल नहीं है। और जो व्रतों का पालन करता है किन्तु हृदय में दया नहीं है तो उसके लिये नरकादि दुर्गति भी सुलभ है।
तपस्यतु चिरंतोव्रं व्रतयत्वतियच्छतु । निर्दयस्तत्फलैर्हीनः षीनश्चैकां दयां चरन ॥
अर्थ- चाहे कोई चिरकाल तक घोर तपस्या करें, व्रत पाले और दान देवे, यदि दया नहीं हो तो उनका कोई फल मिलने वाला नहीं है । और एक दया है तो उनका बहुत फल है।
मनोदयानुविद्धं चेन मुधा क्लिश्नासि सिद्धये । मनोदयानुविद्धं चेन मुधा क्लिश्नासि सिद्धये ॥
अर्थ- अगर दया से भीगा हुआ मन है तो सिद्धि के लिये क्लेश उठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दयालु को सिद्धि प्राप्त कर लेना सुगम है। और जो दया से भीगा हुआ मन नहीं है तो उसको भी सिद्धि के लिये क्लेश उठाने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि निर्दयी को कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। प्रसिद्ध संत कवि तुलसीदासजी ने भी कहा है कि 'परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परपीड़ा सम नहीं अधमाई ।' वेद व्यास ने भी सारे पुराणों का सार २ शब्दों में इस प्रकार बताया है- अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयं । परोपकारः पुण्णाय पापाय परपीडनम् ॥ (अर्थात् १८ पुराणों का सार यह है कि परोपकार ही पुण्य है और परपीडन = हिंसा ही पाप है ।
सर्वेषां समयानां हृदय गर्भश्च सर्वशास्त्राणाम् । व्रत्तगुणशीलादीनां पिंडः सारोपि चाहिंसा ॥
1
अर्थ- सब मतों का हृदय और सब शास्त्रों का गर्भ तथा गुण-शीलादिकों की पिंड ऐसी सारभूत एक अहिंसा ही है। यद्यपि जैन दर्शन में किसी को दुःख देना पाप बताया है। किन्तु इसमें भी इतना और विशेष समझ लेना चाहिए कि यदि कर्त्ता के कषायभाव हो तो पाप हो सकता है। अगर कषाय भाव नहीं है तो अपने या दूसरे को पीड़ा देने मात्र से पाप नहीं होता है। क्योंकि डाक्टर भी आपरेशन करके रोगी को पीड़ा तो पहुँचाता ही है। गुरु भी शिष्य की ताड़ना करता है। किन्तु ऐसा करते हुये भी इनको पाप नहीं लगता है। क्योंकि इनके भाव अहित करने के नहीं हैं अतः इनके कषायभाव नहीं है। जीवहिंसा ही नहीं अन्य पाप भी भावों पर ही निर्भर हैं। यथा
व्रत
मनसैव कृतं पापं न शरीरकृतं कृतम् । येनैवालिंगिता कांता तेनैवालिंगिता सुता ॥
अर्थ- मानसिक परिणामों से किया हुआ ही पाप माना जाता है। बिना मन के केवल शरीर के द्वारा किया हुआ पाप नहीं
मई 2004 जिनभाषित 15
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org