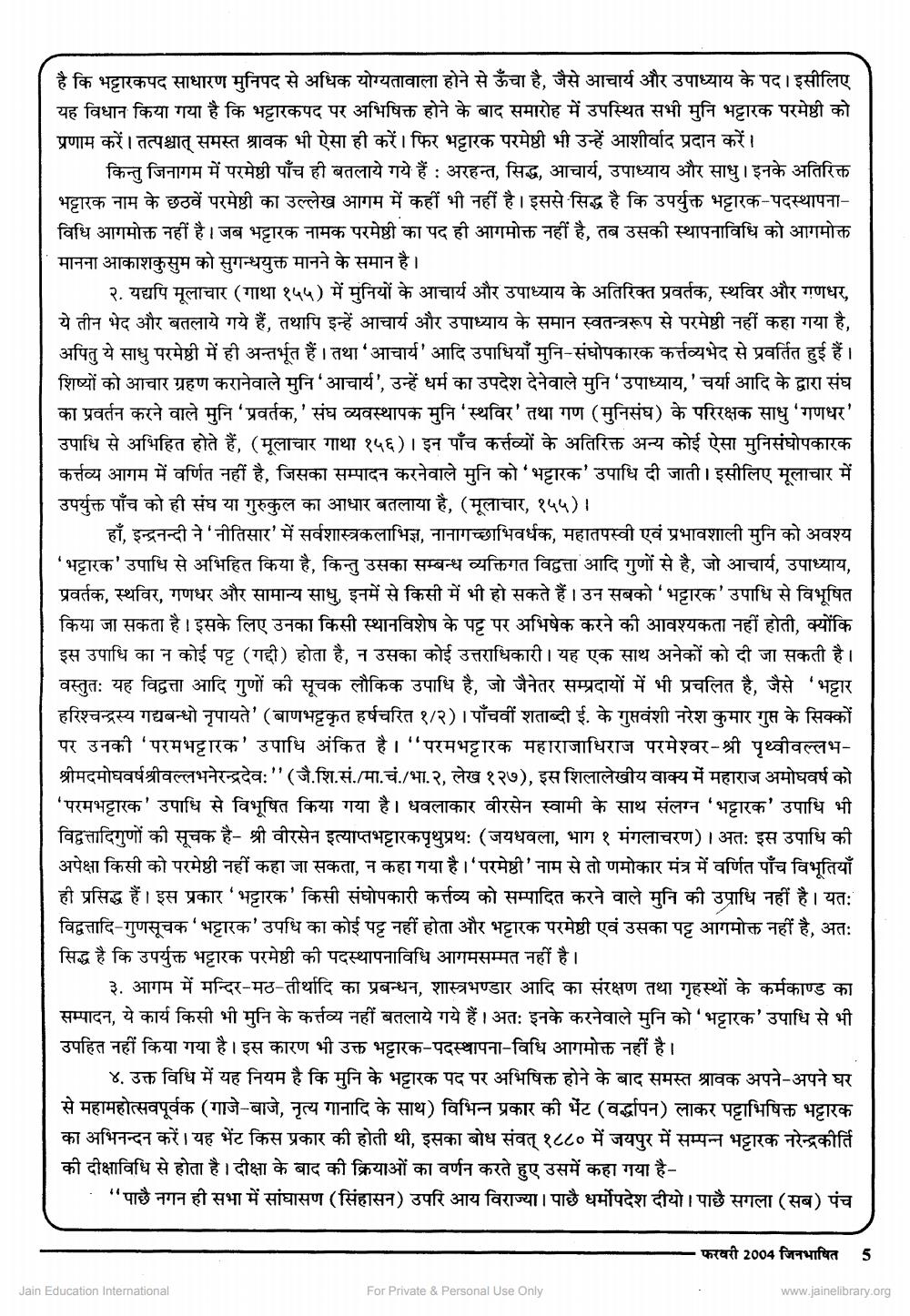________________
है कि भट्टारकपद साधारण मुनिपद से अधिक योग्यतावाला होने से ऊँचा है, जैसे आचार्य और उपाध्याय के पद । इसीलिए यह विधान किया गया है कि भट्टारकपद पर अभिषिक्त होने के बाद समारोह में उपस्थित सभी मुनि भट्टारक परमेष्ठी को प्रणाम करें। तत्पश्चात् समस्त श्रावक भी ऐसा ही करें। फिर भट्टारक परमेष्ठी भी उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें।
किन्तु जिनागम में परमेष्ठी पाँच ही बतलाये गये हैं : अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इनके अतिरिक्त भट्टारक नाम के छठवें परमेष्ठी का उल्लेख आगम में कहीं भी नहीं है। इससे सिद्ध है कि उपर्युक्त भट्टारक-पदस्थापनाविधि आगमोक्त नहीं है। जब भट्टारक नामक परमेष्ठी का पद ही आगमोक्त नहीं है, तब उसकी स्थापनाविधि को आगमोक्त मानना आकाशकुसुम को सुगन्धयुक्त मानने के समान है।
२. यद्यपि मूलाचार (गाथा १५५) में मुनियों के आचार्य और उपाध्याय के अतिरिक्त प्रवर्तक, स्थविर और गणधर, ये तीन भेद और बतलाये गये हैं, तथापि इन्हें आचार्य और उपाध्याय के समान स्वतन्त्ररूप से परमेष्ठी नहीं कहा गया है, अपितु ये साधु परमेष्ठी में ही अन्तर्भूत हैं। तथा 'आचार्य' आदि उपाधियाँ मनि-संघोपकारक कर्त्तव्यभेद से प्रवर्तित हई हैं। शिष्यों को आचार ग्रहण करानेवाले मुनि 'आचार्य', उन्हें धर्म का उपदेश देनेवाले मुनि 'उपाध्याय,' चर्या आदि के द्वारा संघ का प्रवर्तन करने वाले मुनि 'प्रवर्तक,' संघ व्यवस्थापक मुनि 'स्थविर' तथा गण (मुनिसंघ) के परिरक्षक साधु 'गणधर' उपाधि से अभिहित होते हैं, (मूलाचार गाथा १५६) । इन पाँच कर्तव्यों के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा मुनिसंघोपकारक कर्त्तव्य आगम में वर्णित नहीं है, जिसका सम्पादन करनेवाले मनि को 'भद्रारक' उपाधि दी जाती। इसीलिए मलाचार में उपर्युक्त पाँच को ही संघ या गुरुकुल का आधार बतलाया है, (मूलाचार, १५५)।
हाँ, इन्द्रनन्दी ने 'नीतिसार' में सर्वशास्त्रकलाभिज्ञ, नानागच्छाभिवर्धक, महातपस्वी एवं प्रभावशाली मुनि को अवश्य 'भट्टारक' उपाधि से अभिहित किया है, किन्तु उसका सम्बन्ध व्यक्तिगत विद्वत्ता आदि गुणों से है, जो आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, गणधर और सामान्य साधु, इनमें से किसी में भी हो सकते हैं। उन सबको 'भट्टारक' उपाधि से विभूषित किया जा सकता है। इसके लिए उनका किसी स्थानविशेष के पट्ट पर अभिषेक करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इस उपाधि का न कोई पट्ट (गद्दी) होता है, न उसका कोई उत्तराधिकारी। यह एक साथ अनेकों को दी जा सकती है। वस्तुतः यह विद्वत्ता आदि गुणों की सूचक लौकिक उपाधि है, जो जैनेतर सम्प्रदायों में भी प्रचलित है, जैसे 'भट्टार हरिश्चन्द्रस्य गद्यबन्धो नृपायते' (बाणभट्टकृत हर्षचरित १/२)। पाँचवीं शताब्दी ई. के गुप्तवंशी नरेश कुमार गुप्त के सिक्कों पर उनकी 'परमभट्टारक' उपाधि अंकित है। "परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर-श्री पृथ्वीवल्लभश्रीमदमोघवर्षश्रीवल्लभनेरन्द्रदेवः" (जै.शि.सं./मा.चं./भा.२, लेख १२७), इस शिलालेखीय वाक्य में महाराज अमोघवर्ष को 'परमभट्टारक' उपाधि से विभूषित किया गया है। धवलाकार वीरसेन स्वामी के साथ संलग्न 'भट्टारक' उपाधि भी विद्वत्तादिगुणों की सूचक है- श्री वीरसेन इत्याप्तभट्टारकपृथुप्रथः (जयधवला, भाग १ मंगलाचरण) । अतः इस उपाधि की अपेक्षा किसी को परमेष्ठी नहीं कहा जा सकता, न कहा गया है। 'परमेष्ठी' नाम से तो णमोकार मंत्र में वर्णित पाँच विभतियाँ ही प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार 'भट्टारक' किसी संघोपकारी कर्त्तव्य को सम्पादित करने वाले मुनि की उपाधि नहीं है। यतः विद्वत्तादि-गुणसूचक 'भट्टारक' उपधि का कोई पट्ट नहीं होता और भट्टारक परमेष्ठी एवं उसका पट्ट आगमोक्त नहीं है, अत: सिद्ध है कि उपर्युक्त भट्टारक परमेष्ठी की पदस्थापनाविधि आगमसम्मत नहीं है।
३. आगम में मन्दिर-मठ-तीर्थादि का प्रबन्धन, शास्त्रभण्डार आदि का संरक्षण तथा गृहस्थों के कर्मकाण्ड का सम्पादन, ये कार्य किसी भी मुनि के कर्त्तव्य नहीं बतलाये गये हैं। अतः इनके करनेवाले मुनि को 'भट्टारक' उपाधि से भी उपहित नहीं किया गया है। इस कारण भी उक्त भट्टारक-पदस्थापना-विधि आगमोक्त नहीं है।
४. उक्त विधि में यह नियम है कि मुनि के भट्टारक पद पर अभिषिक्त होने के बाद समस्त श्रावक अपने-अपने घर से महामहोत्सवपूर्वक (गाजे-बाजे, नृत्य गानादि के साथ) विभिन्न प्रकार की भेंट (वर्धापन) लाकर पट्टाभिषिक्त भट्टारक का अभिनन्दन करें। यह भेंट किस प्रकार की होती थी, इसका बोध संवत् १८८० में जयपुर में सम्पन्न भट्टारक नरेन्द्रकीर्ति की दीक्षाविधि से होता है। दीक्षा के बाद की क्रियाओं का वर्णन करते हुए उसमें कहा गया है
- "पाछै नगन ही सभा में सांघासण (सिंहासन) उपरि आय विराज्या। पाछै धर्मोपदेश दीयो। पाछै सगला (सब) पंच
- फरवरी 2004 जिनभाषित
5
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org