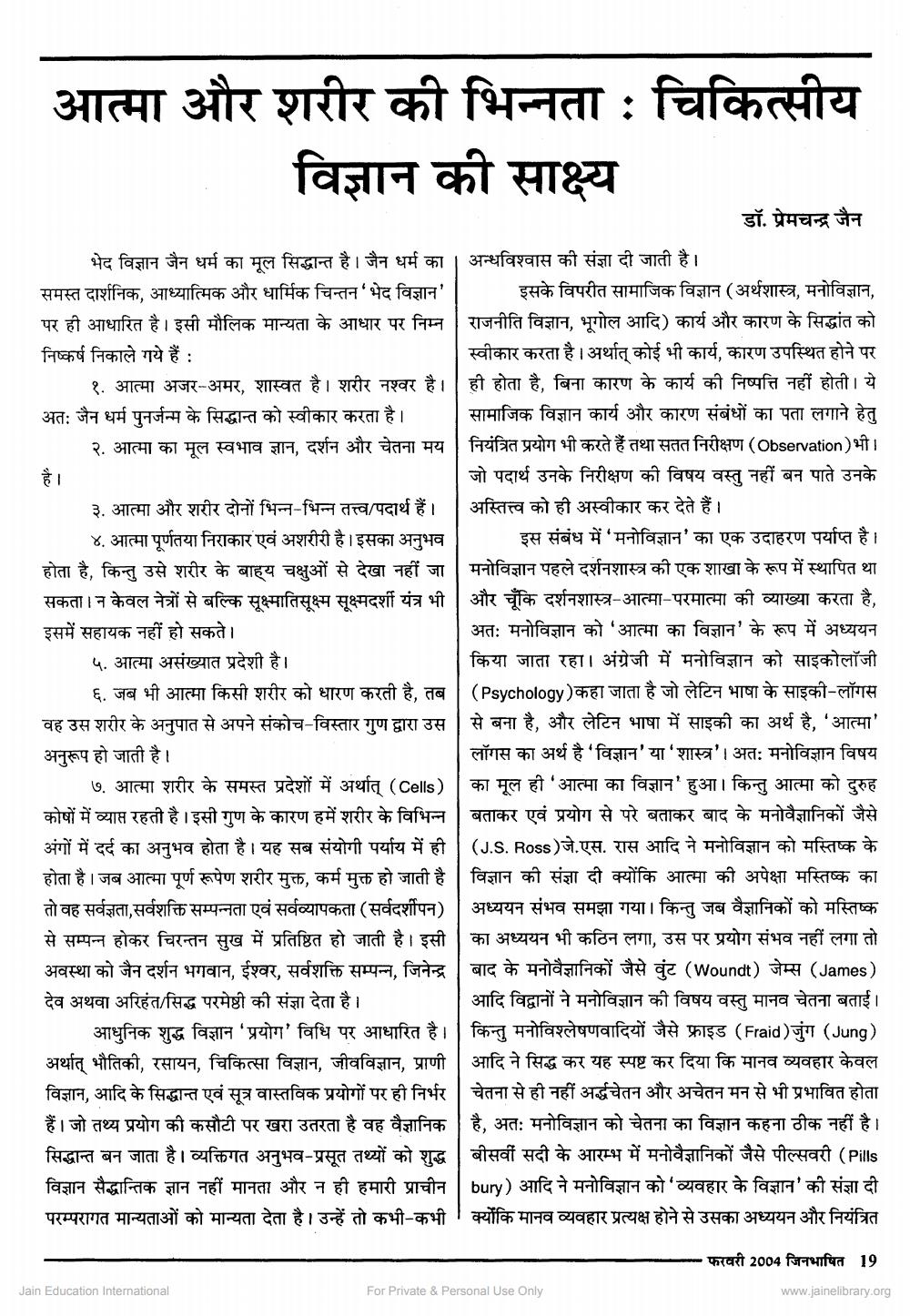________________
आत्मा और शरीर की भिन्नता : चिकित्सीय विज्ञान की साक्ष्य
भेद विज्ञान जैन धर्म का मूल सिद्धान्त है। जैन धर्म का समस्त दार्शनिक, आध्यात्मिक और धार्मिक चिन्तन ' भेद विज्ञान' पर ही आधारित है। इसी मौलिक मान्यता के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकाले गये हैं :
१. आत्मा अजर-अमर शास्वत है। शरीर नश्वर है। अत: जैन धर्म पुनर्जन्म के सिद्धान्त को स्वीकार करता है। २. आत्मा का मूल स्वभाव ज्ञान, दर्शन और चेतना मय
है ।
३. आत्मा और शरीर दोनों भिन्न-भिन्न तत्त्व/पदार्थ हैं। ४. आत्मा पूर्णतया निराकार एवं अशरीरी है। इसका अनुभव होता है, किन्तु उसे शरीर के बाह्य चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता। न केवल नेत्रों से बल्कि सूक्ष्मातिसूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी यंत्र भी इसमें सहायक नहीं हो सकते।
५. आत्मा असंख्यात प्रदेशी है।
६. जब भी आत्मा किसी शरीर को धारण करती है, तब वह उस शरीर के अनुपात से अपने संकोच विस्तार गुण द्वारा उस अनुरूप हो जाती है।
७. आत्मा शरीर के समस्त प्रदेशों में अर्थात् (Cells) कोषों में व्याप्त रहती है। इसी गुण के कारण हमें शरीर के विभिन्न अंगों में दर्द का अनुभव होता है। यह सब संयोगी पर्याय में ही होता है। जब आत्मा पूर्ण रूपेण शरीर मुक्त, कर्म मुक्त हो जाती है तो वह सर्वज्ञता, सर्वशक्ति सम्पन्नता एवं सर्वव्यापकता (सर्वदर्शीपन) से सम्पन्न होकर चिरन्तन सुख में प्रतिष्ठित हो जाती है। इसी अवस्था को जैन दर्शन भगवान, ईश्वर, सर्वशक्ति सम्पन्न, जिनेन्द्र देव अथवा अरिहंत/सिद्ध परमेष्ठी की संज्ञा देता है ।
आधुनिक शुद्ध विज्ञान 'प्रयोग' विधि पर आधारित है। अर्थात् भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान, जीवविज्ञान, प्राणी विज्ञान, आदि के सिद्धान्त एवं सूत्र वास्तविक प्रयोगों पर ही निर्भर हैं। जो तथ्य प्रयोग की कसौटी पर खरा उतरता है वह वैज्ञानिक सिद्धान्त बन जाता है। व्यक्तिगत अनुभव- प्रसूत तथ्यों को शुद्ध विज्ञान सैद्धान्तिक ज्ञान नहीं मानता और न ही हमारी प्राचीन परम्परागत मान्यताओं को मान्यता देता है। उन्हें तो कभी-कभी
Jain Education International
डॉ. प्रेमचन्द्र जैन
अन्धविश्वास की संज्ञा दी जाती है।
इसके विपरीत सामाजिक विज्ञान (अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, भूगोल आदि) कार्य और कारण के सिद्धांत को स्वीकार करता है। अर्थात् कोई भी कार्य, कारण उपस्थित होने पर ही होता है, बिना कारण के कार्य की निष्पत्ति नहीं होती। ये सामाजिक विज्ञान कार्य और कारण संबंधों का पता लगाने हेतु नियंत्रित प्रयोग भी करते हैं तथा सतत निरीक्षण (Observation) भी । जो पदार्थ उनके निरीक्षण की विषय वस्तु नहीं बन पाते उनके अस्तित्त्व को ही अस्वीकार कर देते हैं ।
इस संबंध में 'मनोविज्ञान' का एक उदाहरण पर्याप्त है। मनोविज्ञान पहले दर्शनशास्त्र की एक शाखा के रूप में स्थापित था और चूँकि दर्शनशास्त्र - आत्मा-परमात्मा की व्याख्या करता है, अतः मनोविज्ञान को 'आत्मा का विज्ञान' के रूप में अध्ययन किया जाता रहा। अंग्रेजी में मनोविज्ञान को साइकोलॉजी (Psychology) कहा जाता है जो लेटिन भाषा के साइकी-लॉगस से बना है, और लेटिन भाषा में साइकी का अर्थ है, 'आत्मा' लॉगस का अर्थ है 'विज्ञान' या 'शास्त्र' । अतः मनोविज्ञान विषय का मूल ही 'आत्मा का विज्ञान' हुआ । किन्तु आत्मा को दुरुह बताकर एवं प्रयोग से परे बताकर बाद के मनोवैज्ञानिकों जैसे (J.S. Ross) जे. एस. रास आदि ने मनोविज्ञान को मस्तिष्क के विज्ञान की संज्ञा दी क्योंकि आत्मा की अपेक्षा मस्तिष्क का अध्ययन संभव समझा गया। किन्तु जब वैज्ञानिकों को मस्तिष्क का अध्ययन भी कठिन लगा, उस पर प्रयोग संभव नहीं लगा तो बाद के मनोवैज्ञानिकों जैसे वुंट (Woundt) जेम्स (James ) आदि विद्वानों ने मनोविज्ञान की विषय वस्तु मानव चेतना बताई। किन्तु मनोविश्लेषणवादियों जैसे फ्राइड (Fraid ) जुंग (Jung) आदि ने सिद्ध कर यह स्पष्ट कर दिया कि मानव व्यवहार केवल चेतना से ही नहीं अर्द्धचेतन और अचेतन मन से भी प्रभावित होता है, अतः मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहना ठीक नहीं है। बीसवीं सदी के आरम्भ में मनोवैज्ञानिकों जैसे पील्सवरी (Pills bury) आदि ने मनोविज्ञान को 'व्यवहार के विज्ञान' की संज्ञा दी क्योंकि मानव व्यवहार प्रत्यक्ष होने से उसका अध्ययन और नियंत्रित
फरवरी 2004 जिनभाषित 19
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org