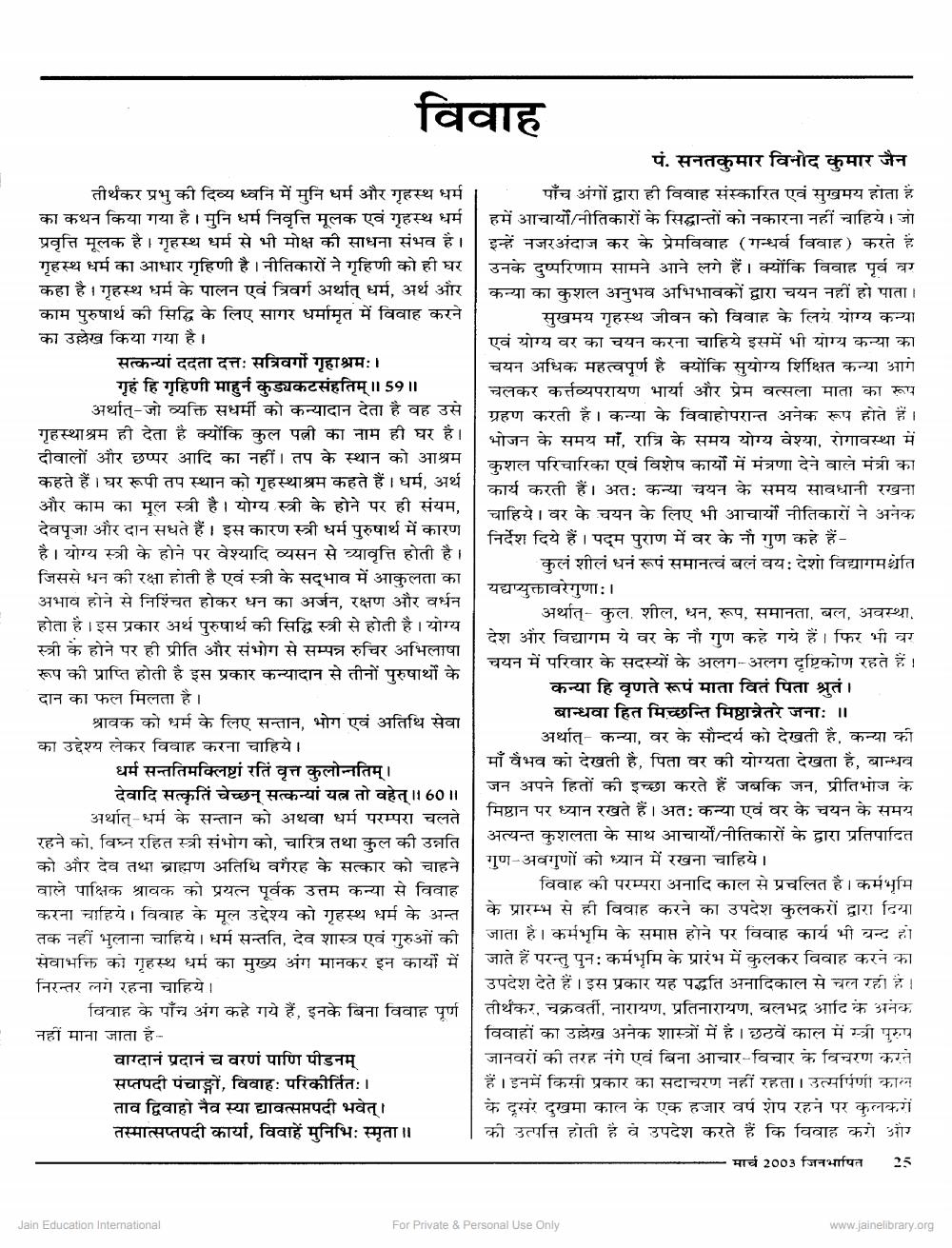________________
तीर्थंकर प्रभु की दिव्य ध्वनि में मुनि धर्म और गृहस्थ धर्म का कथन किया गया है। मुनि धर्म निवृत्ति मूलक एवं गृहस्थ धर्म प्रवृत्ति मूलक है। गृहस्थ धर्म से भी मोक्ष की साधना संभव है। गृहस्थ धर्म का आधार गृहिणी है नीतिकारों ने गृहिणी को ही घर कहा है। गृहस्थ धर्म के पालन एवं त्रिवर्ग अर्थात् धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए सागर धर्मामृत में विवाह करने का उल्लेख किया गया है।
1
विवाह
सत्कन्यां ददता दत्तः सत्रिवर्गो गृहाश्रमः ।
गृहं हि गृहिणी माहुर्न कुड्यकटसंहतिम् ॥ 59 ॥ अर्थात् जो व्यक्ति सधर्मी को कन्यादान देता है वह उसे गृहस्थाश्रम ही देता है क्योंकि कुल पत्नी का नाम ही घर हैं। दीवालों और छप्पर आदि का नहीं। तप के स्थान को आश्रम कहते हैं। घर रूपी तप स्थान को गृहस्थाश्रम कहते हैं। धर्म, अर्थ और काम का मूल स्त्री है। योग्य स्त्री के होने पर ही संयम, देवपूजा और दान सधते हैं। इस कारण स्त्री धर्म पुरुषार्थ में कारण हैं। योग्य स्त्री के होने पर वेश्यादि व्यसन से व्यावृत्ति होती है। जिससे धन की रक्षा होती है एवं स्त्री के सद्भाव में आकुलता का अभाव होने से निश्चित होकर धन का अर्जन, रक्षण और वर्धन होता है। इस प्रकार अर्थ पुरुषार्थ की सिद्धि स्त्री से होती है। योग्य स्त्री के होने पर ही प्रीति और संभोग से सम्पन्न रुचिर अभिलाषा रूप की प्राप्ति होती है इस प्रकार कन्यादान से तीनों पुरुषार्थों के दान का फल मिलता है।
श्रावक को धर्म के लिए सन्तान, भोग एवं अतिथि सेवा का उद्देश्य लेकर विवाह करना चाहिये ।
धर्म सन्ततिमक्लिष्टां रतिं वृत्त कुलोन्नतिम् ।
वाग्दान प्रदानं च वरणं पाणि पीडनम् सप्तपदी पंचाङ्गों, विवाहः परिकीर्तितः । ताव दिवाहो नैव स्याद्यावत्सप्तपदी भवेत्। तस्मात्सप्तपदी कार्या, विवाहें मुनिभिः स्मृता ॥
अर्थात्- कन्या, वर के सौन्दर्य को देखती है, कन्या की माँ वैभव को देखती है, पिता वर की योग्यता देखता हैं, बान्धव जन अपने हितों की इच्छा करते हैं जबकि जन, प्रीतिभोज के मिष्ठान पर ध्यान रखते हैं। अतः कन्या एवं वर के चयन के समय अत्यन्त कुशलता के साथ आचार्यों/ नीतिकारों के द्वारा प्रतिपादित गुण-अवगुणों को ध्यान में रखना चाहिये ।
देवादि सत्कृतिं चेच्छन् सत्कन्यां यत्न तो वहेत् ॥ 60 ॥ अर्थात्-धर्म के सन्तान को अथवा धर्म परम्परा चलते रहने को विघ्न रहित स्त्री संभोग को, चारित्र तथा कुल की उन्नति को और देव तथा ब्राह्मण अतिथि वगैरह के सत्कार को चाहने वाले पाक्षिक श्रावक को प्रयत्न पूर्वक उत्तम कन्या से विवाह करना चाहिये । विवाह के मूल उद्देश्य को गृहस्थ धर्म के अन्त तक नहीं भुलाना चाहिये । धर्म सन्तति, देव शास्त्र एवं गुरुओं की सेवाभक्ति को गृहस्थ धर्म का मुख्य अंग मानकर इन कार्यों में निरन्तर लगे रहना चाहिये।
विवाह की परम्परा अनादि काल से प्रचलित है। कर्मभूमि के प्रारम्भ से ही विवाह करने का उपदेश कुलकरों द्वारा दिया जाता है। कर्मभूमि के समाप्त होने पर विवाह कार्य भी बन्द हो जाते हैं परन्तु पुनः कर्मभूमि के प्रारंभ में कुलकर विवाह करने का उपदेश देते हैं। इस प्रकार यह पद्धति अनादिकाल से चल रही है।
विवाह के पाँच अंग कहे गये हैं, इनके बिना विवाह पूर्ण तीर्थंकर चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र आदि के अनेक नहीं माना जाता है
विवाहों का उल्लेख अनेक शास्त्रों में है। छठवें काल में स्त्री पुरुष जानवरों की तरह नंगे एवं बिना आचार-विचार के विचरण करते हैं। इनमें किसी प्रकार का सदाचरण नहीं रहता। उत्सर्पिणी काल के दूसरे दुखमा काल के एक हजार वर्ष शेष रहने पर कुलकरों की उत्पत्ति होती है वे उपदेश करते हैं कि विवाह करो और मार्च 2003 जिनभाषित
Jain Education International
पं. सनतकुमार विनोद कुमार जैन
पाँच अंगों द्वारा ही विवाह संस्कारित एवं सुखमय होता है। हमें आचार्यो/ नीतिकारों के सिद्धान्तों को नकारना नहीं चाहिये। जां इन्हें नजरअंदाज कर के प्रेमविवाह (गन्धर्व विवाह) करते है उनके दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। क्योंकि विवाह पूर्व वर कन्या का कुशल अनुभव अभिभावकों द्वारा चयन नहीं हो पाता ।
सुखमय गृहस्थ जीवन को विवाह के लिये योग्य कन्या एवं योग्य वर का चयन करना चाहिये इसमें भी योग्य कन्या का चयन अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि सुयोग्य शिक्षित कन्या आगे चलकर कर्त्तव्यपरायण भार्या और प्रेम वत्सला माता का रूप ग्रहण करती हैं। कन्या के विवाहोपरान्त अनेक रूप होते हैं। भोजन के समय माँ, रात्रि के समय योग्य वेश्या, रोगावस्था में कुशल परिचारिका एवं विशेष कार्यों में मंत्रणा देने वाले मंत्री का कार्य करती हैं। अतः कन्या चयन के समय सावधानी रखना चाहिये । वर के चयन के लिए भी आचार्यो नीतिकारों ने अनेक निर्देश दिये हैं। पद्म पुराण में वर के नी गुण कहे हैं
कुलं शीलं धनं रूपं समानत्वं बलं वय: देशी विद्यागमश्चेति यद्यप्युक्तावरेगुणाः ।
अर्थात्- कुल शील, धन, रूप, समानता, बल, अवस्था, देश और विद्यागम ये वर के नौ गुण कहे गये हैं। फिर भी वर चयन में परिवार के सदस्यों के अलग-अलग दृष्टिकोण रहते हैं ।
कन्या हि वृणते रूपं माता वितं पिता श्रुतं । बान्धवा हित मिच्छन्ति मिष्ठात्रेतरे जनाः ॥
For Private & Personal Use Only
25
www.jainelibrary.org