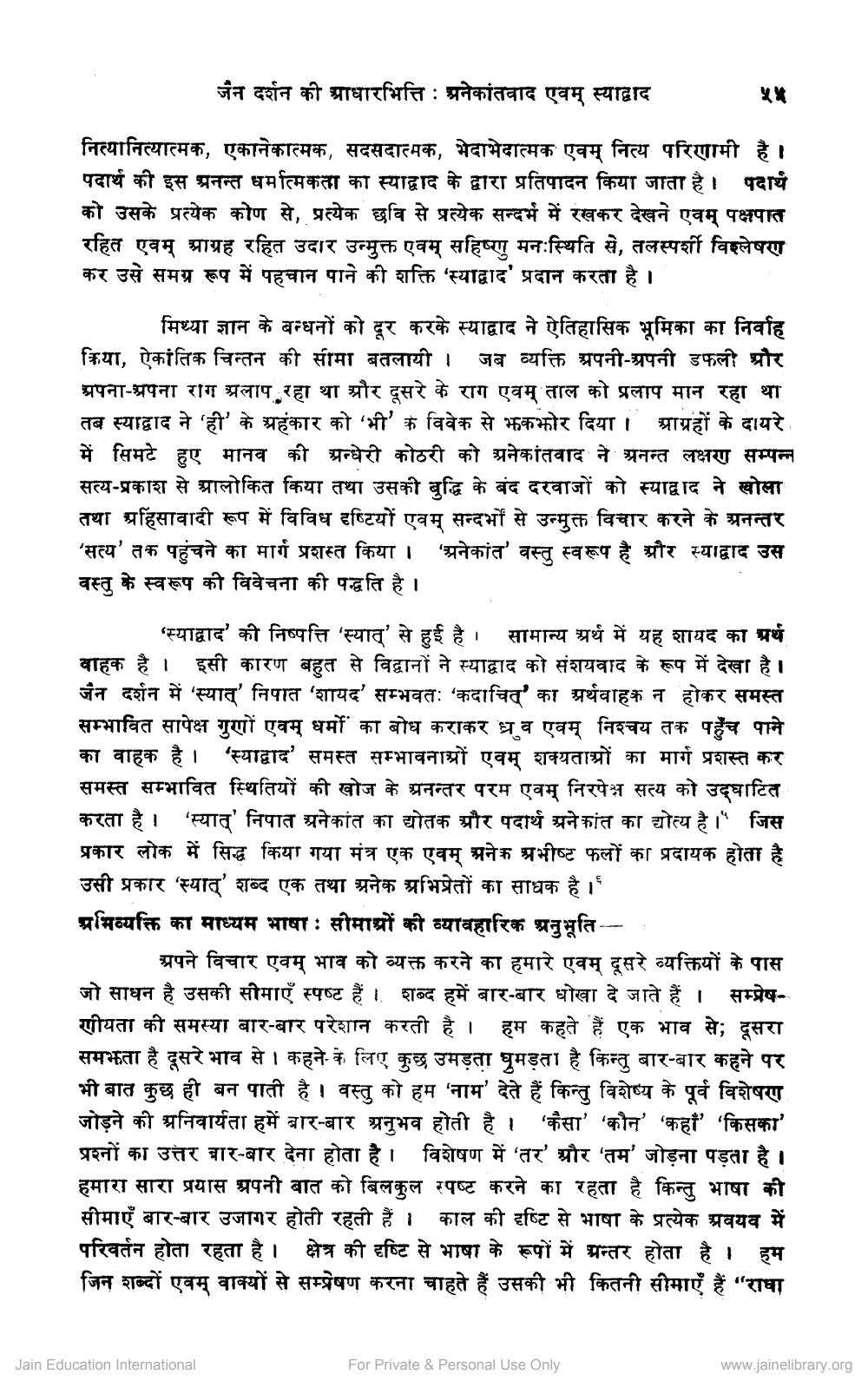________________
जैन दर्शन की आधारभित्ति : अनेकांतवाद एवम् स्याद्वाद
नित्यानित्यात्मक, एकानेकात्मक, सदसदात्मक, भेदाभेदात्मक एवम् नित्य परिणामी है। पदार्थ की इस अनन्त धर्मात्मकता का स्याद्वाद के द्वारा प्रतिपादन किया जाता है। पदार्थ को उसके प्रत्येक कोण से, प्रत्येक छवि से प्रत्येक सन्दर्भ में रखकर देखने एवम् पक्षपात रहित एवम् प्राग्रह रहित उदार उन्मुक्त एवम् सहिष्णु मनःस्थिति से, तलस्पर्शी विश्लेषण कर उसे समग्र रूप में पहचान पाने की शक्ति 'स्याद्वाद' प्रदान करता है।
मिथ्या ज्ञान के बन्धनों को दूर करके स्याद्वाद ने ऐतिहासिक भूमिका का निर्वाह किया, ऐकांतिक चिन्तन की सीमा बतलायी। जब व्यक्ति अपनी-अपनी डफली और अपना-अपना राग अलाप रहा था और दूसरे के राग एवम् ताल को प्रलाप मान रहा था तब स्याद्वाद ने 'ही' के अहंकार को 'भी' के विवेक से झकझोर दिया। प्राग्रहों के दायरे में सिमटे हुए मानव की अन्धेरी कोठरी को अनेकांतवाद ने अनन्त लक्षण सम्पन्न सत्य-प्रकाश से आलोकित किया तथा उसकी बुद्धि के बंद दरवाजों को स्यावाद ने खोला तथा अहिंसावादी रूप में विविध दृष्टियों एवम् सन्दर्भो से उन्मुक्त विचार करने के अनन्तर 'सत्य' तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। 'अनेकांत' वस्तु स्वरूप है और स्याद्वाद उस वस्तु के स्वरूप की विवेचना की पद्धति है ।
___ 'स्याद्वाद' की निष्पत्ति 'स्यात्' से हुई है। सामान्य अर्थ में यह शायद का अर्थ वाहक है। इसी कारण बहुत से विद्वानों ने स्याद्वाद को संशयवाद के रूप में देखा है। जैन दर्शन में 'स्यात्' निपात 'शायद' सम्भवतः 'कदाचित्' का अर्थवाहक न होकर समस्त सम्भावित सापेक्ष गुणों एवम् धर्मों का बोध कराकर ध्र व एवम् निश्चय तक पहुँच पाने का वाहक है। 'स्याद्वाद' समस्त सम्भावनाओं एवम् शक्यताओं का मार्ग प्रशस्त कर समस्त सम्भावित स्थितियों की खोज के अनन्तर परम एवम् निरपेक्ष सत्य को उद्घाटित करता है। 'स्यात्' निपात अनेकांत का द्योतक और पदार्थ अनेकांत का द्योत्य है। जिस प्रकार लोक में सिद्ध किया गया मंत्र एक एवम् अनेक अभीष्ट फलों का प्रदायक होता है उसी प्रकार ‘स्यात्' शब्द एक तथा अनेक अभिप्रेतों का साधक है।' अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा : सीमानों की व्यावहारिक अनुभूति ---
__ अपने विचार एवम् भाव को व्यक्त करने का हमारे एवम् दूसरे व्यक्तियों के पास जो साधन है उसकी सीमाएँ स्पष्ट हैं। शब्द हमें बार-बार धोखा दे जाते हैं । सम्प्रेषणीयता की समस्या बार-बार परेशान करती है। हम कहते हैं एक भाव से; दूसरा समझता है दूसरे भाव से । कहने के लिए कुछ उमड़ता घुमड़ता है किन्तु बार-बार कहने पर भी बात कुछ ही बन पाती है। वस्तु को हम 'नाम' देते हैं किन्तु विशेष्य के पूर्व विशेषण जोड़ने की अनिवार्यता हमें बार-बार अनुभव होती है। 'कैसा' 'कौन' 'कहाँ' 'किसका' प्रश्नों का उत्तर बार-बार देना होता है। विशेषण में 'तर' और 'तम' जोड़ना पड़ता है। हमारा सारा प्रयास अपनी बात को बिलकुल स्पष्ट करने का रहता है किन्तु भाषा की सीमाएँ बार-बार उजागर होती रहती हैं। काल की दृष्टि से भाषा के प्रत्येक अवयव में परिवर्तन होता रहता है। क्षेत्र की दृष्टि से भाषा के रूपों में अन्तर होता है। हम जिन शब्दों एवम् वाक्यों से सम्प्रेषण करना चाहते हैं उसकी भी कितनी सीमाएँ हैं "राधा
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org