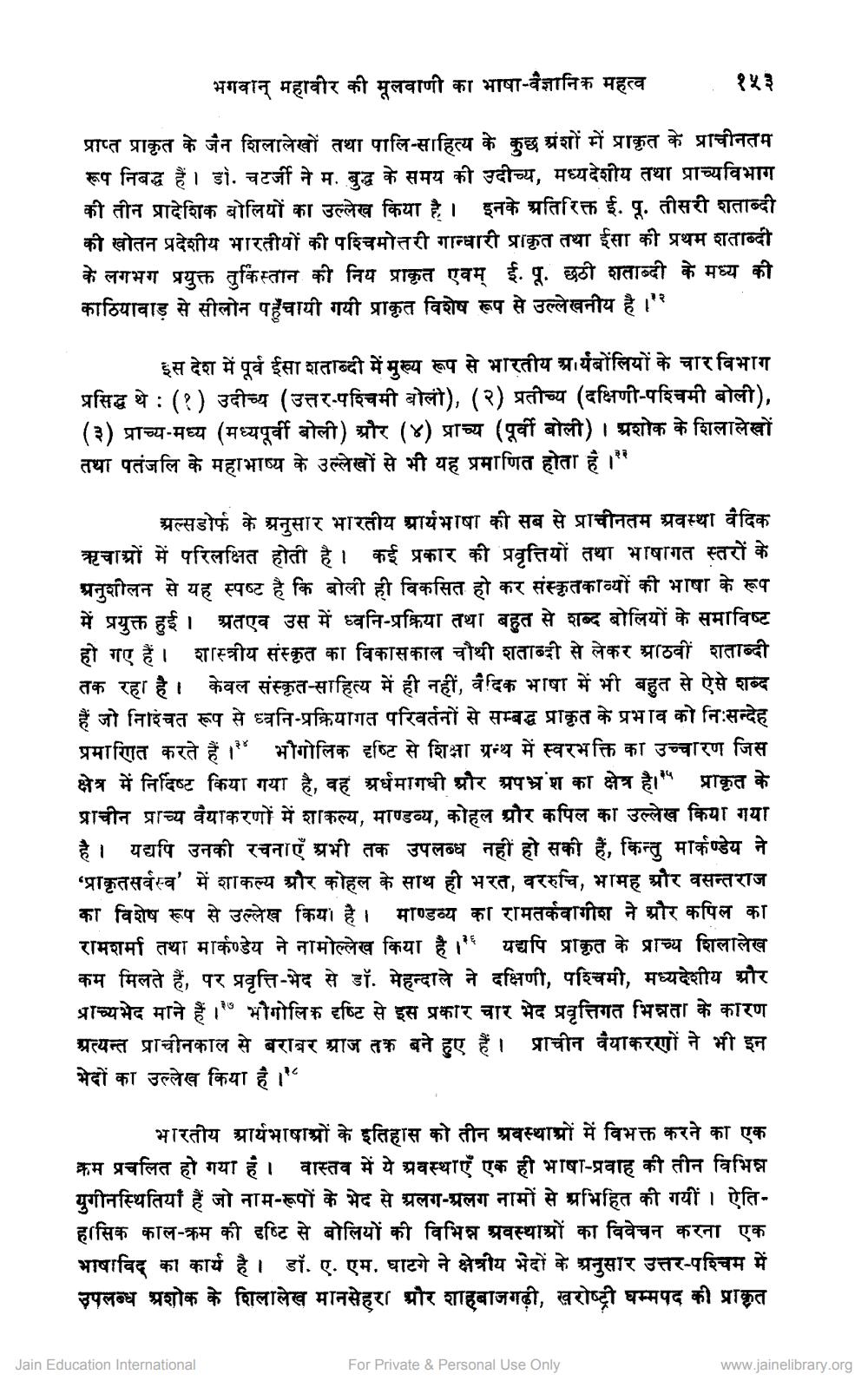________________
भगवान् महावीर की मूलवाणी का भाषा वैज्ञानिक महत्व
प्राप्त प्राकृत के जैन शिलालेखों तथा पालि-साहित्य के कुछ अंशों में प्राकृत के प्राचीनतम रूप निबद्ध हैं। डॉ. चटर्जी ने म. बुद्ध के समय की उदीच्य, मध्यदेशीय तथा प्राच्यविभाग की तीन प्रादेशिक बोलियों का उल्लेख किया है । इनके अतिरिक्त ई. पू. तीसरी शताब्दी की खोतन प्रदेशीय भारतीयों की पश्चिमोत्तरी गान्धारी प्राकृत तथा ईसा की प्रथम शताब्दी के लगभग प्रयुक्त तुर्किस्तान की निय प्राकृत एवम् ई. पू. छठी शताब्दी के मध्य की atforवाड़ से सीलोन पहुँचायी गयी प्राकृत विशेष रूप से उल्लेखनीय है । "
१५३
इस देश में पूर्व ईसा शताब्दी में मुख्य रूप से भारतीय बोलियों के चार विभाग प्रसिद्ध थे : (१) उदीच्य (उत्तर-पश्चिमी बोली), (२) प्रतीच्य (दक्षिणी-पश्चिमी बोली), (३) प्राच्य - मध्य ( मध्यपूर्वी बोली ) और (४) प्राच्य (पूर्वी बोली ) । अशोक के शिलालेखों तथा पतंजलि के महाभाष्य के उल्लेखों से भी यह प्रमाणित होता है।
अल्सडोर्फ के अनुसार भारतीय श्रार्यभाषा की सब से प्राचीनतम अवस्था वैदिक ऋचाओं में परिलक्षित होती है। कई प्रकार की प्रवृत्तियों तथा भाषागत स्तरों के अनुशीलन से यह स्पष्ट है कि बोली ही विकसित हो कर संस्कृतकाव्यों की भाषा के रूप में प्रयुक्त हुई । अतएव उस में ध्वनि-प्रक्रिया तथा बहुत से शब्द बोलियों के समाविष्ट हो गए हैं । शास्त्रीय संस्कृत का विकासकाल चौथी शताब्दी से लेकर आठवीं शताब्दी तक रहा है। केवल संस्कृत-साहित्य में ही नहीं, वैदिक भाषा में भी बहुत से ऐसे शब्द हैं जो निश्चित रूप से ध्वनि-प्रक्रियागत परिवर्तनों से सम्बद्ध प्राकृत के प्रभाव को निःसन्देह प्रमाणित करते हैं । * भौगोलिक दृष्टि से शिक्षा ग्रन्थ में स्वरभक्ति का उच्चारण जिस क्षेत्र में निर्दिष्ट किया गया है, वह अर्धमागधी और अपभ्रंश का क्षेत्र है। " प्राकृत के प्राचीन प्राच्य वैयाकरणों में शाकल्य, माण्डव्य, कोहल श्रौर कपिल का उल्लेख किया गया है । यद्यपि उनकी रचनाएँ अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी हैं, किन्तु मार्कण्डेय ने 'प्राकृतसर्वस्व' में शाकल्य और कोहल के साथ ही भरत, वररुचि, भामह और वसन्तराज का विशेष रूप से उल्लेख किया है । माण्डव्य का रामतर्कवागीश ने और कपिल का रामशर्मा तथा मार्कण्डेय ने नामोल्लेख किया है । ६ यद्यपि प्राकृत के प्राच्य शिलालेख कम मिलते हैं, पर प्रवृत्ति-भेद से डॉ. मेहन्दाले ने दक्षिणी, पश्चिमी, मध्यदेशीय और प्राच्यभेद माने हैं । " भौगोलिक दृष्टि से इस प्रकार चार भेद प्रवृत्तिगत भिन्नता के कारण अत्यन्त प्राचीनकाल से बराबर आज तक बने हुए हैं। प्राचीन वैयाकरणों ने भी इन भेदों का उल्लेख किया है ।"
भारतीय आर्यभाषाओं के इतिहास को तीन श्रवस्थानों में विभक्त करने का एक क्रम प्रचलित हो गया है । वास्तव में ये अवस्थाएँ एक ही भाषा प्रवाह की तीन विभिन्न युगीनस्थितियाँ हैं जो नाम-रूपों के भेद से अलग-अलग नामों से अभिहित की गयीं । ऐतिहासिक काल-क्रम की दृष्टि से बोलियों की विभिन्न अवस्थाओं का विवेचन करना एक भाषाविद का कार्य है । डॉ. ए. एम. घाटगे ने क्षेत्रीय भेदों के अनुसार उत्तर-पश्चिम में उपलब्ध अशोक के शिलालेख मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, खरोष्ट्री घम्मपद की प्राकृत
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org