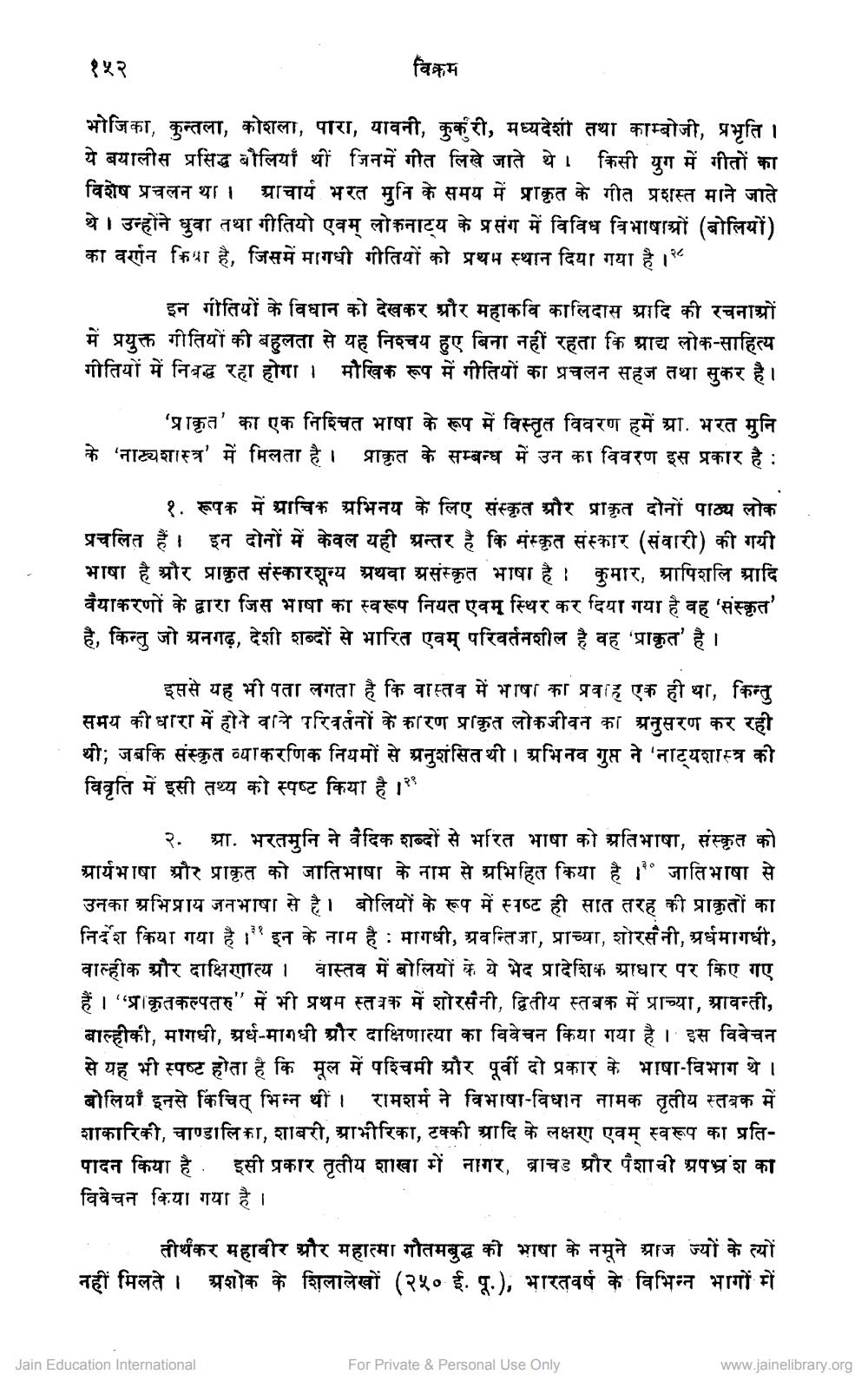________________
१५२
विक्रम
भोजिका, कुन्तला, कोशला, पारा, यावनी, कुर्कुरी, मध्यदेशी तथा काम्बोजी, प्रभृति । ये बयालीस प्रसिद्ध बौलियाँ थीं जिनमें गीत लिखे जाते थे । किसी युग में गीतों का विशेष प्रचलन था । प्राचार्य भरत मुनि के समय में प्राकृत के गीत प्रशस्त माने जाते थे। उन्होंने धुवा तथा गीतियो एवम् लोकनाट्य के प्रसंग में विविध विभाषाओं (बोलियों) का वर्णन किया है, जिसमें मागधी गीतियों को प्रथम स्थान दिया गया है । २८
इन गीतियों के विधान को देखकर और महाकवि कालिदास आदि की रचनाओं में प्रयुक्त गीतियों की बहुलता से यह निश्चय हुए बिना नहीं रहता कि श्राद्य लोक-साहित्य गीतियों में निबद्ध रहा होगा । मौखिक रूप में गीतियों का प्रचलन सहज तथा सुकर है ।
'प्राकृत' का एक निश्चित भाषा के रूप में विस्तृत विवरण हमें प्रा. भरत मुनि के 'नाट्यशास्त्र' में मिलता है । प्राकृत के सम्बन्ध में उन का विवरण इस प्रकार है :
१. रूपक में श्राचिक अभिनय के लिए संस्कृत और प्राकृत दोनों पाठ्य लोक प्रचलित हैं । इन दोनों में केवल यही अन्तर है कि संस्कृत संस्कार ( संवारी) की गयी भाषा है और प्राकृत संस्कारशून्य अथवा असंस्कृत भाषा है। कुमार, आपिशलि प्रादि वैयाकरणों के द्वारा जिस भाषा का स्वरूप नियत एवम् स्थिर कर दिया गया है वह 'संस्कृत' है, किन्तु जो अनगढ़, देशी शब्दों से भारित एवम् परिवर्तनशील है वह 'प्राकृत' है ।
इससे यह भी पता लगता है कि वास्तव में भाषा का प्रवाह एक ही था, किन्तु समय की धारा में होने वाले परिवर्तनों के कारण प्राकृत लोकजीवन का अनुसरण कर रही थी; जबकि संस्कृत व्याकरणिक नियमों से अनुशंसित थी । अभिनव गुप्त ने 'नाट्यशास्त्र की विवृति में इसी तथ्य को स्पष्ट किया है । २९
२. प्रा. भरतमुनि ने वैदिक शब्दों से भरित भाषा को प्रतिभाषा, संस्कृत को आर्यभाषा और प्राकृत को जातिभाषा के नाम से अभिहित किया है ।" जातिभाषा से उनका अभिप्राय जनभाषा से है । बोलियों के रूप में स्पष्ट ही सात तरह की प्राकृतों का निर्देश किया गया है । इनके नाम है : मागधी, अवन्तिजा, प्राच्या, शोरसैनी, अर्धमागधी, वाल्हीक और दाक्षिणात्य | वास्तव में बोलियों के ये भेद प्रादेशिक आधार पर किए गए हैं । "प्राकृतकल्पतरु' में भी प्रथम स्तवक में शोरसैनी, द्वितीय स्तबक प्राच्या, आवन्ती,
की, मागधी, अर्ध-मागधी और दाक्षिणात्या का विवेचन किया गया है। इस विवेचन से यह भी स्पष्ट होता है कि मूल में पश्चिमी और पूर्वी दो प्रकार के भाषा विभाग थे । बोलियाँ इनसे किंचित् भिन्न थीं । रामशर्म ने विभाषा - विधान नामक तृतीय स्तबक में शाकारिकी, चाण्डालिका, शाबरी, आभीरिका, टक्की आदि के लक्षण एवम् स्वरूप का प्रतिपादन किया है. इसी प्रकार तृतीय शाखा में नागर, ब्राचड प्रौर पैशाची अपभ्रंश का विवेचन किया गया है ।
तीर्थंकर महावीर और महात्मा गौतमबुद्ध की भाषा के नमूने आज ज्यों के त्यों नहीं मिलते। अशोक के शिलालेखों ( २५० ई. पू.), भारतवर्ष के विभिन्न भागों में
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org