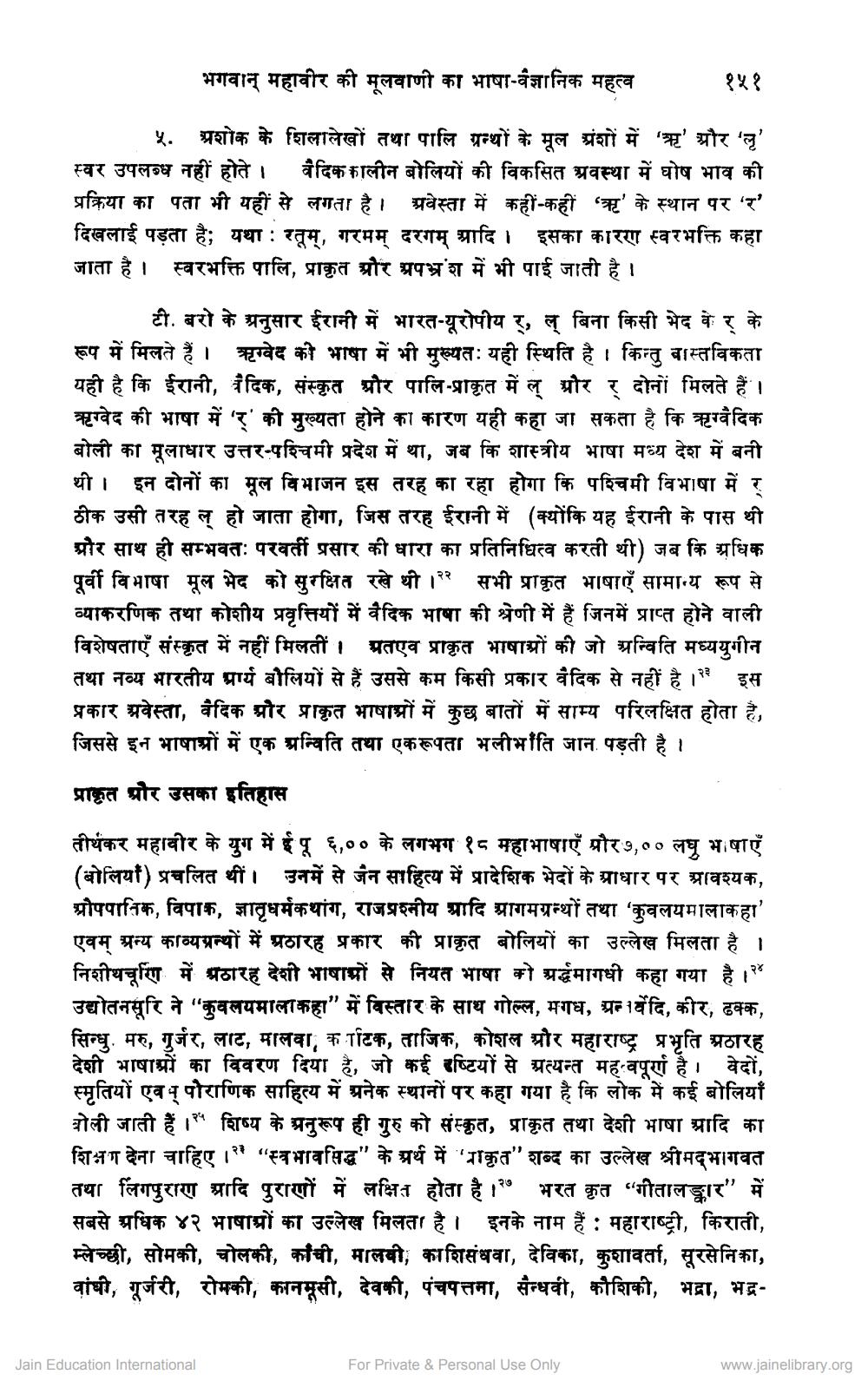________________
भगवान् महावीर की मूलवाणी का भाषा-वैज्ञानिक महत्व
१५१
५. अशोक के शिलालेखों तथा पालि ग्रन्थों के मूल अंशों में 'ऋ' और 'लु' स्वर उपलब्ध नहीं होते। वैदिक कालीन बोलियों की विकसित अवस्था में घोष भाव की प्रक्रिया का पता भी यहीं से लगता है। अवेस्ता में कहीं-कहीं 'ऋ' के स्थान पर 'र' दिखलाई पड़ता है; यथा : रतूम्, गरमम् दरगम् आदि। इसका कारण स्वरभक्ति कहा जाता है। स्वरभक्ति पालि, प्राकृत और अपभ्रश में भी पाई जाती है।
टी. बरो के अनुसार ईरानी में भारत-यूरोपीय र, ल बिना किसी भेद के र के रूप में मिलते हैं। ऋग्वेद की भाषा में भी मुख्यतः यही स्थिति है । किन्तु वास्तविकता यही है कि ईरानी, वैदिक, संस्कृत और पालि-प्राकृत में ल और र् दोनों मिलते हैं। ऋग्वेद की भाषा में 'र' की मुख्यता होने का कारण यही कहा जा सकता है कि ऋग्वैदिक बोली का मूलाधार उत्तर-पश्चिमी प्रदेश में था, जब कि शास्त्रीय भाषा मध्य देश में बनी थी। इन दोनों का मूल विभाजन इस तरह का रहा होगा कि पश्चिमी विभाषा में र ठीक उसी तरह ल हो जाता होगा, जिस तरह ईरानी में (क्योंकि यह ईरानी के पास थी
और साथ ही सम्भवतः परवर्ती प्रसार की धारा का प्रतिनिधित्व करती थी) जब कि अधिक पूर्वी विभाषा मूल भेद को सुरक्षित रखे थी ।२२ सभी प्राकृत भाषाएँ सामान्य रूप से व्याकरणिक तथा कोशीय प्रवृत्तियों में वैदिक भाषा की श्रेणी में हैं जिनमें प्राप्त होने वाली विशेषताएँ संस्कृत में नहीं मिलतीं। प्रतएव प्राकृत भाषामों की जो अन्विति मध्ययुगीन तथा नव्य भारतीय प्रार्य बौलियों से हैं उससे कम किसी प्रकार वैदिक से नहीं है ।२३ इस प्रकार अवेस्ता, वैदिक और प्राकृत भाषाओं में कुछ बातों में साम्य परिलक्षित होता है, जिससे इन भाषाओं में एक अन्विति तथा एकरूपता भलीभांति जान पड़ती है । प्राकृत और उसका इतिहास तीर्थंकर महावीर के युग में ई पू ६,०० के लगभग १८ महाभाषाएँ प्रौर ७,०० लघु भाषाएँ (बोलियाँ) प्रचलित थीं। उनमें से जैन साहित्य में प्रादेशिक भेदों के आधार पर आवश्यक, प्रौपपातिक, विपाक, ज्ञातृधर्मकथांग, राजप्रश्नीय आदि आगमग्रन्थों तथा 'कुवलयमालाकहा' एवम् अन्य काव्यग्रन्थों में अठारह प्रकार की प्राकृत बोलियों का उल्लेख मिलता है । निशीथचूरिण में अठारह देशी भाषामों से नियत भाषा को अर्धमागधी कहा गया है ।२४ उद्योतनसूरि ने "कुवलयमालाकहा" में विस्तार के साथ गोल्ल, मगध, अन्वेदि, कीर, ढक्क, सिन्धु. मरु, गुर्जर, लाट, मालवा, कीटक, ताजिक, कोशल और महाराष्ट्र प्रभृति अठारह देशी भाषाओं का विवरण दिया है, जो कई रष्टियों से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वेदों, स्मृतियों एवम् पौराणिक साहित्य में अनेक स्थानों पर कहा गया है कि लोक में कई बोलियाँ बोली जाती हैं । २५ शिष्य के अनुरूप ही गुरु को संस्कृत, प्राकृत तथा देशी भाषा आदि का शिक्षा देना चाहिए । २२ "स्वभावसिद्ध" के अर्थ में 'प्राकृत" शब्द का उल्लेख श्रीमद्भागवत तथा लिंगपुराण आदि पुराणों में लक्षित होता है । २७ भरत कृत "गीतालङ्कार" में सबसे अधिक ४२ भाषाओं का उल्लेख मिलता है। इनके नाम हैं : महाराष्ट्री, किराती, म्लेच्छी, सोमकी, चोलकी, कांची, मालवी, काशिसंधवा, देविका, कुशावर्ता, सूरसेनिका, वांधी, गूर्जरी, रोमकी, कानमूसी, देवकी, पंचपत्तना, सैन्धवी, कौशिकी, भद्रा, भद्र
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org