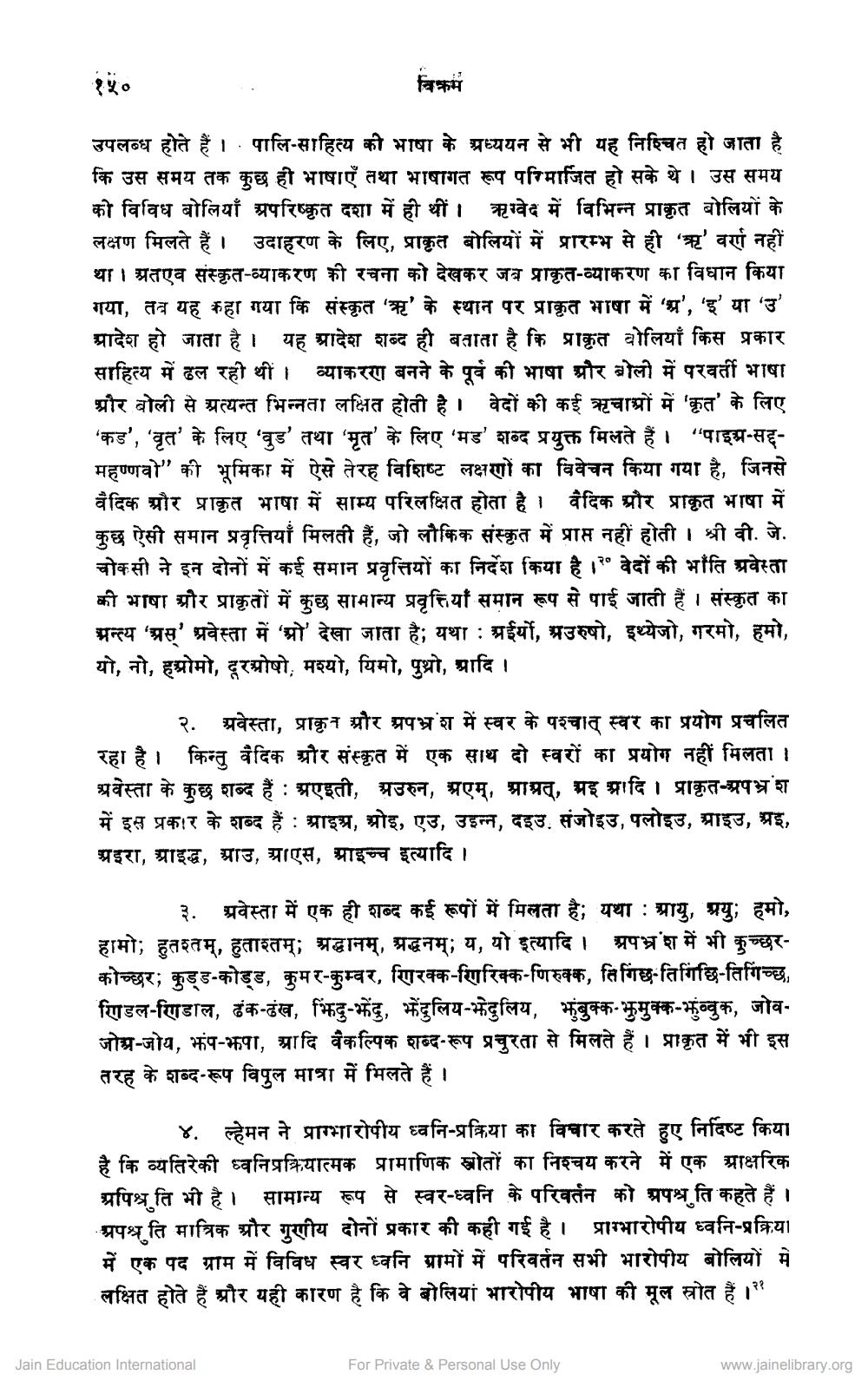________________
१५०
विक्रम
उपलब्ध होते हैं । . पालि-साहित्य की भाषा के अध्ययन से भी यह निश्चित हो जाता है कि उस समय तक कुछ ही भाषाएँ तथा भाषागत रूप परिमार्जित हो सके थे। उस समय को विविध बोलियाँ अपरिष्कृत दशा में ही थीं। ऋग्वेद में विभिन्न प्राकृत बोलियों के लक्षण मिलते हैं। उदाहरण के लिए, प्राकृत बोलियों में प्रारम्भ से ही 'ऋ' वर्ण नहीं था। अतएव संस्कृत-व्याकरण की रचना को देखकर जब प्राकृत-व्याकरण का विधान किया गया, तब यह कहा गया कि संस्कृत 'ऋ' के स्थान पर प्राकृत भाषा में 'अ', 'इ' या 'उ' आदेश हो जाता है। यह आदेश शब्द ही बताता है कि प्राकृत बोलियाँ किस प्रकार साहित्य में ढल रही थीं। व्याकरण बनने के पूर्व की भाषा और बोली में परवर्ती भाषा
और बोली से अत्यन्त भिन्नता लक्षित होती है। वेदों की कई ऋचाओं में 'कृत' के लिए 'कड', 'वृत' के लिए 'वुड' तथा 'मृत' के लिए 'मड' शब्द प्रयुक्त मिलते हैं। “पाइअ-सद्दमहण्णवो" की भूमिका में ऐसे तेरह विशिष्ट लक्षणों का विवेचन किया गया है, जिनसे वैदिक और प्राकृत भाषा में साम्य परिलक्षित होता है। वैदिक और प्राकृत भाषा में कुछ ऐसी समान प्रवृत्तियाँ मिलती हैं, जो लौकिक संस्कृत में प्राप्त नहीं होती। श्री वी. जे. चोकसी ने इन दोनों में कई समान प्रवृत्तियों का निर्देश किया है ।२० वेदों की भाँति अवेस्ता की भाषा और प्राकृतों में कुछ सामान्य प्रवृत्तियां समान रूप से पाई जाती हैं । संस्कृत का अन्त्य 'अस्' अवेस्ता में 'ओ' देखा जाता है; यथा : अईयो, अउरुषो, इथ्येजो, गरमो, हमो, यो, नो, होमो, दूरोषो, मश्यो, यिमो, पुथ्रो, आदि ।
२. अवेस्ता, प्राकृत और अपभ्रश में स्वर के पश्चात् स्वर का प्रयोग प्रचलित रहा है। किन्तु वैदिक और संस्कृत में एक साथ दो स्वरों का प्रयोग नहीं मिलता। अवेस्ता के कुछ शब्द हैं : अएइती, अउरुन, अएम्, प्राग्रत्, अइ प्रादि । प्राकृत-अपभ्रंश में इस प्रकार के शब्द हैं : आइत्र, अोइ, एउ, उइन्न, दइउ. संजोइउ, पलोइउ, पाइउ, अइ, अइरा, पाइद्ध, पाउ, अाएस, आइच्च इत्यादि ।
३. अवेस्ता में एक ही शब्द कई रूपों में मिलता है; यथा : आयु, प्रयु; हमो, हामो; हुतश्तम्, हुताश्तम्; अद्धानम्, अद्धनम्; य, यो इत्यादि। अपभ्रश में भी कुच्छरकोच्छर; कुड्ड-कोड्ड, कुमर-कुम्वर, णिरक्क-णिरिक्क-णिरुक्क, तिगिछ-तिगिछि-तिगिच्छ, णिडल-णिडाल, ढंक-ढंख, झिंदु-मेंदु, मेंदुलिय-भेदुलिय, मुंबुक्क झुमुक्क-झुव्वुक, जोवजो-जोय, झंप-झपा, आदि वैकल्पिक शब्द-रूप प्रचुरता से मिलते हैं। प्राकृत में भी इस तरह के शब्द-रूप विपुल मात्रा में मिलते हैं।
४. ल्हेमन ने प्राग्भारोपीय ध्वनि-प्रक्रिया का विचार करते हुए निर्दिष्ट किया है कि व्यतिरेकी ध्वनिप्रक्रियात्मक प्रामाणिक स्त्रोतों का निश्चय करने में एक प्राक्षरिक अपिथ ति भी है। सामान्य रूप से स्वर-ध्वनि के परिवर्तन को अपश्रु ति कहते हैं। अपश्र ति मात्रिक और गुणीय दोनों प्रकार की कही गई है। प्राग्भारोपीय ध्वनि-प्रक्रिया में एक पद ग्राम में विविध स्वर ध्वनि ग्रामों में परिवर्तन सभी भारोपीय बोलियों में लक्षित होते हैं और यही कारण है कि वे बोलियां भारोपीय भाषा की मूल स्रोत हैं ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org